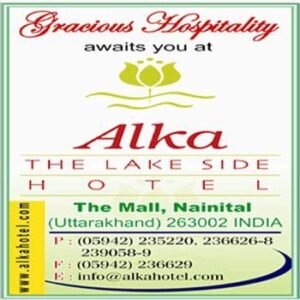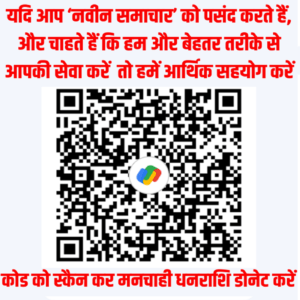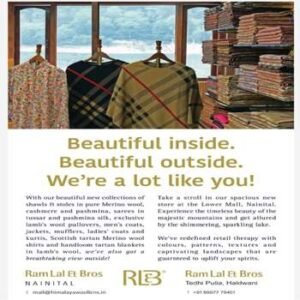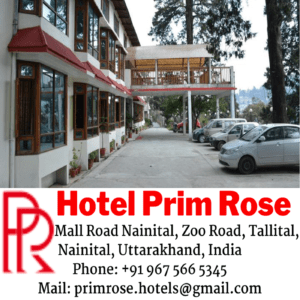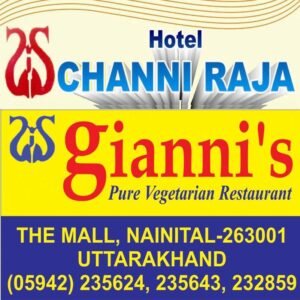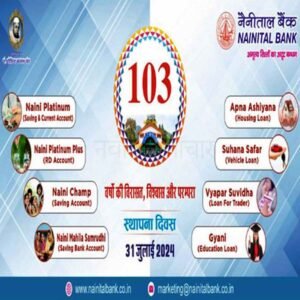संचार, समाचार लेखन, संपादन, विज्ञापन, फीचर व ब्रांड प्रबंधन

संचार
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल। संचार एक तकनीकी शब्द है जो अंग्रेजी के कम्यूनिकेशन का हिन्दी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है, किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। इसके माध्यम से मनुष्य के सामाजिक संबंध बनते और विकसित होते हैं। मानवीय समाज की समस्त प्रक्रिया संचार पर आधारित है। इसके बिना मानव नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य अपनी जाग्रतावस्था में संचार करता है अर्थात बोलने सुनने सोचने देखने पढ़ने लिखने या विचार विमर्श में अपना समय लगाता है। जब मनुष्य अपने हाव भाव संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो वह संचार कहलाता है।
पत्रकारिता से संबंधित निम्न लेख भी सम्बंधित लाइनों पर क्लिक करके पढ़ें :
-
पत्रकारिता : संकल्पना, प्रकृति और कार्यक्षेत्र, महिला पत्रकार, पत्रकारिता की उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, वृद्धि और विकास
-
विश्व व भारत में पत्रकारिताका इतिहास
-
उत्तराखण्ड की पत्रकारिता का इतिहास
-
विश्व व भारत में रेडियो-टेलीविज़न का इतिहास तथा कार्यप्रणाली
-
फोटोग्राफी का इतिहास एवं संबंधित आलेख व समाचार
-
कुमाऊं के ब्लॉग व न्यूज पोर्टलों का इतिहास
-
संचार, समाचार लेखन, संपादन, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो, फीचर व ब्रांड प्रबंधन
-
संचार के द्विपद, बहुपद, अधिनायकवादी, उदारवादी, सामाजिक उत्तरदायित्व युक्त, कम्युनिस्ट व एजेंडा सेटिंग सिद्धांत
-
न्यू मीडिया (इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि) : इतिहास और वर्तमान
-
इंटरनेट-नए मीडिया के ताजा महत्वपूर्ण समाचार
-
यहां कानून से भी लंबे निकले सोशल मीडिया के हाथ…
-
-
संचार की परिभाषा
· संकेतों द्वारा होने वाला संप्रेषण संचार है – लुडबर्ग
· मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों व भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है – लीलैंड ब्राउन
· संचार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजे गये संदेश के संप्रेषण की प्रक्रिया है – डैनिस मैक कवैल
· संचार समानुभूति का विनिमय है – कौफीन और शाँ
· संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे – थीयो हैमानसंचार प्रक्रिया
वेब पर वायरल :
संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला प्रेषक कहलाता है और संदेश प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता। दोनों के बीच एक माध्यम होता है जिसके सहयोग से प्रेषक का संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है। प्राप्तकर्ता के दिल दिमाग पर प्रभाव डालता है जिससे सामाजिक सरोकारों में बदलाव आता है। देश तथा विदेश में मनुष्य की दस्तकें बढ़ती है इसलिये संचार प्रक्रिया का पहला चरण प्रेषक होता है। इसे इनकोडिंग भी कहते है । इनकोडिंग के बाद विचार सार्थक संदेश के रूप में ढल जाता है। जब प्राप्तकर्ता अपने मस्तिक में उक्त संदेश को ढाल लेता है तो संचार की भाषा में डीकोडिंग कहतें हैं। डीकोडिंग के बाद प्राप्तकर्ता उस संदेश का अर्थ समझता है। वह अपनी प्रतिक्रिया प्रेषक को भेजता है। तो उस प्रक्रिया को फीडबैक कहतें हैं।संचार के कार्य
संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपंन करती है –
· सूचना या जानकारी देना ।
· संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना।
· संचार व्यक्तियों समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है।
· संचार विभिन्न तथ्यों विचारों मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है।
· मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
· संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है।संचार के प्रकार:
अंत:व्यक्तिक संचार
यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी परिधि में स्वंय व्यक्ति होता है। मनुष्य अपने अनुभवों घटनाओं व्यक्तियों प्रभावों एवं परिणामों का आकलन करता है। संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश भेजने वाला स्वंय ही होता है। आत्मक विश्लेषण आत्मविवेचन आत्मप्रेरणा आदि इसी प्रकार के संचार कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते है जब एक व्यक्ति अकेला अपने आप से बात करता है तो उसे स्वगत संचार कहा जाता है। क्योंकि वह स्वयं से ही संचार करता है।
अंतरवैयक्तिक संचार
जब व्यक्ति एक दूसरे बातचीत करता है तो उसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। बातचीत सामने बैठकर टेलीफोन मोबाइल पेजर संगीत चित्र ड्रामा लोककला इत्यादि से हो सकती है। इस संचार प्रक्रिया में संदेशों का प्रेषण मौखिक भी हो सकता है और स्पर्श मुस्कुराहट आदि से भी। इसमें प्रतिपुष्टि तुरंत हो सकती है। संदेश प्रेषक और संदेश ग्राहक की निकटता इस प्रकार के संचार की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है।
अंतरवैयक्तिक संचार दुतरफा प्रक्रिया है अर्थात स्त्रोता संदेश प्राप्त करते ही प्रतिक्रया देता है। यह संचार प्रक्रिया गतिशील होता है।समूह संचार
जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने बैठकर विचार विमर्श, विचार गोष्ठी वाद विवाद कार्य शिविर सार्वजनिक व्याख्यान इंटरव्यू आदि करता है तो उसे समूह संचार कहते है। यह बहुत प्रभावशाली होता है। क्योंकि इसमें वक्ता को अपने अपने क्षेत्र में अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। स्कूल कॉलेज प्रशिक्षण केन्द्र चौपाल रंगमंच कमेटी हॉल जैसे प्रमुख स्थानों पर संचार गतिशील होता । दूसरे शब्दों में समूह संचार उन व्यक्तियों के बीच संभव है जो किसी उद्देश्य के लिये अमुख स्थान पर एकत्र होते हैं।
जन संचार
जनसंचार का अर्थ विस्तृत आकार के बिखरे हुये समूह तक संचार माध्यमों द्वारा संदेश पहुंचाना है। पर इस प्रकार के संचार में भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। रेडियो टेलीविजन टेपरिकार्डर फिल्म वीडियो कैसेट सीडी के अलावा समाचारपत्र पत्रिकायें पुस्तकें पोस्टर इत्यादि इसके माध्यम कहलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत विशाल है इसे किसी परिधि में रखना कठिन है। वर्तमान समाज में जनसंचार का कार्य सूचना प्रेषण विश्लेषण ज्ञान एवं मुल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है।
कनाडा में जन्मे प्रोफेसर, फिलॉसफर और कम्यूनिकेशन थियोरिस्ट मैक्लूहान ने ही मीडिया की मशहूर थियोरी दी है- द मीडियम इज द मैसेज (माध्यम ही संदेश है).
मैक्लूहान ने कहा था कि कम्यूनिकेशन ही विकास निर्धारित करता है. साथ ही टेक्नॉलजी ही एक समाज को एक आकार देता है.
टीवी की शुरुआत के दौर में ही मैक्लूहान ने इंटरनेट का विजन पेश कर दिया था उन्होंने कह दिया था कि ये कम्यूनिकेशन सबकुछ बदल देगा. उन्होंने संभावना जता दी थी कि इस नए मीडियम का प्रभाव अभूतपूर्व होगा और वो बिल्कुल सही थे.

मार्शल मैक्लूहान उन्होंने कई किताबें लिखी हैं- अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडियम इद द मैसेज, द गुटेनबर्ग गैलेक्सी आदि.उन्होंने संचार की इस थ्योरी को चार हिस्सों में बांटा है-
- मौखिक संचार
- शब्दों के जरिए संचार
- छपाई का दौर
- इलेक्ट्रॉनिक दौर.
संचार और माॅडेल…..
पृथ्वी पर मानव सभ्यता के साथ जैसे-जैसे संचार प्रक्रिया का विकास होता गया, वैसे-वैसे संचार के प्रारूपों का भी। अत: संचार का अध्ययन प्रारूपों के अध्ययन के बगैर अधूरा माना जाता है। समाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, संचार शास्त्र, प्रबंध विज्ञान इत्यादि के अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान में प्रारूपों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाज वैज्ञानिकों व संचार विशेषज्ञों ने अपने-अपने समय के अनुसार संचार के विभिन्न प्रारूपों का प्रतिपादन किया है। सामान्य अर्थों में हिन्दी भाषा के च्प्रारूपज् शब्द से अभिप्राय रेखांकन से लिया जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा रूशस्रड्डद्य में कहते हैं।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार- च्प्रारूप से अभिप्राय किसी वस्तु को उसके लघु रूप में प्रस्तुत करना है।ज् प्रारूप वास्तविक संरचना न होकर उसकी संक्षिप्त आकृति होती है। जैसे- पूरी दुनिया को बताने के लिए छोटा सा च्ङ्गलोबज्। किसी सामाजिक घटना अथवा इकाई के व्यवहारिक स्वरूप को बताने के लिए अनुभव के सिद्धांत के आधार पर तैयार की गई सैद्धांतिक परिकल्पना को प्रारूप कहते हैं। दूसरे शब्दों में- प्रारूप किसी घटना अथवा इकाई का वर्णन मात्र नहीं होता है, बल्कि उसकी विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है। प्रारूप के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली जानकारी या सूचना, वास्तविक जानकारी या सूचना के काफी करीब होता है। इस प्रकार, प्रारूप देखने में भले ही काफी छोटा होता है, लेकिन अपने अंदर वास्तविकता की व्यापकता को समेटे होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने प्रारूप को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है :-- प्रारूप प्रतीकों एवं क्रियान्वित नियमों की एक ऐसी संरचना है, जो किसी प्रक्रिया के अस्तित्व से सम्बन्धित बिन्दुओं के समानीकरण के लिए संकल्पित की जाती है।
- प्रारूप संचार यथा- घटना, वस्तु, व्यवहार का सैद्धान्तिक तथा सरलीकृत प्रस्तुतिकरण है।
- किसी घटना, वस्तु अथवा व्यवहारात्मक प्रक्रिया की चित्रात्मक, रेखात्मक या वाचिक अभिव्यक्ति का प्रारूप है।
- प्रारूप एक ऐसी विशेष प्रक्रिया या प्रविधि है, जिसे किसी अज्ञात सम्बन्ध अथवा वस्तुस्थिति की व्याख्या के लिए संदर्भ बिन्दु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
संचार एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। परिवर्तनशीलता के अनुपात में संचार प्रक्रिया की जटिलता घटती-बढ़ती रहती है। संचार प्रारूप सिद्धांतों पर आधारित संचरना होती है, जिसमें व्यक्ति व समाज पर पडऩे वाले प्रभावों की अवधारणाओं को भी सम्मलित किया जाता है। अत: संचार प्रारूप की संरचना संचार प्रक्रिया की समझ व परिभाषा पर निर्भर करती है। संचार शास्त्री डेविटो के शब्दों में- संचार प्रारूप संचार की प्रक्रियाओं व विभिन्न तत्वों को संगठित करने में सहायक होती है। ये प्रारूप संचार के नये-नये तथ्यों की खोज में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुभवजन्य व अन्वेषणात्मक कार्यों द्वारा ये प्रारूप भावी अनुसंधान के लिए संचार से सम्बन्धित प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इन प्रारूपों की मदद से संचार से सम्बन्धित पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। संचार की विभिन्न प्रक्रियाओं व तत्वों का मापन किया जा सकता है।संचार के मॉडल :
संचार की प्रक्रिया का अध्ययन एक विज्ञान है। यह प्रक्रिया जटिल है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से इस प्रक्रिया का वर्णन किया है। संचार की प्रक्रिया को बताने वाला चित्र मॉडल कहलाता है। इन मॉडलों से हमें संचार की गतिशील और सक्रिय प्रक्रिया समझने में आसानी होती है। ये संचार के सिद्धांत और इसके तत्वों के बारे में भी बताते हैं। संचार मॉडल से हमें पता चलता है कि संचार में किन-किन तत्वों की क्या भूमिका है और ये एक दूसरे का कैसे प्रभावित करते हैं?
संचार की शुरुआत लाखों साल पहले जीव की उत्पत्ति के साथ मानी जाती है। संचार की प्रक्रिया और इससे जुड़े कई सिद्धांत की जानकारी हमें प्राचीन ग्रथों से मिलती है। लेकिन उन जानकारियों पर और अध्ययन की आवश्यकता है। अरस्तू की व्याख्या के आधार पर कुछ विद्वानों ने संचार के सबसे पुराने मॉडल को बनाने की कोशिश की है। आप उसके बारे में जानते हैं?
एक तरफा संचार प्रारूप(One-way Communication Modal)संचार का यह प्रारूप तीर की तरह होता है, जिसके अंतर्गत संचारक अपने सदेश को सीधे प्रापक के पास प्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक तरफ संचार प्रारूप के अंतगर्त केवल संचारक अपने विचार, जानकारी, अनुभव इत्यादि को सूचना के रूप में सम्प्रेषित करता है। उपरोक्त सूचना के संदर्भ में प्रापक अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है अथवा प्रतिक्रिया करता है तो संचारक उससे अंजान रहता है। एक तरफा संचार प्रक्रिया की परिकल्पना सर्वप्रथम हिटलर और रूजवेल्ट जैसे तानाशाह शासकों ने की, लेकिन इसका प्रतिपादन २०वीं शताब्दी के तीसरे दशक के दौरान अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने किया। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग ने कार्ल होवलैण्ड की अध्यक्षता में अस्त्र परिचय कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए गठित मनोवैज्ञानिकों की एक विशेष कमेटी ने अपने अध्ययन के द्वारा पाया कि संचारक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषित संदेश का प्रापकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट 1949 में प्रकाशित हुई। इसको अद्यो्रलिखित रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है :-इस प्रारूप से स्पष्ट है कि सूचना का प्रवाह संचारक से प्रापक तक एक तरफा होता है, जिसमें संचार माध्यम मदद करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र इत्यादि की मदद से सूचना का सम्प्रेषण एक तरफा संचार का उदाहरण है। इस प्रारूप का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सूचना के प्रवाह को मात्र संचार माध्यमों की मदद से दर्शाया गया है, जबकि समाज में सूचना का प्रवाह बगैर संचार माध्यमों के प्रत्यक्ष भी होता है।दो तरफा संचार प्रारूप(Two- way Communication Modal)संचार के इस प्रारूप में संचारक और प्रापक की भूूमिका समान होती है। दोनों अपने-अपने तरीके से संदेश सम्प्रेषण का कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आमने-सामने बैठकर संदेश सम्प्रेषण के दौरान रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे संचार माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ती है। दो तरफा संचार प्रारूप में संचारक और प्रापक को समान रूप से अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलता है। संचारक और प्रापक के आमने-सामने न होने की स्थिति में दो तरफा संचार के लिए टेलीफोन, मोबाइल, ई-मेल, एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैटिंग, अंतर्देशीय व पोस्टकार्ड जैसे संचार माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसमें टेलीफोन, मोबाइल, ई-मेल व एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स व चैटिंग अत्याधुनिक संचार माध्यम है, जिनका उपयोग करने से संचारक और प्रापक के समय की बचत होती है, जबकि अंतर्देशीय व पोस्टकार्ड परम्परागत संचार माध्यम है, जिसमें संचारक द्वारा सम्प्रेषित संदेश को प्रापक तक पहुंचने में पर्याप्त समय लगता है। समाज में दो तरफा संचार माध्यम के बगैर भी होता है। पति-पत्नी, गुरू-शिष्य, मालिक-नौकर इत्यादि के बीच वार्तालॉप की प्रक्रिया दो तरफा संचार का उदाहरण है।उपरोक्त प्रारूप से स्पष्ट है कि सूचना का प्रवाह संचारक से प्रापक की ओर होता है। समय, काल व परिस्थिति के अनुसार संचारक और प्रापक की भूमिका बदलती रहती है। संचारक से संदेश ग्रहण करने के उपरान्त प्रापक जैसे ही अपनी बात को कहना शुरू करता है, वैसे ही वह संचारक की भूमिका का निर्वाह करने लगता है। इसी प्रकार उसकी बात को सुनते समय संचारक की भूमिका बदलकर प्रापक की हो जाती है।अरस्तू का मॉडल :
-
करीब 2300 साल पहले ग्रीस के दार्शनिक अरस्तू ने अपनी किताब ”रेटॉरिक” में संचार की प्रक्रिया के बारे में बताया है। रेटॉरिक का हिन्दी में अर्थ होता है भाषण देने की कला। अरस्तू ने संचार की प्रक्रिया को बताते हुए पॉंच प्रमुख तत्वों की व्याख्या की है। संचार प्रेषक (भेजने वाला), संदेश (भाषण), प्राप्तकर्त्ता, प्रभाव और विभिन्न अवसर।
अरस्तू के विश्लेषण को निम्नलिखित चित्र या मॉडल के द्वारा समझा जा सकता है।

अरस्तू के अनुसार संचार की प्रक्रिया रेखीय है। रेखीय का अर्थ है एक सीधी लाईन में चलना। प्रेशक श्रोता को संदेश भेजता है जिससे उस पर एक प्रभाव उत्पन्न होता है। हर अवसर के लिए संदेश अलग-अलग होते हैं।
अरस्तू के अनुसार संचार का मुख्य उद्देष्य है श्रोता पर प्रभाव उत्पन्न करना। इसके लिए प्रेषक विभिन्न अवसरों के अनुसार अपने संदेश बनाता है और उन्हें श्रोता तक पहुंचाता है जिससे कि उनपर प्रभाव डाला जा सके। विभिन्न अवसरों पर संदेश कैसे तैयार किये जाये? इसका विश्लेषण भी अरस्तू करते हैं। संदेश तैयार करने के लिए वे तीन प्रमुख घटकों की चर्चा करते हैं, पैथोस्, इथोस् और लोगोस्।
पैथोस् का शाब्दिक अर्थ है दुःख। अरस्तु के अनुसार यदि संदेश इस तरह से तैयार किये जायें, जिससे कि श्रोता के मन में दुःख या इससे संबधित भाव उत्पन्न हो सके तो श्रोता के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अपनी बात मनवाई जा सकती है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपका छोटा भाई आपके साथ बाजार जाने की जिद करता है, लेकिन आप उसे नहीं ले जाना चाहते हैं। लेकिन, जब वो जोर-जोर से रोने बिलखने लगता है तो आप मजबूर होकर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकरण का विश्लेषण करके देखिए। बच्चे ने संचार की शुरुआत की और अपने संदेश को उसने दुःख से इस तरह भर दिया कि श्रोता उसकी बात मानने को मजबूर हो गया। अर्थात प्रेषक ने अवसर के अनुरूप अपने संदेश का निर्माण किया। जिससे कि श्रोता पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न हो सके।
मैंने पहले कहा था कि रेटॉरिक का अर्थ होता है भाषण देने की कला। यह मुख्य रूप से प्राचीन काल में राजनेताओं को सिखाई जाती थी, आज भी कई कुशल राजनेता ऐसे हैं जो अरस्तू की व्याख्या को अपने भाषण में आत्मसात करते हैं। तो क्या आप के दिग्गज नेता आशुतोष ने भी गजेन्द्र हत्याकान्ड मामले में अरस्तू के संदेशों से सीख ली थी? आपको याद होगा कि वे दहाड़े मारकर रोने लगे थे।
”इथॉस्” का शाब्दिक अर्थ है विश्वशनीयता। विश्वशनीयता को लंबे समय में हासिल किया जा सकता है। इसके लिए प्रेषक को अपने आचार-व्यवहार में इस तरह के परिवर्तन लाने होते हैं जिससे कि सामान्य जन का विश्वास उस पर मजबूत हो सके। जब लोगों का विश्वास उस पर होगा तो वो जो भी संदेश देगा उसका प्रभाव श्रोता पर अनुकूल पड़ेगा। इसे समझने के लिए शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर को याद करिये। सीजर की हत्या हो गयी है। मार्क अंटोनी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपना भाषण देता है। उस प्रसिद्ध भाषण के बाद विद्रोह हो जाता है। अंटोनी पर लोगों का विश्वास है क्योंकि उसकी छवि भरोसेमंद है। अंटोनी के इस प्रसिद्ध भाषण में अरस्तू के बताये तीनों तत्व पैथॉस्, इथॉस् और लोगॉस् का बखूबी प्रयोग किया है। इसी तरह महाभारत में युधिष्ठिर पर इतना विश्वास है कि उसके कहे झूठ पर विश्वास करके उसके गुरू द्रोणाचार्य अपना हथियार जमीन पर रख देतें हैं, और उनकी हत्या हो जाती है। यह भी इथॉस् का ही एक उदाहरण है।
लोगॉस् का शाब्दिक अर्थ है तर्क। अरस्तू कहते हैं कि प्रेषक का संदेश तर्क से भरपूर होना चाहिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशक को अपनी बात तार्किक तरीके से रखनी चाहिए जिससे कि श्रोता पर प्रभाव पड़े। जूलियस सीजर नाटक में अंटोनी के भाषण में संदेश बड़े तार्किक तरीके से रखे गये हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। न्यायालय में वकील मुकदमें की पैरवी करता है। इस दौरान वो प्रेषक है जबकि न्यायाधीश महोदय श्रोता। वकील को अपने संदेश या बातों से जज को प्रभावित करना है। इसके लिए वो तर्क का सहारा लेता है और घटना का तार्किक विश्लेषण न्यायाधीश के सामने रखता है। यदि संदेश तर्कपूर्ण है तो इसका प्रभाव पड़ता है और वकील साहब न्यायाधीश महोदय से अपने पक्ष में फैसला ले लेते हैं।
संचार की बुलेट थ्योरी : अतीत एवं वर्तमान का पुनरावलोकन
डा. राम प्रवेश राय, जन संचार के सिद्धांतों को लेकर अक्सर ये बहस चलती रहती है कि ये पुराने सिद्धांत व्यवहार मे महत्वहीन साबित होते है और पत्रकारिता शिक्षण मे इन सिद्धांतों पर अधिक ज़ोर नहीं देना चाहिए। ऐसा ही एक सिद्धांत है बुलेट या हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी इसको एक चरणीय संचार मॉडल के रूप मे भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि किसी जन माध्यम से प्रसारित संदेश सीधे श्रोताओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। अर्थात जन माध्यमों द्वारा सूचना प्रेषित करने और श्रोताओ द्वारा सूचना प्राप्त करने के बीच अन्य कोई चरण नहीं होता। जिस प्रकार बंदूक से निकली गोली सीधे निशाने पर पहुँचती है उसी प्रकार जन माध्यमों से निकला संदेश भी सीधे श्रोताओ तक पहुंचता है। यहाँ ध्यान देने के दो प्रमुख बिन्दु है- एक तो जन माध्यम की शक्ति यानि इसके अनुसार जन माध्यम इतने शक्तिशाली है कि उनकी पहुँच प्रत्येक श्रोता तक सीधी है और यह जब चाहे श्रोता तक अपनी बात पहुंचा सकता है। दूसरा श्रोताओं का अत्यधिक तत्पर और उत्सुक होना जिससे जन माध्यमों द्वारा प्रसारित कोई भी संदेश वह तुरंत प्राप्त कर लें।
 (Source: Communication theories and models by N. Andal, Himalaya Publishing House, 2011, page-119)
(Source: Communication theories and models by N. Andal, Himalaya Publishing House, 2011, page-119)उपरोक्त मॉडल से यह स्पष्ट होता है कि ट्रांसमीटर द्वारा प्रेषित संदेश होमोजीनियस (समरूप) जनता द्वारा ग्रहण किया जाता है और ट्रांसमीटर तथा जनता के मध्य अन्य कोई चरण मौजूद नहीं है अतः इसको एक चरणीय संचार या बुलेट सिद्धांत कहा जाता है। हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी संचार के एक चरण के साथ-साथ इसके प्रभाव को भी महत्व देती है जिसको निम्न चित्र के अनुसार समझा सकता है –
जन माध्यम इंजेक्शन कि भांति श्रोताओ के दिमाग मे संदेश भरते है और श्रोता तुरंत ही इसपर प्रतिक्रिया करते है। हाइपोडर्मिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ सिरिन्ज है और इसीलिए इस मॉडल का नाम हाइपोडर्मिक रखा गया है। इसके अनुसार तीन प्रमुख बिन्दु प्रमुख सामने आते है-
1- लिनियर कमुनिकेशन- अर्थात ये एक रेखीय संचार मॉडल है जो जन माध्यम से सीधे श्रोता तक पहुंचता है।
2- पैसिव आडिएन्स- अर्थात निष्क्रिय श्रोता, जन माध्यम जो भी संदेश चाहे श्रोता के दिमाग मे भर सकता है और श्रोता उसका कोई विरोध नहीं करेगा।
3- नो इंडिविजुयल डिफ़ेरेन्स- सभी श्रोता एक समान होते है जिनमे कोई वैयक्तिक अंतर नहीं होता। इसलिए जो भी संदेश प्रसारित किए जाते है सभी श्रोता उस संदेश को एक जैसे ही समझते है। जैसे यदि किसी माध्यम से डॉग प्रसारित किया गया है तो सभी श्रोता उसको डॉग ही समझेगे कोई भी पेट स्ट्रे डॉग आदि नहीं समझेगा।इस सिद्धांत का विकास 1930 के आस पास हुआ था और 40 के दशक के अध्ययनो मे जन माध्यमों को अत्यंत शक्तिशाली और जनता के विचारो को त्वरित प्रभावित करने वाला बताया गया। शायद जन माध्यमों के इस शक्तिशाली प्रभाव को सहयोग प्रदान करने वाले निंलिखित कारण थे-
• रेडियो और टीवी का उदय एवं त्वरित गति से उसका विकास
• पर्सुएशन इंडस्ट्री जैसे विज्ञापन और प्रोपोगंडा व्यवसाय का उदय
• पयान फंड (Payne Fund) का अध्ययन जो 1930 मे किया गया और बच्चो पर मोशन पिक्चर्स का प्रभाव देखा गया
• द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की जन माध्यमों पर मोनोपोली आदियह मॉडल भी बुलेट सिधान्त का ही समर्थन करता है क्योंकि यह भी मीडिया की त्वरित पहुँच और उसके शक्तिशाली प्रभाव को ही बताता है। इस मॉडल को संचार वैज्ञानिको ने निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है-
Hypodermic model uses the same idea of shooting paradigm. It suggests that the media injects its message straight into the passive audience. ——– Croteau Hones, 1997
This passive audience is immediately affected by these messages. The public essentially cannot escape from the media’s influence and is therefore considered a “sitting duck” ——– Croteau Hones, 1997
Both models suggest that the public is vulnerable to the message shot at them because of the limited communication tools and the studies of media effect on the masses at the time. ——– Davis, Baron 1981
व्यावहारिक पक्ष :
नए माध्यमों के प्रति जनता का जुड़ाव काफी अधिक होता है और जब 30 के दशक मे इस सिद्धांत का विकास हुआ तो रेडियो सबसे नया माध्यम था फलतः लोगो का जुड़ाव भी रेडियो के प्रति सर्वाधिक था इसी सं विज्ञापन इंडस्ट्री का भी उदय हुआ था तो विज्ञापन कंपनियाँ भी लोगो को लुभाने के लिए नए नए प्रयोग कर रही थी। इन माध्यमों का कितना असर लोगो पर था इसका उदाहरण 30 अक्तूबर 1938 को मिलता है जब आसीन वेल्स और मर्करी थियेटर ने एच॰ जी॰ वेल्स “War of the world” रेडियो संस्करण प्रसारित किया। पहली बार किसी रेडियो कार्यक्रम के बीच एक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया, इस न्यूज़ बुलेटिन को श्रोताओं ने क्या सुना वह इस प्रकार था-“Martians had begun an invasion of earth in a place called Grover’s Mil, New Jersey”
ये समाचार श्रोताओ के लिए एक भयानक समाचार साबित हुआ। इस समाचार ने सोशल साइकलोजी, सिविल डिफ़ेंस और ब्राडकास्ट इतिहास को बदल कर रखा दिया। लगभग 12 मिलियन अमेरिकियो ने यह प्रसारण सुना जिसके कारण ट्रैफिक, संचार प्रणाली, धार्मिक सेवाएँ ठप पड़ गई, एक अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया था और लोगो को लग रहा था कि वास्तव मे कोई एलियन आक्रमण हुआ है। लोग अपने शहर को छोड़ कर गाँव की ओर भागने लगे, राशन की दुकानों पर लंबी लाइन लग गई। अमेरिका अचानक से बेहाल हालत मे आ गया था। जबकि ये प्रसारण रेडियो नाटक ही हिस्सा था। इस घटना के बाद संचार वैज्ञानिको ने “war of the world” को मैजिक बुलेट सिधान्त के मुख्य उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया।
अब इस सिद्धांत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे देखे तो मुज्जफरपुर की घटना बुलेट थ्योरी का ही उदाहरण है, जहा फेसबुक पर कोई आपत्तीजनक कंटेन्ट अपलोड होने पर दंगे भड़क गए और बाद मे ये भी खबर आई कि जो विडियो फेसबुक पर अपलोड हुआ था वो भारत का नहीं था। ऐसा कुछ मंज़र उस दिन भी था जब बाबरी मस्जिद केस का फैसला आना था सरकारी ओफिसेज बंद हो गए सभी शहरो मे कौकसी बढ़ा दी गई बाज़ार भी खाली हो गए, ऐसा इसलिए था कि यदि किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला आया और वह जैसे ही मीडिया मे प्रसारित होगा दंगे भड़क उठेंगे अर्थात इस सिद्धांत के पूर्वानुमान के आधार पर ही ऐसे कदम उठाए गए लेकिन कोर्ट का फैसला आने और मीडिया मे प्रसारित होने के बाद भी सब कुछ शांत रहा और किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं मिली। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मच के दौरान इस सिद्धांत के असर को देखा जा सकता है। इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि इस पुराने सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी है लेकिन इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर नहीं देखने को मिलता है ऐसा शायद इसलिए है कि अब मीडिया का स्वरूप खुद इतना व्यापक हो गया है कि अब मीडिया कंटेन्ट वर्ग विशेष के लिए तैयार हो रहे है न कि सामान्य श्रोता के लिए।
डॉ॰ राम प्रवेश राय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में न्यू मीडिया के सहायक प्रोफेसर हैं
लॉसवेल मॉडल (Lasswell’s model)
हेराल्ड डी. लॉसवेल अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री हैं, लेकिन इनकी दिलचस्पी संचार शोध के क्षेत्र में थी। इन्होंने ने सन् १९४८ में संचार का एक शाब्दिक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे दुनिया का पहला व्यवस्थित प्रारूप कहा जाता है। यह फार्मूला प्रश्न के रूप में था। लॉसवेल के अनुसार- संचार की किसी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका निम्न पांच प्रश्नों के उत्तर को तलाश करना। यथा--
- कौन (who)
- क्या कहा (says what)
- किस माध्यम से (in which channel),
- किससे (To whom) और
- किस प्रभाव से (with what effect)।
इसे निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से समझा जा सकता है :-इन पांच प्रश्नों के उत्तर से जहां संचार प्रक्रिया को आसानी से समझे में सहुलित मिलती है, वहीं संचार शोध के पांच क्षेत्र भी विकसित होते हैं, जो निम्नांकित हैं :-1. Who Communicator Analysis संचारकर्ता विश्लेषण2. Saya what Massige Analysia अंतर्वस्तु विश्लेषण3. In Which channel Mediam Analysis माध्यम विश्लेषण4. To whom Audience Analysis श्रोता विश्लेषण5.with what effect Impact Analysis प्रभाव विश्लेषणहेराल्ड डी. लॉसवेल ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका में प्रचार की प्रकृति, तरीका और प्रचारकों की भूमिका विषय पर अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि आम जनता के विचारों, व्यवहारों व क्रिया-कलापों को परिवर्तित या प्रभावित करने में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी आधार पर लॉसवेल ने अरस्तु के संचार प्रारूप के दोषों को दूर कर अपना शाब्दिक संचार फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसमें अवसर के स्थान पर संचार माध्यम का उल्लेेख किया। लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप का निर्माण बहुवादी समाज को केंद्र में रखकर किया, जहां भारी संख्या में संचार माध्यम और विविध प्रकार के श्रोता मौजूद थे। हेराल्ड डी. लॉसवेल ने अपने संचार प्रारूप में फीडबैक को प्रभाव के रूप में बताया है तथा संचार प्रक्रिया के सभी तत्त्वों को सम्मलित किया है।लॉसवेल फार्मूले की सीमाएं : स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, शिकागो के सदस्य रह चुके हेराल्ड डी.लॉसवेल का फार्मूले को संचार प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय लोकप्रियता मिली है। इसके बावजूद संचार विशेषज्ञों इसे निम्नलिखित सीमा तक ही प्रभावी बताया है :-
-
- लॉसवेल का फार्मूला एक रेखीय संचार प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण सीधी रेखा में कार्य करता है।
- इसमें फीडबैक को स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है।
- संचार की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
- संचार को जिन पांच भागों में विभाजित किया गया है, वे सभी आपस में अंत:सम्बन्धित हंै।
- संचार के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यवधान को नजर अंदाज किया गया है।
-
ऑसगुड-श्राम का संचार प्रारूप (OSGOOD-SCHRAMM’S MODAL OF COMMUNICATION)
इस मॉडल को चाल्स ई.ऑसगुड ने प्रतिपादित किया है। आपको बता दें कि ऑसगुड एक मनोभाषा विज्ञानी थे। इस मॉडल को उन्होंने साल-1954 में प्रतिपादित किया। इस मॉडल के अनुसार संचार गत्यात्मक और परिवर्तनशील होता है, जिसमें शामिल होने वाले संचारक और प्रापक इनकोडिंग औग डिकोडिंग के साथ-साथ संदेश की व्याख्या भी करते हैं। इस मॉडल के अनुसार संचारक एक समय ऐसा आता है जब संचारक की भूमिका बदलकर प्रापक की हो जाती है तो वहीं प्रापक की भूमिका बदलकर संचारक की हो जाती है। अत: संचारक और प्रापक दोनों को व्याख्याकार की भूमिका निभानी पड़ती है।इस मॉडल को हम सर्कुलर प्रारुप भी कहते है।संचार के इस मॉडल को डेविड के. बरलो ने साल 1960 में प्रतिपादित किया।जो कि निम्न है-इस मॉडल में S-M-C-R का अर्थ है :-S : Source (प्रेषक)M : Message (संदेश)C : Channel (माध्यम)R : Receiver (प्रापक)प्रेषक (Source) : जो किसी बात, भावना या विचार को किसी माध्यम से दूसरे तक पहुंचाता है उसे प्रेषक कहते हैं। संचार में प्रेषक का अहम योगदान है। प्रेषक बोलकर, लीखकर, संकेत देकर संचार कर सकता है।संदेश (Message) : प्रेषक जो विचार या भावना दूसरे तक पहुंचाता है उसे संदेश कहते है। संदेश किसी भी रुप में शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतिक इत्यादि रुप में हो सकती है। संदेष भाषाई दृष्टि से हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि तथा चित्रात्मक दृष्टि से फिल्म, फोटोग्राफ इत्यादि के रूप में हो सकती है।माध्यम ( Channel) : माध्यम की मदद से ही संचारक संदेश को प्रापक तक पहुंचता है। संचार के दौरान प्रेषक द्वारा कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। प्रापक देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, सुंघ कर तथा चखकर संदेश को ग्रहण कर सकता है।प्रापक (Receiver ) : संदेश को ग्रहण करने में प्रापक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि प्रापक की सोच सकारात्मक होती है तो संदेश अर्थपूर्ण होता है। इसके विपरीत, प्रेषक के प्रति नकारात्मक सोच होने की स्थिति में संदेश भी अस्पष्ट होता है।
खबरों का खेल बनाम एजेंडा सेटिंग
विनीत उत्पल
मालूम हो कि एजेंडा सेटिंग तीन तरीके से होता है, मीडिया एजेंडा, जो मीडिया बहस करता है। दूसरा पब्लिक एजेंडा जिसे व्यक्तिगत तौर पर लोग बातचीत करते हैं और तीसरा पॉलिसी एजेंडा जिसे लेकर पॉलिसी बनाने वाले विचार करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति काफी हद तक मीडिया को प्रभावित करती है। ऐसे में मीडिया कौन-सी खबरों को तवज्जो देता है, किस खबर का न्यूज वेल्यू किस तरह आंकता है और ऑडियंस की रुचि कैसी खबरों में है, आदि बातें मायने रखती हैं और फिर खबरों के प्रसारण के बाद उन्हीं बातों पर आम लोग अपनी राय कायम करते हैं।(मैक्सवेल)
खबरों के शतरंजी खेल में कौन ‘राजा” है और कौन ‘प्यादा”, दर्शकों और पाठकों के लिए इसे समझना काफी मुश्किल है। हालांकि वे अपनी राय खबरिया चैनलों पर दिखाई जा रही खबरों और अखबारों में छपे मोटे-मोटे अक्षरों के हेडलाइंस को पढ़कर ही बनाती है और लगातार उन मुद्दों पर विचार-विमर्श भी करती है। यही वह विंदु होता है जहां से मीडिया की एजेंडा सेटिंग का प्रभाव पड़ना शुरू होता है। मीडिया की एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहती है कि मीडिया कुछ घटनाओं या मुद्दों को कमोबेश कवरेज देकर राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक बहसों या चर्चाओं का एजेंडा तय करता है। आज खबरिया चैनलों पर प्राइम टाइम की खबरें देंखें तो यह एजेंडा सेटिंग पूरी तरह साफ-साफ समझ में आती है। इस प्राइम टाइम पर सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाई जाती बल्कि जोरदार चर्चा के साथ बहस भी की जाती है। चाहे ईपीएफ पर कर लगाने की बात हो या फिर जेएनयू के छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने का मामला।
अन्ना आंदोलन के दौरान लोकपाल मामले में संसद में बहस के दौरान शरद यादव ने युवा सांसदों से सवाल किया था कि आप लोग बुद्धू बक्से में बहस के लिए क्यों जाते हैं। वह पिछले दस सालों से वहां बहस करने के लिए नहीं जाते हैं। तो उन्होंने जाने-अनजाने जिस मुद्दे की ओर पूरा देश का ध्यान आकर्षित किया था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इसी मीडिया एजेंडा थ्योरी की ओर ही ध्यान आकर्षित कराया था। इस थ्योरी को सरकार के साथ-साथ राजनीतिक दल और कॉरपोरेट समूह बखूबी समझते हैं क्योंकि इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जब भर किसी गंभीर मसला सामने आता है तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, सरकार और कॉरपोरेट समूह के तेजतर्रार प्रवक्ता इस पर चर्चा कर रहे होते हैं और अपने हिसाब से एजेंडे का मुंह मोड़ते रहते हैं।
आज पाठक या दर्शक ही मीडिया का प्रोडक्ट हो चुका है। जाहिर-सी बात है कि हर प्रोडक्ट को एक बाजार की जरूरत होती है और मीडिया का बाजार और खरीदार का रास्ता विज्ञापन से होकर विज्ञापन तक जाता है। यानी मीडिया का बाजार उसका विज्ञापनदाता है। इस मसले को अमेरिका के संदर्भ में नोम चोमस्की अच्छी तरह समझाते हैं। वे लिखते हैं कि वास्तविक मास मीडिया लोगों को डायवर्ट कर रही है। वे प्रोफेशनल स्पोट्र्स, सेक्स स्कैंडल या फिर बड़े लोगों के व्यक्तिगत बातों को जमकर सामने रखती हैं। क्या इससे इतर और कोई गंभीर मामले ही नहीं होते। जितने बड़े मीडिया घराने हैं वे एजेंडे को सेट करने में लगे हुए हैं। अमेरिका के न्यूयार्क टाइम्स और सीबीएस ऐसे मामलों के बादशाह हैं। उनका कहना है कि अधिकतर मीडिया इसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। संस्थानिक ढांचा भी कमोबेश उसी तरह का है। न्यूयार्क टाइम्स एक कॉरपोरेशन है और वह अपने प्रोडक्ट को बेचता है। उसका प्रोडक्ट ऑडियंस है। वे अखबार बेचकर पैसे नहीं बनाते। वे वेबसाइट के जरिए खबरें पेश करके खुश हैं। वास्तव में जब आप उनके अखबार खरीदते हैं तो वे पैसे खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ऑडियंस एक प्रोडक्ट है, इसलिए लोगों के लिए उन लोगों से लिखाया जाता है तो समाज के टॉप लेवल नियतिनियंता हैं। आपको अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार चाहिए और बाजार आपका विज्ञापनदाता है। चाहे टेलीविजन हो या अखबार या और कुछ आप ऑडियंस को बेच रहे होते हैं। (नोम चोमस्की)
यही कारण है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर जब ‘टाइम” मैग्जीन ने कवर स्टोरी छापी और ‘वाशिंगटन पोस्ट” ने लिखा तो भारत सरकार की नींद हराम हो गई। यह मीडिया एजेंडा का ही प्रभाव था कि वैश्विक स्तर पर अपनी साख को बचाने के लिए भारत की कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में कई फैसले लिए। क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि 1990 के दशक में जब मनमोहन सिंह भारत के वित्तमंत्री थे तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का दौर लाया था और भारत अमेरिका सहित दुनिया के आर्थिक संपन्न देशों की नजरों में छा गया। यही वह समय था जब मनमोहन सिंह उस दुनिया के चहेते बन गए लेकिन आज जब पश्चिमी मीडिया ने खिचार्इं की तो फिर उन्हें कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए।
आज के दौर में चाहे सरकार हो या विपक्ष या फिर सिविल सोसाइटी के सदस्य, हर कोई एजेंडा सेट करने में लगा है। देशद्रोह, जेएनयू, अख़लाक़, कन्हैया, रोहित बेमुला, लोकपाल, भ्रष्टाचार, आंदोलन, चुनाव, विदेशी मीडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, टूजी एस्पेक्ट्रम मामला, कोयला आवंटन मामले आदि ऐसे मामले हैं जिनके जरिए विभिन्न रूपों में एजेंडे तय किए गए। क्योंकि हर मामले में चाहे न्यूज चैनल हो या फिर अखबार, हर जगहों पर जमकर बहस हुई और मीडिया की नई भूमिका लोगों ने देखा कि किस तरह आरोपी और आरोप लगाने वाले एक ही मंच पर अपनी-अपनी सफाई दे रहे हैं।
यहीं से मामला गंभीर होता जाता है कि क्या मीडिया की भूमिका एजेंडा सेट करने के लिए होती है। अभी अधिक समय नहीं बीता जब ‘पेड न्यूज” को लेकर संसद तक में हंगामा मचा था। मीडिया के पर्दे के पीछे पेड न्यूज ने किस तरह का खेल खेल रही थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मीडिया एजेंडा सेटिंग की ओर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। यह मामला पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय में सामने आया और इस थ्योरी को लेकर पहली बार मैक्सवेल मैकॉम्ब और डोनाल्ड शॉ ने लिखा। 1922 में पहली बार वाल्टर लिप्पमेन ने इस मामले में अपनी बात सामने रखी थी। उनके मुताबिक लोग किसी भी मामले में सीधे तौर पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि वे स्यूडो वातावरण में रहते हैं। ऐसे में मीडिया उनके लिए काफी मायने रखता है क्योंकि यह उनके विचारों को प्रभावित करता है। (वाल्टर लिप्पमेन) मालूम हो कि मैक्सवेल मैकॉम्ब और शॉ के द्वारा एजेंडा सेटिंग थ्योरी सामने रखने के बाद इस मामले पर करीब सवा चार सौ अध्ययन हो जुके हैं। वैश्विक तौर पर भौगोलिक और एतिहासिक स्तर पर यह एजेंडा कई स्वरूपों में सामने आया बावजूद इसके दुनिया में तमाम तरह के मसले हैं और तमाम तरह की खबरें भी हैं।
अभी तक एजेंडा सेटिंग के गिरफ्त में विदेशी चैनलों और अखबारों के शामिल होने की खबरें सामने आती थीं लेकिन अब भारतीय मीडिया पूरी तरह इसकी चपेट में है। अखबारों की हेडलाइंस के आकार, खबरों का आकार और प्लेसमेंट मीडिया एजेंडा का कारक होता है तो वहीं टीवी चैनलों में खबरों के पोजिशन और लंबाई उसकी प्राथमिकता और महत्ता को तय करती है। इस मामले में आनंद प्रधान लिखते हैं कि कहने को इन दैनिक चर्चाओं में उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण खबर या घटनाक्रम पर चर्चा होती है लेकिन आमतौर पर यह चैनल की पसंद होती है कि वह किस विषय पर प्राइम टाइम चर्चा करना चाहता है। वह कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतंत्र में ये चर्चाएं कई कारणों से महत्वपूर्ण होती हैं। ये चर्चाएं न सिर्फ दर्शकों को घटनाओं व मुद्दों के बारे में जागरूक करती हैं और जनमत तैयार करती हैं बल्कि लोकतंत्र में वाद-संवाद और विचार-विमर्श के लिए मंच मुहैया कराती हैं। वह आगे लिखते हैं कि न्यूज मीडिया इन चर्चाओं और बहसों के जरिये ही कुछ घटनाओं और मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय/क्षेत्रीय एजेंडे पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं।(आनंद प्रधान) हालांकि एजेंडे का प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देता, इसका प्रभाव दूरगामी भी होता है। वालग्रेव और वॉन एलिस्ट कहते हैं कि एजेंडा सेटिंग का यह मतलब नहीं होता है कि उसके प्रभाव स्पष्ट दीखने लगें बल्कि यह टॉपिक, मीडिया के प्रकार आैर इसके विस्तार के सही समुच्चय के तौर पर सामने आता है। (वालग्रेव एंड वॉन एलिस्ट, 2006)
वर्तमान में भारतीय न्यूज़ चैनलों की खबरों का विश्लेषण करें तो मैक्सवेल ई मैकॉम्ब और डोनाल्ड शॉ द्वारा जनसंचार के एजेंडा सेटिंग थ्योरी के निष्कर्ष साफ दिखाई देंगे। पिछले कुछ समय से जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं उनके जरिए न्यायपालिका से लेकर संसदीय प्रक्रिया तक के एजेंडे तय हुए हैं। सबसे ताजातरीन मामला आरुषि हत्याकांड का है। आज के दौर में ऐसा लगता है हमारा पूरा का पूरा मीडिया एजेंडा सेटिंग के सिद्धांत में उलझकर रह गया है। ट्रायल और ट्रीब्यूनल्स को किस तरह भारतीय मीडिया पेश करते हैं, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना ही नहीं, एजेंडा सेटिंग कई तरह के प्रभाव से भी जुड़े होते हैं मसलन फायदेमंद प्रभाव, खबरों को नजरअंदाज करना, खबरों के प्रकार और मीडिया गेटकीपिंग आदि। (डेयरिंग एंड रोजर्स, 1996:15)
पिछले दिनों एक साक्षात्कार में शेखर गुप्ता मीडिया एजेंडा थ्योरी की बारीकियों को बताते हुए कहा था कि मीडिया का मूल सवाल खड़े करना है लेकिन यह एजेंडा तब हो जाता है जब आप सवाल के जरिए किसी एजेंडे को खड़े करते हैं। इन मसलों पर अब विचार नहीं किया जाता। मसलन भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हुआ आंदोलन मीडिया को और व्यापक बनाते हैं। यदि मीडिया अच्छे कारणों को लेकर चल रही है और इससे समाज को बड़े पैमाने पर फायदा होगा तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि जेंडर की समानता को लेकर चलाया गया कंपेन काफी प्रभावशाली रहा था और ‘गुड एजेंडा सेटिंग” का उदाहरण है। साक्षरता, सूचना अधिकार आदि को लेकर चलाया गया कंपेन भी इसी का उदाहरण है। (शेखर गुप्ता)
इसी मसले पर सेवंती नैनन का मानना है कि मीडिया में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी मसले को हमारे दिमाग में भर दे। जैसे अन्ना आंदोलन को लेकर जो नॉन स्टॉफ कवरेज टीवी चैनलों के द्वारा किया गया, इससे हर कोई यह सोचने के लिए विवश हो गया कि कौन-सा राष्ट्रीय मसला महत्वपूर्ण है। जहां तक इसके नकारात्मक पहलू की बात है तो हर किसी को चोर कह देना आैर जेल में डालने की बात कहना, गलता है। ऐसे में यह ध्यान देना चाहिए कि सब कुछ टीआरपी ही नहीं होता। (सेवंती नैनन) गौरतलब है कि वरिष्ठ पत्रकार एन. राम ने सकारात्मक पक्ष को एजेंडा बिल्डिंग का नाम दिया है और उनका कहना है लोगों को एजेंडा सेटिंग और प्रोपगैंडा के साथ एजेंडा बिल्डिंग के बीच कनफ्यूज नहीं होनी चाहिए।
मालूम हो कि एजेंडा सेटिंग तीन तरीके से होता है, मीडिया एजेंडा, जो मीडिया बहस करता है। दूसरा पब्लिक एजेंडा जिसे व्यक्तिगत तौर पर लोग बातचीत करते हैं और तीसरा पॉलिसी एजेंडा जिसे लेकर पॉलिसी बनाने वाले विचार करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति काफी हद तक मीडिया को प्रभावित करती है। ऐसे में मीडिया कौन-सी खबरों को तवज्जो देता है, किस खबर का न्यूज वेल्यू किस तरह आंकता है और ऑडियंस की रुचि कैसी खबरों में है, आदि बातें मायने रखती हैं और फिर खबरों के प्रसारण के बाद उन्हीं बातों पर आम लोग अपनी राय कायम करते हैं।(मैक्सवेल)
आखिर किस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं और किस तरह के विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं, इनकी निगरानी करने वाली संस्थाएं कहां हैं। शुरुआती दौर में एजेंडा सेटिंग के तहत समाचारों का विश्लेषण पब्लिक ओपेनियन पोलिंग डाटा के साथ किया जाता था और राजनीतिक चुनाव के दौरान इसकी मदद से काफी कुछ तय हो जाता है। यही कारण है कि नोम चोमस्की कहते हैं कि इन मामलों में पीआर रिलेशन इंडस्ट्री, पब्लिक इंटलेक्चुअल, बिग थिंकर (जो ओप एड पेज पर छपते हैं) की भूमिका पर ध्यान देना होगा। हालांकि समय के साथ मीडिया के एजेंडे में बदलाव होता रहता है और ऐसा होना लाजिमी भी है क्योंकि एक बात तय होती है कि पत्रकारों की सहभागिता के साथ-साथ आम लोग किसी खास मुद्दे पर बात करते हैं और बहस करते हैं।
नोम चोमस्की कहते हैं कि मीडिया की जो भी कंपनियां है, सभी बड़ी कंपनियां हैं और मुनाफे की मलाई काटते हैं। उनका मानना है कि निजी अर्थव्यवस्था की शीर्षस्थ सत्ता संरचना का हिस्सा होती हैं और ये मीडिया कंपनियां मुख्य तौर पर ऊपर बैठे बड़े लोगों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर आप उन आकाओं के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। बड़ी मीडिया कंपनियां इसी आका तंत्र का एक हिस्सा है। (नोम चोमस्की) ऐसे में हमें विभिन्न एजेंडों, मीडिया की प्राथमिकता, आम लोगों और कानूनविदों के बीच अंतर को समझना होगा। किस तरह की खबरों को प्रमोट किया जाता है और किस तरह खबरों से खेला जा रहा है, वह भी एजेंडा सेटिंग में मायने रखते हैं। जैसे मीडिया कभी घरेलू मामलों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय मामलों को तवज्जो देने लगता है या फिर घरेलू मसलों में से किसी खास मसले की खबरें लगातार दिखाई जाती हैं। (रोजर्स एंड डेयरिंग, 1987)
बहरहाल, लोकतंत्र के इस लोक में मीडिया पर बाजार का जबर्दस्त प्रभाव है क्योंकि पेड न्यूज तो पैसे कमाने का साधन मात्र था लेकिन मीडिया एजेंडा तो पूरे तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके दायरे में सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं आते बल्कि पूरे लोक की सोच और समझ के साथ नियति निर्धारकों का मंतव्य भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मीडिया एजेंडे थ्योरी को समझना होगा और इसके जरिए पड़ने वाले प्रभाव पर भी बारीक नजर रखनी होगी।
-
प्रभावी समाचार लेखन के गुर
मनुष्य एक सामाजिक और जिज्ञासु प्राणी है। वह जिस समूह, समाज या वातावरण में रहता है उस के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक रहता है। अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकर उसे एक प्रकार के संतोष, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और कहीं न कहीं उसे उसकी इसी जिज्ञासा ने आज सृष्टि का सबसे विकसित प्राणी भी बनाया है। प्राचीन काल से ही उसने सूचनाओं को यहां से वहां पहुंचाने के लिए संदेशवाहकों, तोतों व घुड़सवारों की मदद लेने, सार्वजनिक स्थानों पर संदेश लिखने जैसे तमाम तरह के तरीकों, विधियों और माध्यमों को खोजा और विकसित किया। पत्र के जरिये समाचार प्राप्त करना भी एक पुराना माध्यम है जो लिपि और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद अस्तित्व में आया, और आज भी प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र रेडियो टेलिविजन, मोबाइल फोन व इंटरनेट समाचार प्राप्ति के आधुनिकतम संचार माध्यम हैं, जो छपाई, रेडियो व टेलीविजन जैसी वैज्ञानिक खोजों के बाद अस्तित्व में आए हैं।
समाचार की परिभाषा
सामान्य मानव गतिविधियों से इतर जो कुछ भी नया और खास घटित होता है, समाचार कहलाता है। मेले, उत्सव, दुर्घटनाएं, विपदा, सरकारी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सरकारी सुविधाओं का न मिलना सब समाचार हैं। विचार घटनाएं और समस्याओं से समाचार का आधार तैयार होता है। किसी भी घटना का अन्य लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके बारे में पैदा होने वाली सोच से समाचार की अवधारणा का विकास होता है। किसी भी घटना विचार और समस्या से जब काफी लोगों का सरोकार हो तो यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने योग्य है।
समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं तथा सूचनाओं और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरु होता है।
कुछ परिभाषाएंः
- किसी घटना की नई सूचना समाचार है: नवीन चंद्र पंत
- वह सत्य घटना या विचार जिसे जानने की अधिकाधिक लोगों की रूचि हो: नंद किशोर त्रिखा
- किसी घटना की असाधारणता की सूचना समाचार है: संजीव भनावत
- ऐसी ताजी या हाल की घटना की सूचना जिसके संबंध में लोगों को जानकारी न हो: रामचंद्र वर्मा
- जो हमारे चारों ओर घटित होता है, और हमें प्रभावित करता है, वह समाचार है।
- जिस घटना को पत्रकार लाता व लिखता तथा संपादक समाचार पत्र में छापता या दिखाने योग्य समझ कर टीवी में प्रसारित करता है, वह समाचार है। (क्योंकि यदि वह छपा ही नहीं या टीवी पर दिखाया ही नहीं गया तो फिर समाचार कहां रहा।)
- समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। कोई भी समाचार अगला समाचार आने पर इतिहास बन जाता है।
- समाचार सत्य, विश्वसनीय तथा कल्याणकारी होना चाहिए। जो समाज में दुर्भावना फैलाता हो अथवा झूठा हो, समाचार नहीं हो सकता। सत्यता समाचार का बड़ा गुण है।
- समाचार सूचना देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने वाला भी होना चाहिए।
- समाचार रोचक होना चाहिए। उसे जानने की लोगों में इच्छा होनी चाहिए।
- समाचार अपने पाठकों-श्रोताओं की छह ककार (5W & 1H, What, when, where, why, who and How) (क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ किसके साथ हुआ और कैसे हुआ,) की जिज्ञासाओं का शमन करता हो तथा नए दौर की नई जरूरतों के अनुसार भविष्य के संदर्भ में एक नए सातवें ककार-आगे क्या (6th W-What next) के बारे में भी मार्गदर्शन करे।
समाचार का सीधा अर्थ है-सूचना। मनुष्य के आस-पास और चारों दिशाओं में घटने वाली सूचना। समाचार को अंग्रेजी के न्यूज का हिन्दी समरुप माना जाता है। हालांकि ‘न्यूज’ (NEWS) शब्द इस तरह तो नहीं बना है, परंतु इत्तफाकन ही सही इसका अर्थ और प्रमुख कार्य चारों दिशाओं अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की सूचना देना भी है।
समाचार को बड़ा या छोटा बनाने वाले तत्वः
अक्सर हम समाचारों के छोटा या बढ़ा छपने पर चर्चा करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारा समाचार छपना ही चाहिए, और वह भी बड़े आकार में। साथ ही यह भी लगता है कि खासकर हमारी अरुचि के समाचार बेकार ही आवश्यकता से बड़े आकारों या बड़ी हेडलाइन में छपे होते हैं।
हिन्दी भावानुवाद
- प्रभाव-समाचार जितने अधिक लोगों से संबंधित होगा या उन्हें प्रभावित करेगा, उतना ही बड़ा होगा। किसी दुर्घटना में हताहतों की संख्या जितनी अधिक होगी, अथवा किसी दल, संस्था या समूह में जितने अधिक लोग होंगे, उससे संबंधित उतना ही बड़ा समाचार बनेगा।
- निकटता-समाचार जितना निकट से संबंधित होगा, उतना बड़ा होगा। दूर दुनिया की किसी बड़ी दुर्घटना से निकटवर्ती स्थान की छोटी घटना को भी अधिक स्थान मिल सकता है।
- विशिष्ट व्यक्ति (VIP)-जिस व्यक्ति से संबंधित खबर है, वह जितना विशिष्ट, जितना प्रभावी व प्रसिद्ध होगा, उससे संबंधित खबर उतनी ही बड़ी होगी। अलबत्ता, कई बार वास्तविक समाचार उस वीआईपी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दब कर रह जाती है।
- तात्कालिकता-कोई ताजा घटना बड़े आकार में छपती है, लेकिन उससे भी कुछ बड़ा न हो तो आगे उसके फॉलो-अप छोटे छपते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र छपते के दौरान आखिर समय में प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण खबरें, पहले से प्राप्त कम महत्वपूर्ण खबरों को हटाकर भी बड़ी छापी जाती हैं। पत्रिकाओं में भी छपने के दौरान सबसे लेटेस्ट महत्वपूर्ण समाचार बड़े आकार में छापा जाता है।
- एक्सक्लूसिव होना-यदि कोई समाचार केवल किसी एक समाचार पत्र के पास ही हो, तो वह उसे बड़े आकार में प्रकाशित करता है। लेकिन वही समाचार यदि सभी समाचार पत्रों में होने पर छोटे आकार में प्रकाशित होता है।
समाचार के मूल्य :
समाचार को बड़ा या छोटा यानी कम या अधिक महत्व का बनाने के लिए निम्न तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन्हें समाचार का मूल्य कहा जाता है।
1 व्यापकता: समाचार का विषय जितनी व्यापकता लिये होगा, उतने ही अधिक लोग उस समाचार में रुचि लेंगे, इसलिए वह बड़े आकार में छपेगा।
2 नवीनता: जिन बातों को मनुष्य पहले से जानता है वे बातें समाचार नही बनती। ऐसी बातें समाचार बनती है जिनमें कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी हो। इस प्रकार समाचार का बड़ा गुण है-नई सूचना, यानी समाचार में नवीनता होनी चाहिये। कोई समाचार कितना नया या तत्काल प्राप्त हुआ हो, उसे जानने की उतनी ही अधिक चाहत होती है। कोई भी पुरानी या पहले से पता जानकारी को दुबारा नहीं लेना चाहता। समाचार पत्रों के मामले में एक दिन पुराने समाचार को ‘रद्दी’ कहा जाता है, और उसका कोई मोल नहीं होता। वहीं टीवी के मामले में एक सेकेंड पहले प्राप्त समाचार अगले सेकेंड में ही बासी हो जाता है। कहा जाने लगा है-News this second and History on next second.
3 असाधारणता: हर समाचार एक नई सूचना होता है, परंतु यह भी सच है कि हर नई सूचना समाचार नही होती। जिस नई सूचना में कुछ असाधारणता होगी वही समाचार कहलायेगी। अर्थात नई सूचना में कुछ ऐसी असाधारणता होनी चाहिये जो उसमें समाचार बनने की अंतरनिहित शक्ति पैदा होती है। काटना कुत्ते का स्वभाव है। यह सभी जानते हैं। मगर किसी मनुष्य द्वारा कुत्ते को काटा जाना समाचार है। क्योंकि कुत्ते को काटना मनुष्य का स्वभाव नही है। जिस नई सूचना में असाधारणता नहीं होती वह समाचार नहीं लोकाचार कहलाता है।
4 सत्यता और प्रमाणिकता: समाचार में किसी घटना की सत्यता या तथ्यात्मकता होनी चाहिये। समाचार अफवाहों या उड़ी-उड़ायी बातों पर आधारित नही होते हैं। वे सत्य घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी होते हैं। सत्यता या तथ्यता होने से ही कोई समाचार विश्वसनीय और प्रमाणिक होते हैं।
5 रुचिपूर्णता: किसी नई सूचना में सत्यता होने से ही वह समाचार नहीं बन जाती है। उसमें अधिक लोगों की दिलचस्पी भी होनी चाहिये। कोई सूचना कितनी ही आसाधारण क्यों न हो अगर उसमें लोगों की रुचि न हो, तो वह सूचना समाचार नहीं बन पायेगी। कुत्ते द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को काटे जाने की सूचना समाचार नहीं बन पायेगी। कुत्ते द्वारा काटे गये व्यक्ति को होने वाले गंभीर बीमारी की सूचना समाचार बन जायेगी क्योंकि उस महत्वपूर्ण व्यक्ति में अधिकाधिक लोगों की दिलचस्पी हो सकती है।
6 प्रभावशीलता: समाचार दिलचस्प ही नही प्रभावशील भी होने चाहिये। हर सूचना व्यक्तियों के किसी न किसी बड़े समूह, बड़े वर्ग से सीधे या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़ी होती है। अगर किसी घटना की सूचना समाज के किसी समूह या वर्ग को प्रभावित नही करती तो उस घटना की सूचना का उनके लिये कोई मतलब नही होगा।
7 स्पष्टता: एक अच्छे समाचार की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिये। किसी समाचार में दी गयी सूचना कितनी ही नई, कितनी ही असाधारण, कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन अगर वह सूचना सरल और स्पष्ट भाषा में न हो तो वह सूचना बेकार साबित होगी। क्योंकि ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पायेंगे। इसलिये समाचार की भाषा सीधी और स्पष्ट होनी चाहिये।
समाचार लेखन और संपादन
परिचय: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए वह एक जिज्ञासु प्राणी है। मनुष्य जिस समुह में, जिस समाज में और जिस वातावरण में रहता है वह उस बारे में जानने को उत्सुक रहता है। अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकर उसे एक प्रकार के संतोष, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिये उसने प्राचीन काल से ही तमाम तरह के तरीकों, विधियों और माध्यमों को खोजा और विकसित किया। पत्र के जरिये समाचार प्राप्त करना इन माध्यमों में सर्वाधिक पुराना माध्यम है जो लिपि और डाक व्यवस्था के विकसित होने के बाद अस्तित्व में आया। पत्र के जरिये अपने प्रियजनों मित्रों और शुभाकांक्षियों को अपना समाचार देना और उनका समाचार पाना आज भी मनुष्य के लिये सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। समाचारपत्र रेडियो टेलिविजन समाचार प्राप्ति के आधुनिकतम साधन हैं जो मुद्रण रेडियो टेलीविजन जैसी वैज्ञानिक खोज के बाद अस्तित्व में आये हैं।
समाचार की परिभाषा :
लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर ही करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं। मेलों और उत्सव में वे साथ होते हैं। दुर्घटनाओं और विपदाओं के समय वे साथ ही होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव कस्बे या शहर की कॉलोनी में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। विचार घटनाएं और समस्यों से ही समाचार का आधार तैयार होता है। लोग अपने समय की घटनाओं रूझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं। उनपर विचार करते हैं और इन सबको लेकर कुछ करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन प्रक्रिया के केन्द्र में इनके कारणों प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। समाचार के रूप में इनका महत्व इन्हीं कारकों से निर्धारित होना चाहिये। किसी भी चीज का किसी अन्य पर पड़ने वाले प्रभाव और इसके बारे में पैदा होने वाली सोच से ही समाचार की अवधारणा का विकास होता है। किसी भी घटना विचार और समस्या से जब काफी लोगों का सरोकार हो तो यह कह सकतें हैं कि यह समाचार बनने योग्य है।
समाचार किसी बात को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं के सबसे पहले बताया जाता है और उसके बाद घटते हुये महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरु होता है।
- किसी नई घटना की सूचना ही समाचार है : डॉ निशांत सिंह
- किसी घटना की नई सूचना समाचार है : नवीन चंद्र पंत
- वह सत्य घटना या विचार जिसे जानने की अधिकाधिक लोगों की रूचि हो : नंद किशोर त्रिखा
- किसी घटना की असाधारणता की सूचना समाचार है : संजीव भनावत
- ऐसी ताजी या हाल की घटना की सूचना जिसके संबंध में लोगों को जानकारी न हो : रामचंद्र वर्मा
समाचार के मूल्य :
1 व्यापकता : समाचार का सीधा अर्थ है-सूचना। मनुष्य के आस दृ पास और चारों दिशाओं में घटने वाली सूचना। समाचार को अंग्रेजी के न्यूज का हिन्दी समरुप माना जाता है। न्यूज का अर्थ है चारों दिशाओं अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की सूचना। इस प्रकार समाचार का अर्थ पुऐ चारों दिशाओं में घटित घटनाओं की सूचना।
2 नवीनता: जिन बातों को मनुष्य पहले से जानता है वे बातें समाचार नही बनती। ऐसी बातें समाचार बनती है जिनमें कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी हो। इस प्रकार समाचार का मतलब हुआ नई सूचना। अर्थात समाचार में नवीनता होनी चाहिये।
3 असाधारणता: हर नई सूचना समाचार नही होती। जिस नई सूचना में समाचारपन होगा वही नई सूचना समाचार कहलायेगी। अर्थात नई सूचना में कुछ ऐसी असाधारणता होनी चाहिये जो उसमें समाचारपन पैदा करे। काटना कुत्ते का स्वभाव है। यह सभी जानते हैं। मगर किसी मनुष्य द्वारा कुत्ते को काटा जाना समाचार है क्योंकि कुत्ते को काटना मनुष्य का स्वभाव नही है। कहने का तात्पर्य है कि नई सूचना में समाचार बनने की क्षमता होनी चाहिये।
4 सत्यता और प्रमाणिकता : समाचार में किसी घटना की सत्यता या तथ्यात्मकता होनी चाहिये। समाचार अफवाहों या उड़ी-उड़ायी बातों पर आधारित नही होते हैं। वे सत्य घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी होते हैं। सत्यता या तथ्यता होने से ही कोई समाचार विश्वसनीय और प्रमाणिक होते हैं।
5 रुचिपूर्णता: किसी नई सूचना में सत्यता और समाचारपन होने से हा वह समाचार नहीं बन जाती है। उसमें अधिक लोगों की दिसचस्पी भी होनी चाहिये। कोई सूचना कितनी ही आसाधरण क्यों न हो अगर उसमे लोगों की रुचि नही है तो वह सूचना समाचार नहीं बन पायेगी। कुत्ते द्वारा किसी सामान्य व्यक्ति को काटे जाने की सूचना समाचार नहीं बन पायेगी। कुत्ते द्वारा काटे गये व्यक्ति को होने वाले गंभीर बीमारी की सूचना समाचार बन जायेगी क्योंकि उस महत्वपूर्ण व्यक्ति में अधिकाधिक लोगों की दिचस्पी हो सकती है।
6 प्रभावशीलता : समाचार दिलचस्प ही नही प्रभावशील भी होने चाहिये। हर सूचना व्यक्तियों के किसी न किसी बड़े समूह, बड़े वर्ग से सीधे या अप्रत्यक्ष रुप से जुड़ी होती है। अगर किसी घटना की सूचना समाज के किसी समूह या वर्ग को प्रभावित नही करती तो उस घटना की सूचना का उनके लिये कोई मतलब नही होगा।
7 स्पष्टता : एक अच्छे समाचार की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिये। किसी समाचार में दी गयी सूचना कितनी ही नई, कितनी ही असाधारण, कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो अगर वह सूचना सरल और स्पष्ट भाष में न हो तो वह सूचना बेकार साबित होगी क्योंकि ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पायेंगे। इसलिये समाचार की भाषा सीधीऔर स्पष्ट होनी चाहिये।उल्टा पिरामिड शैली
ऐतिहासिक विकास :
इस सिद्धांत का प्रयोग 19 वीं सदी के मध्य से शुरु हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृहयुद्ध के दौरान हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेश के जरिये भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवायें अनियमित, महंगी और दुर्लभ थी। यही नहीं कई बार तकनीकी कारणों से टेलीग्राफ सेवाओं में बाधा भी आ जाती थी। इसलिये संवाददाताओं को किसी खबर कहानी लिखने के बजाये संक्षेप में बतानी होती थी और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाओं की जानकारी पहली कुछ लाइनों में ही देनी पड़ती थी।
लेखन प्रक्रिया :
उल्टा पिरामिड सिद्धांत : उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। यह समाचार लेखन का सबसे सरल, उपयोगी और व्यावहारिक सिद्धांत है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा या कहनी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उलट है। इसमें किसी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों या जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहनी या उपन्यास में क्लाइमेक्स सबसे अंत में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के निचले हिस्से में नहीं होती है और इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे उपरी हिस्से में होती है और घटते हुये क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनायें सबसे निचले हिस्से में होती है।समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गये समाचारों के सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः तीन हिस्सों में विभाजित किया जाता है-मुखड़ा या इंट्रो या लीड, बॉडी और निष्कर्ष या समापन। इसमें मुखड़ा या इंट्रो समाचार के पहले और कभी-कभी पहले और दूसरे दोनों पैराग्राफ को कहा जाता है। मुखड़ा किसी भी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी आती है, जिसमें महत्व के अनुसार घटते हुये क्रम में सूचनाओं और ब्यौरा देने के अलावा उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया जाता है। सबसे अंत में निष्कर्ष या समापन आता है। समाचार लेखन में निष्कर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है और न ही समाचार के अंत में यह बताया जाता है कि यहां समाचार का समापन हो गया है।
मुखड़ा या इंट्रो या लीड : उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मुखड़ा लेखन या इंट्रो या लीड लेखन है। मुखड़ा समाचार का पहला पैराग्राफ होता है, जहां से कोई समाचार शुरु होता है। मुखड़े के आधार पर ही समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। एक आदर्श मुखड़ा में किसी समाचार की सबसे महत्वपूर्ण सूचना आ जानी चाहिये और उसे किसी भी हालत में 35 से 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये। किसी मुखड़े में मुख्यतः छह सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाती है दृ क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, क्यों और कैसे हुआ है। आमतौर पर माना जाता है कि एक आदर्श मुखड़े में सभी छह ककार का जवाब देने के बजाये किसी एक मुखड़े को प्राथमिकता देनी चाहिये। उस एक ककार के साथ एक-दो ककार दिये जा सकते हैं।
बॉडी: समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े में उल्लिखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी में होती है। किसी समाचार लेखन का आदर्श नियम यह है कि किसी समाचार को ऐसे लिखा जाना चाहिये, जिससे अगर वह किसी भी बिन्दु पर समाप्त हो जाये तो उसके बाद के पैराग्राफ में ऐसा कोई तथ्य नहीं रहना चाहिये, जो उस समाचार के बचे हुऐ हिस्से की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अपने किसी भी समापन बिन्दु पर समाचार को पूर्ण, पठनीय और प्रभावशाली होना चाहिये। समाचार की बॉडी में छह ककारों में से दो क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कोई घटना कैसे और क्यों हुई, यह जानने के लिये उसकी पृष्ठभूमि, परिपेक्ष्य और उसके व्यापक संदर्भों को खंगालने की कोशिश की जाती है। इसके जरिये ही किसी समाचार के वास्तविक अर्थ और असर को स्पष्ट किया जा सकता है।
निष्कर्ष या समापन : समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गये हैं बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिये। समाचार में तथ्यों और उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिये कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले।
समाचार संपादन :
समाचार संपादन का कार्य संपादक का होता है। संपादक प्रतिदिन उपसंपादकों और संवाददाताओं के साथ बैठक कर प्रसारण और कवरेज के निर्देश देते हैं। समाचार संपादक अपने विभाग के समस्त कार्यों में एक रूपता और समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
संपादन की प्रक्रिया :
रेडियो में संपादन का कार्य प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त होता है।
1. विभिन्न श्रोतों से आने वाली खबरों का चयन
2. चयनित खबरों का संपादन : रेडियो के किसी भी स्टेशन में खबरों के आने के कई स्रोत होते हैं। जिनमें संवाददाता, फोन, जनसंपर्क, न्यूज एजेंसी, समाचार पत्र और आकाशवाणी मुख्यालय प्रमुख हैं। इन स्रोतों से आने वाले समाचारों को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खबरों का चयन किया जाता है। यह कार्य विभाग में बैठे उपसंपादक का होता है। उदाहरण के लिए यदि हम आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र के लिए समाचार बुलेटिन तैयार कर रहे हैं तो हमें लोकल याप्रदेश स्तर की खबर को प्राथमिकता देनी चाहिए। तत् पश्चात् चयनित खबरों का भी संपादन किया जाना आवश्यक होता है। संपादन की इस प्रक्रिया में बुलेटिन की अवधि को ध्यान में रखना जरूरी होता है। किसी रेडियो बुलेटिन की अवधि 5, 10 या अधिकतम 15 मिनट की होती है।
संपादन के महत्वपूर्ण चरण :
1. समाचार आकर्षक होना चाहिए। 2. भाषा सहज और सरल हो।3. समाचार का आकार बहुत बड़ा और उबाऊ नहीं होना चाहिए।4. समाचार लिखते समय आम बोल-चाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।5. शीर्षक विषय के अनुरूप होना चाहिए।
6. समाचार में प्रारंभ से अंत तक तारतम्यता और रोचकता होनी चाहिए।
7. कम शब्दों में समाचार का ज्यादा से ज्यादा विवरण होना चाहिए।
8. रेडियो बुलेटिन के प्रत्येक समाचार में श्रोताओं के लिए सम्पूर्ण जानकारी होना
चाहिये ।
9. संभव होने पर समाचार स्रोत का उल्लेख होना चाहिए।
10. समाचार छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए।
11. रेडियो के सभी श्रोता पढ़े लिखे नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखकर भाषा और शब्दों का चयन किया जाना चाहिए।
12. रेडियो श्रव्य माध्यम है अतः समाचार की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि एक ही बार सुनने पर समझ आ जाए।
13. समाचार में तात्कालिकता होना अत्यावश्यक है। पुराना समाचार होने पर भी इसे अपडेट कर प्रसारित करना चाहिए।
14. समाचार लिखते समय व्याकरण और चिह्नो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके।
समाचार संपादन के तत्व :
संपादन की दृष्टि से किसी समाचार के तीन प्रमुख भाग होते हैं-
1. शीर्षक- किसी भी समाचार का शीर्षक उस समाचार की आत्मा होती है। शीर्षक के माध्यम से न केवल श्रोता किसी समाचार को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, अपितु शीर्षकों के द्वारा वह समाचार की विषय-वस्तु को भी समझ लेता है। शीर्षक का विस्तार समाचार के महत्व को दर्शाता है। एक अच्छे शीर्षक में निम्नांकित गुण पाए जाते हैं-
1. शीर्षक बोलता हुआ हो। उसके पढ़ने से समाचार की विषय-वस्तु का आभास हो जाए।
2. शीर्षक तीक्ष्ण एवं सुस्पष्ट हो। उसमें श्रोताओं को आकर्षित करने की क्षमता हो।
3. शीर्षक वर्तमान काल में लिखा गया हो। वर्तमान काल मे लिखे गए शीर्षक घटना की ताजगी के द्योतक होते हैं।
4. शीर्षक में यदि आवश्यकता हो तो सिंगल-इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। डबल इनवर्टेड कॉमा अधिक स्थान घेरते हैं।
5. अंग्रेजी अखबारों में लिखे जाने वाले शीर्षकों के पहले ‘ए’ ‘एन’, ‘दी’ आदि भाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यही नियम हिन्दी में लिखे शीर्षकों पर भी लागू होता है।
6. शीर्षक को अधिक स्पष्टता और आकर्षण प्रदान करने के लिए सम्पादक या उप-सम्पादक का सामान्य ज्ञान ही अन्तिम टूल या निर्णायक है।
7. शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक हो तो उसे एक ही पंक्ति में लिखा जाए। नाम को तोड़कर दो पंक्तियों में लिखने से शीर्षक का सौन्दर्य समाप्त हो जाता है।
8. शीर्षक कभी भी कर्मवाच्य में नहीं लिखा जाना चाहिए।
2. आमुख- आमुख लिखते समय ‘पाँच डब्ल्यू’ तथा एक-एच के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अर्थात् आमुख में समाचार से संबंधित छह प्रश्न-Who, When, Where, What और How का अंतर पाठक को मिल जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान में इस सिद्धान्त का अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। आज छोटे-से-छोटे आमुख लिखने की प्रवृत्ति तेजी पकड़ रही है। फलस्वरूप इतने प्रश्नों का उत्तर एक छोटे आमुख में दे सकना सम्भव नहीं है। एक आदर्श आमुख में 20 से 25 शब्द होना चाहिए।
3. समाचार का ढाँचा- समाचार के ढाँचे में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः कम से कम 150 शब्दों तथा अधिकतम 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। श्रोताओं को अधिक लम्बे समाचार आकर्षित नहीं करते हैं।
समाचार सम्पादन में समाचारों की निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है-
1. समाचार किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता है।
2. समाचार नीति के अनुरूप हो।
3. समाचार तथ्याधारित हो।
4. समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुरूप विस्तार देना।
5. समाचार की भाषा पुष्ट एवं प्रभावी है या नहीं। यदि भाषा नहीं है तो उसे पुष्ट बनाएँ।
6. समाचार में आवश्यक सुधार करें अथवा उसको पुर्नलेखन के लिए वापस कर दें।
7. समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो।
8. अनावश्यक अथवा अस्पस्ट शब्दों को समाचार से हटा दें।
9. ऐसे समाचारों को ड्राप कर दिया जाए, जिनमें न्यूज वैल्यू कम हो और उनका उद्देश्य किसी का प्रचार मात्र हो।
10. समाचार की भाषा सरल और सुबोध हो।
11. समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न हो।
12. वाक्यों में आवश्यकतानुसार विराम, अद्र्धविराम आदि संकेतों का समुचित प्रयोग हो।
13. समाचार की भाषा में एकरूपता होना चाहिए।
14. समाचार के महत्व के अनुसार बुलेटिन में उसको स्थान प्रदान करना।
समाचार-सम्पादक की आवश्यकताएँ :
एक अच्छे सम्पादक अथवा उप-सम्पादक के लिए आवश्यक होता है कि वह समाचार जगत में अपने ज्ञान-वृद्धि के लिए निम्नांकित पुस्तकों को अपने संग्रहालय में अवश्य रखें-
1. सामान्य ज्ञान की पुस्तकें।
2. एटलस।
3. शब्दकोश।
4. भारतीय संविधान।
5. प्रेस विधियाँ।
6. इनसाइक्लोपीडिया।
7. मन्त्रियों की सूची।
8. सांसदों एवं विधायकों की सूची।
9. प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की सूची।
10. ज्वलन्त समस्याओं सम्बन्धी अभिलेख।
11. भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) पुस्तक।
12. दिवंगत नेताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्बन्धित अभिलेख।
13. महत्वपूर्ण व्यक्तियों व अधिकारियों के नाम, पते व फोन नम्बर।
14. पत्रकारिता सम्बन्धी नई तकनीकी पुस्तकें।
15. उच्चारित शब्द
समाचार के स्रोत :
कभी भी कोई समाचार निश्चित समय या स्थान पर नहीं मिलते। समाचार संकलन के लिए संवाददाताओं को फील्ड में घूमना होता है। क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी घटना घट सकती है, जो एक महत्वपूर्ण समाचार बन सकती है। समाचार प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत निम्न हैं-
1. संवाददाता- टेलीविजन और समाचार-पत्रों में संवाददाताओं की नियुक्ति ही इसलिए होती हैकि वह दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन करें और उन्हें समाचार का स्वरूप दें।
2. समाचार समितियाँ- देश-विदेश में अनेक ऐसी समितियाँ हैं जो विस्तृत क्षेत्रों के समाचारों को संकलित करके अपने सदस्य अखबारों और टीवी को प्रकाशन और प्रसारण के लिए प्रस्तुत करती हैं। मुख्य समितियों में पी.टी.आई. (भारत), यू.एन.आई. (भारत), ए.पी. (अमेरिका), ए.एफ.पी. (फ्रान्स), रॉयटर (ब्रिटेन)।
3. प्रेस विज्ञप्तियाँ- सरकारी विभाग, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठान तथा अन्य व्यक्ति या संगठन अपने से सम्बन्धित समाचार को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखकर ब्यूरो आफिस में प्रसारण के लिए भिजवाते हैं। सरकारी विज्ञप्तियाँ चार प्रकार की होती हैं।
(अ) प्रेस कम्युनिक्स- शासन के महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस कम्युनिक्स के माध्यम से समाचार-पत्रों को पहुँचाए जाते हैं। इनके सम्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रिलीज के बाएँ ओर सबसे नीचे कोने पर सम्बन्धित विभाग का नाम, स्थान और निर्गत करने की तिथि अंकित होती है। जबकि टीवी के लिए रिर्पोटर स्वयं जाता है
(ब) प्रेस रिलीज-शासन के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस रिलीज के द्वारा समाचार-पत्र और टी.वी. चैनल के कार्यालयों को प्रकाशनार्थ भेजे जाते हैं।
(स) हैण्ड आउट- दिन-प्रतिदिन के विविध विषयों, मन्त्रालय के क्रिया-कलापों की सूचना हैण्ड-आउट के माध्यम से दी जाती है। यह प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।
(द) गैर-विभागीय हैण्ड आउट- मौखिक रूप से दी गई सूचनाओं को गैर-विभागीय हैण्ड आउट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।
4. पुलिस विभाग- सूचना का सबसे बड़ा केन्द्र पुलिस विभाग का होता है। पूरे जिले में होनेवाली सभी घटनाओं की जानकारी पुलिस विभाग की होती है, जिसे पुलिसकर्मी-प्रेस के प्रभारी संवाददाताओं को बताते हैं।
5. सरकारी विभाग- पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभाग समाचारों के केन्द्र होते हैं। संवाददाता स्वयं जाकर खबरों का संकलन करते हैं अथवा यह विभाग अपनीउपलब्धियों को समय-समय पर प्रकाशन हेतु समाचार-पत्र और टीवी कार्यालयों को भेजते रहते हैं।
6. चिकित्सालय- शहर के स्वास्थ्य संबंधी समाचारों के लिए सरकारी चिकित्सालयों अथवा बड़े प्राइवेट अस्पतालों से महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।
7. कॉरपोरेट आफिस- निजी क्षेत्र की कम्पनियों के आफिस अपनी कम्पनी से सम्बन्धित समाचारों को देने में दिलचस्पी रखते हैं। टेलीविजन में कई चैनल व्यापार पर आधारित हैं।
8. न्यायालय- जिला अदालतों के फैसले व उनके द्वारा व्यक्ति या संस्थाओं को दिए गए निर्देश समाचार के प्रमुख स्रोत हैं।
9. साक्षात्कार- विभागाध्यक्षों अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार समाचार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
10. समाचारों का फॉलो-अप या अनुवर्तन- महत्वपूर्ण घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट रुचिकर समाचार बनते हैं। दर्शक चाहते हैं कि बड़ी घटनाओं के सम्बन्ध में उन्हें सविस्तार जानकारी मिलती रहे। इसके लिए संवाददाताओं को घटनाओं की तह तक जाना पड़ता है।
11. पत्रकार वार्ता- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान अक्सर अपनी उपलब्धियों को प्रकाशित करने के लिए पत्रकारवार्ता का आयोजन करते हैं। उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य समृद्ध समाचारों को जन्म देते हैं।
उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त सभा, सम्मेलन, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम,विधानसभा, संसद, मिल, कारखाने और वे सभी स्थल जहाँ सामाजिक जीवन की घटना मिलती है, समाचार के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।
सम्पादन व सम्पादकीय विभाग
सम्पादन व सम्पादकीय विभाग पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका अथवा अन्य जनसंचार माध्यम का स्तर उसके सम्पादन व सम्पादकीय विभाग पर निर्भर करता है। सम्पादकीय विभाग जितना सक्रिय, योग्य व व्यावहारिक होगा, वह मीडिया उतना ही अधिक प्रचलित व ख्याति प्राप्त होगा। इसलिए पत्रकारिता को समझने के लिए इस कार्य व विभाग की जानकारी होना अति आवश्यक है।
किसी भी समाचार-पत्र या पत्रिका की प्रतिष्ठा, उसका नाम, उसकी छवि उसके संपादक के नाम के साथ बनती-बिगड़ती है। सम्पादक किसी अच्छी फिल्म को बनाने वाले उस निर्देशक की तरह होता है, जिसे हर बार एक अच्छा अखबार या पत्रिका बनानी होती है। इस काम में उसकी प्रतिभा और उसकी कबिलियत तो महत्व रखती ही है, उसकी टीम और उसके सहयोगियों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इस सम्पादकीय टीम के साथ-साथ जो एक अन्य महत्वपूर्ण चीज होती है। वह है पत्र या पत्रिका का सम्पादकीय पृष्ठ। पत्रिकाओं में जहां सम्पादकीय पृष्ठ प्रारम्भ में होता है वहीं अखबारों में इसकी जगह बीच के पृष्ठों में कहीं होती है।
कुल मिला कर संपादक, सम्पादकीय विभाग और सम्पादकीय पृष्ठ किसी भी पत्र-पत्रिका की सफलता और श्रेष्ठता के सूत्रधार होते हैं। समाचार पत्र-पत्रिकाओं के कार्यालयों में समाचार विभिन्न श्रोतों, जैसे संवाददाताओं तथा एजेंसियों से प्राप्त होते हैं। कई बार विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों इत्यादि की ओर से भी प्रेस रिलीज दी जाती हैं। इन सबको समाचार कक्ष में ‘डेस्क’ पर एकत्र किया जाता है। सारी सामग्री अलग-अलग तरह की होती है। उप-सम्पादक इन सब प्राप्त समाचार-सामग्री की छंटनी, वर्गीकरण, आवश्यक सुधार करते हैं, साथ ही काटते-छांटते या विस्तृत करते हैं और उन्हें प्रकाशन योग्य बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ‘सम्पादन’ के अन्तर्गत आती है।
सम्पादकीय विभाग ‘समाचार पत्र का हृदय’ कहा जा सकता है। कुशल सम्पादन पत्र को जीवन्त और प्राणवान बना देता है। सम्पादकीय विभाग मुख्यतः समाचार, लेख, फीचर, कार्टून, स्तम्भ, सम्पादकीय एवं सम्पादकीय टिप्पणियों आदि सारे कार्यों से जुड़ा होता है। यह विभाग सम्पादक या प्रधान सम्पादक के नेतृत्व में कार्य करता है। इनकी सहायता के लिए कार्य करने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं, जो सहायक सम्पादक, संयुक्त सम्पादक, समाचार सम्पादक, विशेष सम्पादक व उप सम्पादक इत्यादि होते हैं, जो समाचार संकलन से लेकर सम्पादन की विविध प्रक्रियाओं से विभिन्न स्तरों पर सम्बद्ध होते हैं।
किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका में सम्पादन का कार्य एक चूनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे पत्र-पत्रिका का सम्पादन मण्डल पूर्ण करता है। इस सम्पादन मण्डल का मुखिया सम्पादक कहलाता है। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी सामग्री की उपयोगिता व महत्व के लिए सम्पादक ही जिम्मेदार होता है। सम्पादक मण्डल द्वारा पत्र में एक पृष्ठ पर नवीन व समसामयिक विचार, टिप्पणी, लेख एवं समीक्षाएं लिखी जाती हैं, जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य समसामयिक विषयों पर आधारित हो सकती है। इन टिप्पणियों को सम्पादकीय कहते हैं, और जिस पृष्ठ पर पर यह लिखी जाती हैं, उसे सम्पादकीय पृष्ठ कहते हैं। किसी भी समाचार पत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है।
हालांकि वर्तमान दौर में समाचार पत्रों में सम्पादक की भूमिका एक रचनाकार पत्रकार से बदलकर प्रबन्धक पत्रकार जैसी हो गयी है मगर इसके बाद भी सम्पादक का महत्व खत्म नहीं हुआ है और आज भी किसी भी पत्रकार के लिए संपादक बनना एक सपने की तरह ही है।सम्पादन एवं सम्पादकीय किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं। सम्पादन का तात्पर्य किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका के लिए समाचारों व लेखों का चयन, उनको क्रमबद्ध करना, सामग्री का प्रस्तुतीकरण निश्चित करना, संशोधित करना, उनकी भाषा, व्याकरण और शैली में सुधार एवं विश्लेषण करना और उन्हें पाठकों के लिए पठनीय बनाना है।
सम्पादन कार्य को सम्पादित करने हेतु सम्पादक के नेतृत्व में कार्य करने वाली टीम को सम्पादकीय मण्डल या सम्पादकीय विभाग कहा जाता है। सम्पादकीय विभाग के प्रत्येक सदस्य का कार्य महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होता है।
सम्पादकीय विभाग में एक स्टिंगर से लेकर पत्र के सम्पादक तक के अपने-अपने उत्तरदायित्व व योग्यतायें होती हैं। जिनका निर्वाह करते हुये वे एक समाचार पत्र-पत्रिका को पाठकों के बीच लोकप्रिय व पठनीय बनाकर प्रस्तुत करते हैं।सम्पादन का अर्थ
‘सम्पादन’ का शाब्दिक अर्थ कार्य सम्पन्न करना है। किसी भी कार्य को वह अंतिम रूप देना, जिस रूप में उसे प्रस्तुत करना हो, यह ही सम्पादन कहलाता है। किसी भी समाचार पत्र-पत्रिका में समाचार श्रोतों से समाचार एकत्रित कर उसे पाठकों के लिए पठनीय बनाना ही सम्पादन है।
किसी पुस्तक का विषय या सामयिक पत्र के लेख आदि अच्छी तरह देखकर, उनकी त्रुटियां आदि दूर करके और उनका ठीक क्रम लगा कर उन्हें प्रकाशन के योग्य बनाना भी संपादन है। वास्तव में सम्पादन एक कला है, जिसमें समाचारों, लेखों व किसी समाचार पत्र-पत्रिका में प्रकाशित की जाने वाली सभी तरह की सामग्री का चयन, उसको क्रमबद्ध करना, सामग्री का प्रस्तुतीकरण निश्चित करना, उसे संशोधित करना, उसकी भाषा, व्याकरण और शैली में सुधार करना, विश्लेषण करना आदि सभी कार्य सम्मिलित हैं। पृष्ठों की साज-सज्जा करना, शुद्ध और आकर्षक मुद्रण कराने में सहयोग करना भी ‘सम्पादन’ का अंग है।
पत्रकारिता सन्दर्भ कोश में ‘सम्पादन’ का अर्थ इस प्रकार बताया गया हैः ‘‘अभीष्ट मुद्रणीय सामग्री (समाचारों, लेखों एवं अन्य विविध रचनाओं आदि) का चयन, क्रम-निर्धारण, मुद्रणानुरूप संशोधन-परिमार्जन, साज-सज्जा तथा उसे प्रकाशन-योग्य बनाने के लिए अन्य अपेक्षित प्रक्रियाओं को सम्पन्न करना। आवश्यकता पड़ने पर मुद्रणीय सामग्री से सम्बन्धित प्रस्तावना, पृष्ठभूमि सम्बन्धी वक्तव्य अथवा अभीष्ट टिप्पणी आदि प्रस्तुत करना भी सम्पादन के अन्तर्गत आता है।’’
जे.एडवर्ड मरे के अनुसार – “Because copy editing is an art, the most important ingredient after training and talent, is strong motivation. The copy editor must care. Not only should he know his job, he must love it. Every edition, every day. No art yields to less than maximum effort. The copy editor must be motivated by a fierce professional pride in the high quality of editing.’’‘सम्पादन’ आसान काम नहीं है। यह अत्यन्त परिश्रम-साध्य एवं बौद्धिक कार्य है। इसमें मेधा, निपुणता और अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसलिए सम्पादन कार्य करने वाले व्यक्ति को न केवल सावधानी रखनी होती है, बल्कि अपनी क्षमताओं, अभिरूचि तथा निपुणता का पूरा-पूरा उपयोग भी करना होता है। उसे अपने कार्य का पूरा ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कार्य के प्रति एकनिष्ठ लगाव भी होना चाहिए।
समाचार-पत्र कार्यालय में विभिन्न श्रोतों से समाचार प्राप्त होते हैं। संवाददाता (रिपोर्टर), एजेंसियां व कई बार विभिन्न संस्थाओं, राजनीतिक दलों इत्यादि की ओर से प्रेस रिलीज प्रेषित किए जाते हैं। इन सबको समाचार-कक्ष में ‘डेस्क’ पर एकत्र किया जाता है। सारी सामग्री अलग-अलग तरह की होती है। उप-सम्पादक इन सब प्राप्त समाचार-सामग्री की छंटनी व वर्गीकरण करते हैं, तथा उनमें यथावश्यक उनमें सुधार करते हैं, काटते-छांटते या विस्तृत करते हैं और उन्हें प्रकाशन योग्य बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ‘सम्पादन’ के अन्तर्गत आती है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक श्रोतों से प्राप्त समाचारों को संघनित कर मिलाना, एक आदर्श समाचार-कथा (न्यूज स्टोरी) तैयार करना, आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनर्लेखन करना इत्यादि बातें सम्मिलित हैं। सम्पादक केवल काट-छांट तक ही सीमित नहीं हैं, उसमें अनुवाद करना, समाचारों को एक तरह से अपने रंग में रंगना भी शामिल है। वैचारिक दृष्टि से, विशेष रूप से कई बार समाचार-पत्र की रीति-नीति के अनुसार सम्पादक के जरिए उनमें वैचारिक चमक भी पैदा की जाती है।
अतः सम्पादन पत्रकारिता में वह कला है जो समाचार को पाठकों के लिए रूचिकर, मनोरंजक, तथ्यपूर्ण व ज्ञानवर्धक बनाकर परोसती है।
विज्ञापन के माध्यम एवं प्रकार
विज्ञापन का उद्देश्य अपने मकसद की पूर्ति के लिए अपने संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक संप्रेषित करना है। ताकि विज्ञापनकर्ता को अधिक से अधिक लाभ हो सके। विज्ञापन करने वाला यानी विज्ञापनकर्ता अपना संदेश देने के लिए विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करता है। विज्ञापन का संदेश लोगों तक पहुचाने के लिए विज्ञापनकर्ता जिन प्रमुख चीजों पर निर्भर रहता है उनमें बाजार, विज्ञापन का संदेश, विज्ञापन की बनावट के साथ-साथ विज्ञापन के माध्यम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
विज्ञापन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विज्ञापन का संदेश किस उपभोक्ता समूह अथवा वर्ग के लिए तैयार किया गया है? किस वर्ग अथवा उपभोक्ता समूह को लक्ष्य किया जाना है ? और विज्ञापनकर्ता विज्ञापन के जरिए क्या हासिल करना चाहता है ? लेकिन इन सब बातों के अलावा विज्ञापन की सफलता एक और चीज पर भी निर्भर करती है, वह चीज है विज्ञापन का माध्यम। विज्ञापन माध्यम का आशय विज्ञापन को दर्शक, पाठक, श्रोता या उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले माध्यम से है। अलग-अलग परिस्थितियों मे यह माध्यम अलग-अलग प्रकार के होते हैं और किसी विज्ञापन को किस प्रकार के लक्ष्य समूह तक पहुँचाना है, इस बात की सफलता सही माध्यम के चयन पर ही निर्भर करती है।
वस्तुतः माध्यम विज्ञापन के कथ्य अथवा संदेश और विज्ञापन के उपभोक्ता अथवा लक्ष्य समूह के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। विज्ञापन का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उसका माध्यम सही हो। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को दिल्ली से मुम्बई जाना हो और उसके पास काम के लिए दो तीन घंटे का ही समय हो तो ऐसी स्थिति में वह यदि सड़क के माध्यम से अथवा रेल के माध्यम से यात्रा करेगा तो निर्धारित समय में लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि वह हवाई मार्ग को माध्यम बनाएगा तो निश्चित रूप से वह निर्धारित समय में अपनी यात्रा पूरी कर पाएगा और लक्ष्य तक समय पर पहुँच जाएगा। ठीक यही बात विज्ञापन के बारे में भी लागू होती है। माध्यम सही नहीं होगा तो विज्ञापन सही जगह तक पहुंच ही नहीं सकेगा।
विज्ञापन को माध्यम के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य, संदेश, बनावट और प्रसार क्षेत्र के आधार पर भी विज्ञापनों के अलग-अलग वर्ग हैं। विज्ञापन का समग्र अध्ययन करने के लिए इस सब की जानकारी होना जरूरी है क्योंकि इसकी समझ के बिना विज्ञापन और पत्रकारिता के रिश्ते को समझा ही नहीं जा सकता । आज उपभोक्ता और बाजार के विशेषज्ञ दोनों इस बात को समझने लगे हैं कि बाजार की लड़ाई जीतने में विज्ञापन की क्या भूमिका है। इसलिए अब विज्ञापनकर्ता भी माध्यम के चयन के बारे में अधिक सतर्क हो गए हैं।
विज्ञापन के माध्यम
विज्ञापन माध्यम वस्तुतः वे साधन हैं जो उत्पादक या सेवा से सम्बद्ध सूचना या संदेश को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। माध्यम उत्पाद या सेवा और उपभोक्ता के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। विज्ञापन के लिए सही माध्यम का चयन करना एक प्रकार से विज्ञापन की सफलता की चाबी हासिल करना है। यह उसकी सफलता का मूलमंत्र है। किसी भी विज्ञापन का निर्माण करते समय सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उसका प्रसार किस माध्यम से किया जाना है।
माध्यम के चयन के बाद ही विज्ञापन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। हर माध्यम के लिए विज्ञापन का निर्माण भी अलग-अलग तरह से होता है। माध्यम के अनुरूप ही विज्ञापन की भाषा, संदेश और डिजाइन तय की जाती है। उसी के अनुरूप विज्ञापन की कॉपी लिखी जाती है।
विज्ञापनों के प्रकार
माध्यम के आधार पर विज्ञापनों को निम्न प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
1. प्रकाशन माध्यम
2. प्रसारण माध्यम
3. डाक विज्ञापन
4. वाह्य विज्ञापन
5. सचल विज्ञापन
6. उपहार विज्ञापन
विज्ञापन माध्यमों को उनकी विकास यात्रा के आधार पर भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विज्ञापन के प्रारम्भिक माध्यम और विज्ञापन के आधुनिक माध्यम। हालाँकि इस वर्गीकरण का अर्थ यह नहीं है कि विज्ञापन के जो प्रारम्भिक माध्यम थे वो अब उपयोग में नहीं लाए जाते। उनका आज भी बखूबी इस्तेमाल होता है। आधुनिक माध्यम अपेक्षाकृत नए हैं और उनमें अब भी बदलाव और विकास जारी है।
विज्ञापन के प्रारम्भिक माध्यम
विज्ञापन का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ा माना जा सकता है। मिश्र के पिरामिड या चीन की दीवार एक प्रकार से अपने दौर की महान सम्यताओं के विज्ञापन ही थे। राजवंशों के राजचिन्ह, ध्वज आदि भी एक प्रकार के विज्ञापन ही थे। सभ्यता के विकास के साथ-साथ संचार के माध्यम भी बदलते रहे हैं, और उन्ही के साथ विज्ञापनों का स्वरूप और माध्यम भी बदलता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में डुगडुगी बजाकर राजाज्ञा का वाचन किया जाता था, जो एक प्रकार का प्रारम्भिक विज्ञापन ही था। चित्रों द्वारा भी सूचनाएं दी जाती थीं। अशोक के स्तम्भ और उन पर उत्कीर्ण लेख भी एक तरह के विज्ञापन ही हैं। बौद्ध धर्म प्रचारकों के धर्म संदेश भी एक प्रकार से धर्म का विज्ञापन ही होते थे और इन संदेशों ने बौद्ध धर्म के प्रचार- प्रसार में अभूतपूर्व भूमिका भी निभाई थी। सन् 1440 में आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कार के साथ ही विज्ञापन कला को भी एक नया आयाम मिल गया और परचों (हैण्डबिल) तथा पोस्टरों के जरिए विज्ञापन किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया ।
प्राचीन शहर पम्पई के अवशेषों में दुकानों की दीवारों पर इस तरह के प्रतीक चिन्ह मिले हैं जिनसे यह पता चलता था कि वहां पर कौन सी वस्तु उपलब्ध है। प्राचीन रोम और ग्रीस की दुकानों के बाहर भी चिन्ह होते थे। इसी प्रकार सिंधु घाटी के अवशेषों में प्राप्त मोहरें भी एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह या ट्रेड मार्क ही थीं। इस तरह के सभी चिन्हों, प्रतीकों या मोहरों को विज्ञापन के बाह्य माध्यम कहा जा सकता है। ये बाह्य माध्यम विज्ञापन के सबसे प्रारम्भिक माध्यम हैं। दीवारों, सावर्जनिक स्थलों तथा यातायात के साधनों पर चित्रित किए जाने वाले विज्ञापन वाह्य माध्यम कहलाते हैं।
1473 में अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित कर विलियम कैक्सटोन ने पहले मुद्रित विज्ञापन के निर्माण का सूत्रपात किया और 1477 में उसी ने अंगे्रजी में पहला पोस्टर (हैण्ड बिल) छाप कर मुद्रित विज्ञापन की शुरूआत की। 16वीं और 17वीं सदी में अधिकतर विज्ञापन अंगे्रजी के हाथ से लिखे हुए पोस्टरनुमा हैण्ड बिलों के रूप में ही होते थे। 1622 में वीकली न्यूज आॅफ लन्दन का प्रकाशन शुरू हुआ और 1625 में पहली बार इसमें एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ जो एक जहाज के आने की सूचना देता था। मुद्रित माध्यमों में पहला व्यावसायिक विज्ञापन 1652 में प्रकाशित कॉफी का विज्ञापन था। 1657 में चॉकलेट और 1658 में चाय का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।
प्रारम्भिक विज्ञापन माध्यमों में वाह्य माध्यमों और मुद्रित माध्यमों के साथ-साथ डाक माध्यमों का भी अहम स्थान है। उन्नीसवीं सदी में राजकीय डाक सेवा शुरू होने के साथ ही अमेरिका और यूरोप सहित भारतीय उपमहाद्वीप में भी डाक माध्यम का इस्तेमाल विज्ञापनों के प्रसार के लिए प्रारम्भ हो गया। भारत में कपड़ा उत्पादकों और पुस्तक प्रकाशकों ने अपने उत्पादों के प्रचार के लिए डाक द्वारा मुद्रित प्रचार सामग्री उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की शुरूआत की थी।
विज्ञापन के आधुनिक माध्यम
1840 में अमेरिकी में वॉलनी पामर ने मुद्रित विज्ञापन माध्यम के रूप में पत्र-पत्रिकाओं का व्यावसायिक उपयोग प्रारम्भ कर दिया था। वह पत्र-पत्रिकाओं में स्थान खरीद लेता और विज्ञापनकर्ताओं से अधिक मूल्य लेकर उन्हें बेच देता था। यानी यह एक प्रकार से आधुनिक विज्ञापन एजेंसी का प्रारम्भिक रूप था। 1873 तक अमेरिका में ‘लेविस’ जींस मुद्रित माध्यमों में विज्ञापन के जरिए एक ‘ब्रांड’ बन चुकी थी। इसी तरह 1876 में कोका कोला को भी एक ब्रांड के रूप में पहचान मिल गई थी।
मगर विज्ञापन के आधुनिक माध्यम के रूप में मुद्रित माध्यमों को व्यापक पहचान बीसवीं सदी में ही मिल पाई। प्रथम विश्य युद्ध के बाद पुर्ननिर्माण के दौर में जरूरी चीजों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो जाने से विज्ञापन की आवश्यकता और उपयोग में भी जबर्दस्त इजाफा हुआ और इसी के साथ मुद्रित माध्यमों के विज्ञापनों में कला पक्ष और कॉपी लेखन पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इसी दौर में डाक के जरिए विज्ञापन के एक और माध्यम का प्रचलन भी शुरू हुआ। डायरेक्ट मेल नामक यह माध्यम चुनिंंदा लोगों के पास सीधे उत्पाद भी जानकारी डाक द्वारा पहुँचाता था। बड़े उत्पादों के प्रचार में यह माध्यम भी एक प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ।
1928 में पहली बार रेडियो का उपयोग विज्ञापन के माध्यम रूप में किया गया और इसी के साथ श्रव्य माध्यम के रूप में विज्ञापन के लिए एक और माध्यम उपलब्ध हो गया। रेडियो के विज्ञापन जल्द ही लोकप्रिय हो गए। 1950 के दशक में इंग्लैण्ड में सिनेमा घरों में दिखाए जाने के लिए 50 सेकेण्ड से 2 मिनट तक की अवधि की विज्ञापन फिल्में भी बनाई जाने लगी थीं जो दृश्य माध्यम के रूप में विज्ञापन के एक और माध्यम की शुरूआत थीं। इन फिल्मों ने अनेक उत्पादों को रातों रात लोकप्रिय बना दिया और इसी कारण यह माध्यम भी बेहद लोकप्रिय माध्यम बन गया। आज के टेलीविजन विज्ञापनों का जन्म भी इसी से हुआ है। इसी दौर में छोटे उत्पादकों ने सिनेमाघरों में स्लाइड के जरिए अपने उत्पादों के विज्ञापन की शुरूआत की, यह भी जल्द ही एक लोकप्रिय माध्यम बन गया ।
आज टीवी से भी अधिक नए विज्ञापन माध्यम विज्ञापन जगत में हलचल मचा रहे है। आॅन लाइन कम्प्यूटर सेवा, होम शापिंग ब्राडकास्ट और मोबाइल तथा इंटरनेट ने नए विज्ञापन माध्यमों को जन्म दे दिया है, साथ इंटरनेट या ई-मेल के जरिए विज्ञापन को सारी दुनिया में भी पहुँचाया जाना सम्भव हो गया है। इन नए माध्यमों की लागत भी काफी कम है।
विज्ञापन के प्रकाशन माध्यम
प्रकाशन माध्यम या मुद्रण माध्यम विज्ञापन का बहुत पुराना माध्यम है। मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं दोनों ही शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को सूचनाएं और संदेश देकर प्रभावित करती हैं। डायरेक्ट मेल और कैटलॉग आदि भी प्रकाशन माध्यम का हिस्सा हैं। विज्ञापन के प्रकाशन माध्यमों की विशिष्टता इस बात में है कि इस माध्यम के जरिए विज्ञापन एक छोटी सी जगह में बड़ी कलात्मकता से अपनी बात उपभोक्ताओं अथवा ग्राहकों तक संप्रेषित कर देते हैं।
समाचार पत्र :
आज विज्ञापन समाचार पत्र उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं। समाचार पत्रों में तरह-तरह के विज्ञापनों की भरमार भी देखी जा सकती है। समाचार पत्रों का मुख्य कार्य दिन-प्रतिदिन की खबरें समाज के व्यापक हिस्से तक पहुँचाना है, मगर साथ ही ये समाचार देने के साथ-साथ निर्धारित शुल्क लेकर विज्ञापन भी प्रकाशित करते हैं।
समाचार पत्रों के ऐतिहासिक परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि समाचार पत्रों ने अपने विकास के पहले चरण से ही विज्ञापन प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। साक्षरता और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ समाचार पत्रों की लोकप्रियता बढ़ी तो इनमें विज्ञापन प्रकाशित करने की उपादेयता भी बढ़ती गई। आज दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक सभी तरह के समाचार पत्रों में विज्ञापनों की भरमार देखी जा सकती है। क्षेत्रीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के सभी अखबार संसाधन जुटाने के लिए विज्ञापनों के लिए जगह सुरक्षित रखते हैं, और इस स्थान को येन-केन प्रकारेण विज्ञापनों से भरते भी हैं।
जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी व गैर-सरकारी प्रतिष्ठान समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं। कभी-कभी विशिष्ट अवसरों पर उत्पाद या सेवा के विज्ञापन को अधिक प्रभाव के साथ प्रस्तुत करने के लिए विशेष परिशिष्ट भी प्रकाशित किये जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने मंत्रालयों की महत्वपूर्ण सूचनाओं और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाती हैं। राष्ट्रीय समारोहों के अवसर पर भी महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित करवाए जाते है।
समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के लाभ और सीमाएँ दोनों ही हैं। समाचार-पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (टेलीविजन तथा रेडियो) की अपेक्षा सस्ता होता है। एक निश्चित भौगालिक सीमा में रहने वाले समूह के हिसाब से विज्ञापन क्षेत्रीय अथवा प्रांतीय अखबारों में दिए जा सकते है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद तथा सेवाओं संबंधी विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन की भाषा और प्रस्तुति में उपभोक्ता की मनोवृति को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर बदलाव लाकर अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
किंतु समाचारपत्र विज्ञापन की अपनी कुछ सीमाएं अथवा कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी है इसका अल्पकालिक जीवन। इसकी जीवन-अवधि केवल एक दिन की होती है, इसके बाद यह रद्दी हो जाता है। निरक्षर और अशिक्षित उपभोक्ताओं या ग्राहकों के लिए समाचारपत्र के विज्ञापन निरर्थक होते हैं।
समाचार पत्र-पत्रिकाऐं एक सीधा विज्ञापन माध्यम है जो सम्भावित ग्राहकों या उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या तक संदेश पहुँचाता है। यह अपेक्षाकृत सस्ता माध्यम है। समाचार पत्रों के विज्ञापन की लागत विज्ञापन के आकार, स्थान और समाचार पत्र की वितरण संख्या के आधार पर तय होती है। समाचार पत्रो विज्ञापन के जरिए स्थानीय सूचनाएं पहुँचाने के लिए भी आदर्श माध्यम हैं।
डायरेक्ट मेल :
डायरेक्ट मेल आधुनिक दौर का एक ऐसा मुद्रित विज्ञापन माध्यम है जिसका प्रयोग कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को ही लक्ष्य बनाकर किया जाता है। इस माध्यम में संदेश सार्वजनिक न होकर सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनके पास इसे भेजा जाता है। इस माध्यम के द्वारा विज्ञापनकर्ता उपभोक्ता से सीधा संवाद करता है क्योंकि इसमें विज्ञापन को सीधे उपभोक्ता तक भेज दिया जाता है। विज्ञापनकर्ता अपने चुने हुए उपभोक्ताओं या लक्ष्य समूह तक अपने उत्पाद या विषय की जानकारी पत्र, प्रचार सामग्री, फोल्डर आदि के जरिए भेजता है।
इस माध्यम के जरिए कुछ चुने हुए सम्भावित या पुराने उपभोक्ताओं तक विज्ञापनकर्ता का संदेश सीधे पहुँचता है इसलिए इसका असर भी अधिक होता है। बड़े उत्पादों के मामले में यह माध्यम अधिक असर कारक है। उदाहरणार्थः किसी एक कंपनी से कार खरीद चुके ग्राहक के पास वही कंपनी जब अपनी नई कार के बारे में डायरेक्ट मेल से सूचना भेजती है तो ग्राहक पर उसका अधिक असर होता है। इस माध्यम में संदेश विस्तृत और सूचनाप्रद होता है, जिससे उपभोक्ता को उत्पाद की पूरी जानकारी हो जाती है। लेकिन यह तुलनात्मक रूप से मंहगा माध्यम है क्योंकि इसमें संदेश पर व्यय अधिक होता है।
कैटलॉग :
कैटलॉग या सूची पत्र भी एक उपयोगी विज्ञापन माध्यम है। यूरोपीय देशों में एक दौर में कैटलॉग के जरिए खूब विज्ञापन किए जाते थे। कैटलॉग किसी विशेष कंपनी या फर्म के विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। इनमें विज्ञापनकर्ता के विभिन्न उत्पादों का मूल्य, गुणवत्ता रंग, आकार प्रकार, विशेषताओं व उपयोग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है।
कैटलॉग कई प्रकार के होते है। जैसे खुदरा कैटलॉग, व्यावसायिक कैटलॉग और उपभोक्ता कैटलॉग आदि।
कलैण्डर :
कलैण्डर भी विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण मुद्रित माध्यम है। कलैण्डर प्रायः हर घर में लगे होते हैं। यह एक ऐसा प्रभावी माध्यम है जो हर वक्त नजर पड़ने पर उपभोक्ता को उत्पाद की याद दिलाता रहता है। कलैण्डर दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें सिर्फ तारीखें होती हैं और विज्ञापनकर्ता का नाम पता और उत्पाद आदि की जानकारी होती है। दूसरी तरह के कलैण्डरों में आकर्षक चित्र, तस्वीरें आदि होती है, देवी देवताओं के चित्र होते हैं, और इन चित्रों के नीचे या उपर विज्ञापनकर्ता का परिचय होता है। बड़े कारपोरेट घरानों से लेकर सार्वजनिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थान कलैण्डरों को विज्ञापन माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं।
फोल्डर और पैम्फलेट :
ये स्थानीय विज्ञापन के सस्ते माध्यम हैं। पैम्फलेट प्रायः छोटे आकार के रंगीन पतले कागज पर मुद्रित किए जाते हैं और इनमें स्थानीय सेवाओं या उत्पादों के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। पैम्फलेट या तो हाथों हाथ बांट दिए जाते हैं या समाचार पत्रों के साथ वितरित किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले इस माध्यम का असर तत्काल होता है।
फोल्डर भी एक प्रकार के पैम्फलेट हैं, जिनमें पैम्फलेट की अपेक्षा अधिक अच्छे कागज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कागज छपाई के बाद मोड़े (फोल्ड किए) जाते हैं, इसीलिए इन्हें फोल्डर कहा जाता है। फोल्डर में एक उत्पाद या एक संस्थान के एकाधिक उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। फोल्डर में शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र, ब्रांड आदि का विस्तार से प्रयोग होता है। फोल्डर का प्रयोग पर्यटन सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसार के लिए भी खूब होता है।
विज्ञापन के प्रसारण माध्यम
विज्ञापन के प्रसारण माध्यमों में श्रव्य-दृश्य माध्यम शामिल हैं। यह प्रसारण माध्यम विज्ञापन के सबसे बड़े और प्रभावशाली माध्यम हैं, जिनके जरिए विज्ञापनों को व्यापक प्रचार और उन्नत रूप मिला है। रेडियो और टेलीविजन इस श्रेणी के प्रमुख माध्यम हैं।
रेडियो :
रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। जो विश्व व्यापी है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक, हर कहीं इसकी पहंुच है। यह एक ऐसा माध्यम है, जो निरक्षर लोगों तक भी विज्ञापन का संदेश पहुँचा सकता है। भारत में कृषि, ग्रामीण उपभोक्ता वस्तुओं और जनहित की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए इसकी अत्यधिक उपयोगिता है।
माध्यम के रूप में रेडियो का उपयोग कर विज्ञापनों को अनेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे –
1. सामान्य उद्घोषणा के तौर पर
2. नाटकीय संवादों के जरिए
3. किसी खास व्यक्ति की आवाज में विज्ञापित वस्तु की प्रशंसा या
4. उपयोगिता बताकर अथवा
5. लोकगीतों, संगीत और ध्वनि प्रभावों की मदद से।
रेडियो विज्ञापनों में लोकगीतों और संगीत का प्रयोग इन्हें अति विशिष्ट बना देता है। ऐसे अनेक रेडियो विज्ञापन हैं, जो अपनी सुरीली धुन और गेय शैली के कारण लोगों की जुबान पर चढ़ गए। हाल के वर्षों में एफएम रेडियो का तेजी से विकास होने के कारण अब शहरी क्षेत्रों में भी रेडियो विज्ञापनों की लोकप्रियता खूब बढ़ गई है।
हालाँकि दृश्य माध्यमों के विज्ञापनों की तुलना में रेडियो में उद्घोषणा के रूप में प्रस्तुत विज्ञापन अधिक समय तक उपभोक्ताओं की स्मृति में नहीं रह पाते ।
टेलीविजन
टेलीविजन आज विज्ञापन का सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय विज्ञापन माध्यम बन गया है। पश्चिम की तुलना में भारत में टेलीविजन का आगमन अपेक्षाकृत नया है। देश में 1976 में दूरदर्शन से पहली बार विज्ञापनों का प्रसारण हुआ मगर आज दूरदर्शन देश का सबसे प्रभावी विज्ञापन माध्यम है। बड़ी-बड़ी कंपनियां, कारपोरेट हाऊस, संस्थाएं और संगठन अपने उत्पादों अथवा सेवाओं के विज्ञापन टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। टेलीविजन द्वारा प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में दृश्य और श्रव्य प्रभावों के साथ-साथ संगीत और विज्ञापित वस्तु की विशेषताएं बताने के लिए विशेष प्रभावों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो टेलीविजन को एक सर्वाधिक प्रभावशाली विज्ञापन माध्यम के रूप में स्थापित करता है। यह एक चमत्कारिक और बहुसंवेदी माध्यम है जो विज्ञापनकर्ता को अपनी बात पूरी तरह संप्रेषित करने का पूरा-पूरा अवसर देता है।
टेलीविजन के विज्ञापन उपभोक्ता और उत्पाद के बीच की दूरी को बहुत कम कर देते हैं। उपभोक्ता उत्पाद की खूबियों को सजीव ढंग से देखता है, इसलिए उस पर इन विज्ञापनों का असर भी अधिक होता है। इन विज्ञापनों के सीधे प्रभाव के कारण उपभोक्ता का निर्णय प्रक्रिया पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है।
टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन मुख्यतः दो प्रकार के होते है।
1. स्पॉट विज्ञापन
2. प्रायोजित कार्यक्रम
स्पॉट एडवरटिजमेंट या समयबद्ध विज्ञापन बहुत छोटी अवधि के होते हैं। इस तरह के विज्ञापनों में उत्पाद की गुणवत्ता, खूबियों, मूल्य आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। इनमें उत्पाद को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और प्रायः इनका प्रभाव चैंकाने वाला होता है। इस तरह के कार्यक्रम न्यूज चैनलों में समाचारों के बीच-बीच में, खेलों के प्रसारण के दौरान बीच-बीच में या अन्य चैनलों में कार्यक्रमों के बीच में कहीं भी दिखाए जा सकते हैं। क्रिकेट के मैचों में तो हर ओवर के बाद या किसी खिलाड़ी के आऊट होने पर भी इस तरह के विज्ञापन दिखा दिए जाते हैं।
प्रायोजित कार्यक्रम इस तरह के विज्ञापन हैं जो दीर्घ अवधि के लिए किसी विशेष उत्पाद का प्रचार करते है। उदाहरणार्थः यदि किसी विशेष चैनल में 30 मिनट के किसी खास कार्यक्रम का नियमित प्रसारण होता है तो ऐसे किसी कार्यक्रम को किसी विशेष उत्पाद की ओर से प्रायोजित कर दिया जाता है। तब प्रायोजक का नाम भी ऐसे कार्यक्रम से जुड़ जाता है और कार्यक्रम के दौरान कई बार प्रायोजक का उल्लेख किया जाता है। मनोरंजन चैनलों में इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रमों की भरमार होती है। क्रिकेट में तो कई बार पूरी प्रतियोगिता ही किसी खास प्रायोजक द्वारा प्रायोजित होती है और ऐसे मैचों के सजीव प्रसारण में बार-बार प्रायोजक का जिक्र होता रहता है।
टेलीविजन के विज्ञापन ब्रांड का महत्व बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धौनी जैसे बड़े खिलाड़ियों या सिने कलाकारो को किसी खास उत्पााद के ब्रांड एम्बेसेडर के तौर पर प्रस्तुत कर विज्ञापनकर्ता बड़ा लाभ पा सकता है, उसका उत्पाद रातों-रात लोकप्रिय हो सकता है।
टेलीविजन ने जहां भाषा और लिपि की सीमाएं खत्म कर दी है, वहीं इस माध्यम में एक बड़ी कमी यह है कि टेलीविजन यह बेहद खर्चीला माध्यम है। टेलीविजन विज्ञापन की निर्माण प्रक्रिया जटिल है और इसमें लागत भी अधिक आती है। साथ ही यदि विज्ञापन बार-बार नहीं दिखाया जाता तो इस बात की भी आशंका रहती है कि वह उपभोक्ता तक पहुंच भी पाया है अथवा नहीं।
फिल्म व वीडियो :
सिनेमा भी एक खास प्रकार का श्रव्य-दृश्य विज्ञापन का माध्यम है। इसका इस्तेमाल सिनेमाघरों में लघु फिल्मों या स्लाइड्स के जरिए उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने के लिए किया जाता है। इस माध्यम की खूबी यह है कि इसमें इस बात की गारंटी होती है कि इसे एक निश्चित दर्शक वर्ग देखेगा ही। फिल्म माध्यम में स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ मशहूर ब्रांड भी अपने विज्ञापन करते हैं।
कई बार कोई विशेष उत्पाद किसी पूरी फीचर फिल्म के साथ ही इस तरह के अनुबंध कर लेता है कि फिल्म में उसी के उत्पाद मसलन होटल, रेस्तरां, विमान सेवा, प्रतिष्ठान आदि का प्रदर्शन कहानी के हिस्से के रूप में कर दिया जाता है।
उदाहरणार्थ किसी फिल्म का नायक विमान यात्रा कर रहा है तो फिल्म में उसे किसी विशेष विमान सेवा के विमान से जाते हुए दिखाया जाता है। दृश्यों में उस विमान सेवा के कर्मचारी, विमान आदि भी दिखा दिए जाते हैं। यह विज्ञापन का एक महंगा तरीका है।
फिल्मों की तरह से ही वीडियो फिल्मों के जरिए भी विज्ञापन किए जाते हैं। आजकल स्थानीय तौर पर चलने वाले केबल नेटवर्क वीडियो फिल्मों के जरिए स्थानीय उत्पादों का विज्ञापन जमकर करने लगे हैं।
इंटरनेट :
इंटरनेट आज विज्ञापन का सबसे नया और विस्तृत माध्यम बन चुका है। अंतराष्ट्रीय व्यापार जगत आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने उत्पादों का विज्ञापन कर रहा है और अपना प्रचार-प्रसार कर रहा है। वेब एडवरटाईजिंग यानी इंटरनेट के जरिए विज्ञापन आज एक तेजी से लोकप्रिय हो रहा विज्ञापन माध्यम बन गया है। इंटरनेट के जरिए विज्ञापन अधिक महंगा भी नहीं है और इसका प्रसार क्षेत्र असीमित है इसलिए इसका असर भी व्यापक होता है। फिर भी इंटरनेट अभी सर्व जन का विज्ञापन माध्यम नहीं बन सका है और इसकी पहंचु एक खास वर्ग तक ही सीमित है। यही हाल मोबाइल विज्ञापनों का भी है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में विज्ञापन के दृश्य-श्रव्य माध्यम ही सर्वाधिक प्रभावशाली और असरदार माध्यम बन गए हैं और तकनीक के विकास के साथ-साथ इन माध्यमों का भी उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है।
टेलीविजन न्यूज
भारतीय पौराणिक ग्रंथ महाभारत की कथा में संजय द्वारा धृतराष्ट्र के पास बैठे-बैठे महाभारत के युद्व क्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाने का उल्लेख भले ही मिलता हो मगर आधुनिक टेलीविजन के इतिहास को अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। सन् 1900 में पहली बार रूसी वैज्ञानिक कोंस्तातिन पेस्र्की ने सबसे पहली बार टेलीविजन शब्द का इस्तेमाल चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाले एक प्रारम्भिक यंत्र के लिए किया था। 1922 के आस-पास पहली बार टेलीविजन का प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था। 1926 में इंग्लैण्ड के जॉन बेयर्ड और अमेरिका के चाल्र्स फ्रांसिस जेनकिंस ने मैकेनिकल टेलीविजन के जरिए चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का सफल प्रयोग किया।
पहले इलेक्ट्रानिक टेलीविजन का आविष्कार रूसी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ब्लादीमिर ज्योर्खिन ने 1927 में किया। हालांकि इसकी दावेदारी जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भी करते रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रानिक टेलीविजन उनके देश में बनाया गया। बहरहाल 1939 में पहली बार अमेरिकी रेडियो प्रसारण कंपनी आरसीए ने न्यूयार्क विश्व मेले के उद्घाटन और राष्ट्रपति रूजवैल्ट के भाषण का सीधा टेलीविजन प्रसारण किया। बीबीसी रेडियो 1930 में और बीवीसी टेलीविजन 1932 में स्थापित हो गया था। इसने 1936 के आस पास कुछ टीवी कार्यक्रम बनाए भी। इसी बीच दूसरा विश्वयुद्व छिड़ जाने से टीवी के विकास की रफ्तार कम हो गई।
1 जुलाई 1941 को अमेरिकी कंपनी कोलम्बिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने न्यूयार्क टेलीविजन स्टेशन से रोजाना 15 मिनट के न्यूज बुलेटिन की शुरूआत की। यह प्रसारण सीमित दर्शकों के लिए था। विश्वयुद्व की समाप्ति के बाद तकनीकी विकास के दौर में 1946 में रंगीन टेलीविजन के आविष्कार ने टीवी न्यूज के विकास में एक बड़ी छलांग का काम किया। 50 के दशक में अमेरिकी प्रसारण कंपनी एनबीसी और एनसीबीएस ने रंगीन न्यूज बुलेटिन शुरू किए तो बीबीसी टीवी ने भी दैनिक न्यूज बुलेटिन शुरू कर दिए। 1980 में टेड टर्नर ने सीएनएन के 24 घंटे के न्यूज चैनल की शुरूआत की। 24 घंटे का यह न्यूज चैनल जल्द ही लोकप्रिय हो गया और 1986 में स्पेस शटल चैलेजंर के दुघर्टनाग्रस्त होने के सजीव प्रसारण ने इसे बहुत ख्याति प्रदान की। लगभग 10 वर्ष बाद 1989 में ब्रिटेन में भी रूपर्ट मर्डोक ने लन्दन से स्काई न्यूज के नाम से 24 घंटे का न्यूज चैनल शुरू किया जबकि टीवी न्यूज में काफी नाम कमा चुके बीबीसी को 24 घंटे का न्यूज चैनल शुरू करने के लिए 1997 तक इन्तजार करना पड़ा। आज विश्व के प्रायः हर देश में एक से अधिक न्यूज चैनल हैं। पश्चिमी टीवी न्यूज चैनलों का एकाधिकार और दबदबा भी अब कम होता जा रहा है और अल जजीरा जैसे चैनल टीवी खबरों की दुनिया में पश्चिमी एकाधिकार को कड़ी चुनौती देने लगे हैं।
भारत में टेलीविजन का आगमन 1959 में हो गया था। प्रारम्भ में यह माना गया था कि भारत जैसे गरीब देश में इस महंगी टैक्नोलॉजी वाले माध्यम का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे यह धारणा खुद ब खुद बदलती चली गई। 1964 में दूरदर्शन पर पहली बार न्यूज की शुरूआत हुई। शुरू में यह रेडियो यानी आकाशवाणी के अधीन था। इसका असर दूरदर्शन के समाचारों पर भी दिखाई देता था। लेकिन 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों के आयोजन, एशियाड के साथ ही देश में रंगीन टेलीविजन की शुरूआत हो गई और यहीं से दूरदर्शन के समाचारों में एक नए युग की शुरूआत भी हुई। इसी दौर में हिंदी के अलावा उर्दू, संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के न्यूज बुलेटिन भी शुरू हुए। संसदीय चुनावों के कवरेज ने दूरदर्शन न्यूज को काफी लोकप्रिय बनाया मगर उसे अभी निजी चैनलों की चुनौती नहीं मिली थी।
भारतीय टेलीविजन में निजी क्षेत्र का खबरों की दुनिया में प्रवेश 1994 में हुआ। पहले जैन टीवी और फिर जी टीवी ने न्यूज बुलेटिन शुरू किए। पहला चौबीस घंटे का न्यूज चैनल भी जैन टीवी का ही था जो अधिक समय तक चल नहीं पाया। जी न्यूज ने 1 फरवरी 1999 को चौबीस घंटे का न्यूज चैनल शुरू किया जो आज भी चल रहा है। इसी बीच बीओआई ने भी न्यूज चैनल शुरू किया, मगर खर्चीले प्रबन्धन ने उसे भी जल्द ही डुबा दिया। लेकिन भारत में टीवी न्यूज को सही मायनों में स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है ‘आज तक’। यह 17 जुलाई 1995 को आज तक 20 मिनट के न्यूज बुलेटिन के तौर पर दूरदर्शन में शुरू हुआ था। सुरेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल संपादन व प्रस्तुतिकरण ने जल्द ही आजतक को सर्वश्रेष्ठ और विश्वसनीय समाचार बुलेटिन बना दिया। इसकी सफलता की नींव पर 31 दिसम्बर 2000 को आज तक के 24 घंटे के निजी न्यूज चैनल की शुरूआत हुई जो अब भी सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है।
आज देश में 100 से अधिक निजी न्यूज चैनल हैं और सब अपनी-अपनी विशिष्टताओं के साथ खबरों की दुनिया में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तकनीक के सस्ते होते जाने से भी टीवी न्यूज का विस्तार तेजी से हुआ है। पहले न्यूज चैनल शुरू करने में 50 करोड़ से अधिक खर्च आता था तो आज महज कुछ करोड़ रूपयों में न्यूज चैनल शुरू हो जाता है। मगर तकनीक सस्ती होने के साथ ही टीवी न्यूज में भी सस्तापन आने लगा है, गम्भीरता और लोक जिम्मेदारी की भावना कम होने से साथ-साथ सनसनी और नाटकीयता बढ़ने लगी है। टीवी न्यूज के भविष्य के लिए यह शुभ संकेत नही कहे जा सकते, मगर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा।
रेडियो
इलेक्ट्रानिक मीडिया का पहला क्रातिकारी कदम रेडियो को माना जाता है। उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में सन् 1895 में इटली के वैज्ञानिक गुगलीनो मारकोनी ने बेतार संकेतों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हार्टीजियन तरंगों द्वारा प्रसारित करने में सफलता हासिल कर रेडियो की अवधारणा को जन्म दिया। जल्द ही रेडियो, टेलीफोन और बेतार का तार समुद्री यातायात में संचार का प्रमुख साधन बन गये। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक संचार और प्रचार के लिए भी रेडियो का खूब इस्तेमाल हुआ था। विश्व युद्व के बाद रेडियो का इस्तेमाल जनसंचार मीडिया के तौर पर किए जाने के लिए परीक्षण शुरू हुए और 1920 में अमेरिका के पिट्सवर्ग में दुनिया का पहला रेडियो प्रसारण केन्द्र स्थापित हुआ। 23 फरवरी 1920 को मारकोनी की कंपनी ने भी चैम्सफोर्ड, इंग्लैण्ड से अपने पहले रेडियो कार्यक्रम का सफल प्रसारण किया। 14 नवम्बर 1922 को लन्दन में ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। मारकोनी भी इसके संस्थापकों में एक थे। एक जनवरी 1927 को इस कंपनी को ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन, बीबीसी मंे परिवर्तित कर दिया गया।
भारत में 8 अगस्त 1921 को टाइम्स आॅफ इण्डिया के मुम्बई कार्यालय ने एक विशेष रेडियो संगीत कार्यक्रम का प्रसारण कर भारत में रेडियो प्रसारण की नींव रखी। इस प्रसारण को पुणे तक सुना गया था। इसी के साथ पश्चिम की तरह भारत में भी शौकिया रेडियो क्लबों की स्थापना होने लगी। 13 नवम्बर 1923 को कोलकाता से रेडियो क्लब आॅफ बंगाल ने और 8 जून 1924 को बाम्बे रेडियो क्लब मुम्बई ने अपने प्रसारण शुरू किए। साथ ही चेन्नई, करांची तथा रंगून में भी ऐसे ही प्रसारण केन्द्र शुरू हो गए। आर्थिक अभावों के कारण प्रायः ये सभी रेडियो क्लब दीर्घजीवी नहीं रह पाए लेकिन इसके बावजूद रेडियो की लोकप्रियता कम नहीं हुई।
23 जुलाई 1927 को चेन्नई में इण्डियन ब्राडकास्टिंग कंपनी (आईबीसी) का विधिवत उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन द्वारा किया गया। उस समय भारत में कुल 3594 रेडियो सेट थे। तब रेडियो सेट रखने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लगातार घाटे के कारण जल्द ही आईबीसी को बंन्द करने की नौबत आ गई लेकिन रेडियो सुनने के आदी हो चुके लोगों के तीव्र विरोध के कारण सरकार ने इसका प्रसारण जारी रखने का फैसला किया और 1 अपै्रल 1930 को इण्डियन स्टेट ब्राडकांस्टिंग सर्विस की स्थापना हुई जो बाद में आकाशवाणी में परिवर्तित हो गई।
आज आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क हो चुका है। एक अरब से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच है। देश भर में आकाशवाणी के 250 से अधिक छोटे बड़े केन्द्र हैं। 25 से अधिक भाषाओं और 150 से अधिक बोलियों में इसके कार्यक्रम प्रसारित होते है। एफएम (फ्रीक्वेंसी मोड्युलेटर) सेवा की शुरूआत के साथ भारत में रेडियो को एक नया जीवन मिला है। आज आकाशवाणी के साथ-साथ प्रायः हर बड़े शहर में एक दो निजी एफएम रेडियो प्रसारण हो रहें है, और लोगों को मनोरंजन के साथ सूचना भी उपलब्ध करा रहे है।
रेडियो टैक्नोलॉजी के डिजीटल हो जाने से भी रेडियो को नया जीवन मिल गया है और अब तो वल्र्ड स्पेस रेडियो भी भारत में उपलब्ध है। देश में आज 25 करोड़ से अधिक रेडियो सेट हैं और आज भी दूर दराज के इलाकों में सूचना और संचार का यह सबसे भरासेमंद साधन है।
हालांकि रेडियो के और भी कई उपयोग हैं, मसलन पुलिस व सेना इसे अपने विभागीय संचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विमान यात्राओं के संचालन में भी इसका प्रयोग होता है। समुद्री यात्राओं, पर्वतारोहण अभियानों व अन्य साहसिक अभियानों में भी इसका इस्तेमाल संचार के विश्वस्त साधन के रूप में किया जाता है। वैसे तो ध्वनि की रफ्तार 345 मीटर प्रति सेकेंड होती है लेकिन रेडियो प्रसारण की तकनीक के कारण इसकी गति 1,86,000 मील प्रति मिनट हो जाती है। इसी कारण रेडियो के जरिए लाखों मील दूर तक की बात हम एक सैकेंड से भी कम समय में सुन लेते हैं।
रेडियो क्योंकि बोले जाने वाले शब्दों का माध्यम है। इसलिए इसके समाचारों की भाषा भी प्रिंट्र मीडिया के समाचारों से कुछ अलग होती है। इसलिए रेडियो के लिए समाचार बनाते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं।
1- समाचार में शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि वो श्रोता को आसानी से समझ में आ जाएं।
2- वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिये और उनमें शब्द आम बोलचाल की भाषा के
होने चाहिए।
3- सरलता रेडियो समाचार लेखन का सबसे जरूरी तत्व है, अतः रेडियो समाचार सरल ढंग से लिखा जाना चाहिए।
4- चूंकि श्रोता के पास रेडियो समाचार को अखबार की तरह फिर से पढ़ पाने की सुविधा नहीं होती इसलिए महत्वपूर्ण सूचना व जरूरी अंश को एक से अधिक बार लिखा जाना चाहिए लेकिन इस तरह कि वह सिर्फ दोहराव ही
न लगे ।
5- रेडियो समाचारों में उपर्युक्त, पूर्ववर्णित, निम्नलिखित, पिछले पैराग्राफ में
आदि शब्दों से एकदम बचना चाहिए।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेडियो निःसंदेह आज भी इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों में अग्रणी है और एफएम की युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता ने इसे एक प्रकार से फिर से पुर्नजीवित कर दिया है और एक बार फिर लोग रेडियो की ओर से मुड़ने लगे हैं।
फीचर
फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिन्दी में फीचर के लिये रुपक शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन फीचर के लिये हिन्दी में प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है – किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है। लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नही होता है।फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव – जन्तु, तीज – त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति – परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है।
फीचर के प्रकार·
- सूचनात्मक फीचर
-
व्यक्तिपरक फीचर
-
विवरणात्मक फीचर
-
विश्लेषणात्मक फीचर
-
साक्षात्कार फीचर
-
इनडेप्थ फीचर
-
विज्ञापन फीचर
-
अन्य फीचर
फीचर की विशेषतायें
-
किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है।
-
एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिये।
-
फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिये।
-
फीचर का विषय रोचक होना चाहिये या फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिये।
-
फीचर को शुरु से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिये।
-
फीचर को ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तनसूचक होना चाहिये।
-
फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिये।
-
फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है।
-
फीचर को सीधा सपाट न होकर चित्रात्मक होना चाहिये।
-
फीचर कीभाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ–साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिये।
फीचर लेखन की प्रक्रिया
- विषय का चयन
- सामग्री का संकलन
- फीचर योजना
विषय का चयन
किसी भी फीचर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला है। इसलिये फीचर का विषय समयानुकूल, प्रासंगिक और समसामयिक होना चाहिये। अर्थात फीचर का विषय ऐसा होना चाहिये जो लोक रुचि का हो, लोक – मानव को छुए, पाठकों में जिज्ञासा जगाये और कोई नई जानकारी दे।
सामग्री का संकलन
फीचर का विषय तय करने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चरण है विषय संबंधी सामग्री का संकलन। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में किसी विषय पर लिखा गया फीचर उबाऊ हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र – पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा फीचर लेखक को बहुत सामग्री लोगों से मिलकर, कई स्थानों में जाकर जुटानी पड़ सकती है।
फीचर योजना
फीचर से संबंधित पर्याप्त जानकारी जुटा लेने के बाद फीचर लेखक को फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध खाका बनाना चाहिये।
फीचर लेखन की संरचना
· विषय प्रतिपादन या भूमिका
· विषय वस्तु की व्याख्या
· निष्कर्षविषय प्रतिपादन या भूमिका
फीचर लेखन की संरचना के इस भाग में फीचर के मुख्य भाग में व्याख्यायित करने वाले विषय का संक्षिप्त परिचय या सार दिया जाता है। इस संक्षिप्त परिचय या सार की कई प्रकार से शुरुआत की जा सकती है। किसी प्रसिद्ध कहावत या उक्ति के साथ, विषय के केन्द्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके, घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर। भूमिका का आरेभ किसी भी प्रकार से किया जाये इसकी शैली रोचक होनी चाहिये मुख्य विषय का परिचय इस तरह देना चाहिये कि वह पूर्ण भी लगे लेकिन उसमें ऐसा कुछ छूट जाये जिसे जानने के लिये पाठक पूरा फीचर पढ़ने को बाध्य हो जाये।
विषय वस्तु की व्याख्या
फीचर की भूमिका के बाद फीचर के विषय या मूल संवेदना की व्याख्या की जाती है। इस चरण में फीचर के मुख्य विषय के सभी पहलुओं को अलग – अलग व्याख्यायित किया जाना चाहिये। लेकिन सभी पहलुओं की प्रस्तुति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रमबद्धता होनी चाहिये। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिये फीचर में मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिये।
निष्कर्ष
फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। इस भाग में फीचर लेखक अपने ऴिषय को संक्षिप्त रुप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुये फीचर को समाप्त करता है। साथ ही वह कुछ सवालों को पाठकों के लिये अनुत्तरित भी छोड़ सकता है। और कुछ नये विचार सूत्र पाठकों से सामने रख सकता है जिससे पाठक उन पर विचार करने को बाध्य हो सके।
फीचर संरचना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू
किसी रचना का यह एक जरुरी हिस्सा होता है और यह उसकी मूल संवेदना या उसके मूल विषय का बोध कराता है। फीचर का शीर्षक मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिये जिससे वह पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके।
छायाचित्र
छायाचित्र होने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है जिसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विषय से संबंधित छायाचित्र देने से विषय और भी मुखर हो उठता है। साथ ही छायाचित्र ऐसा होना चाहिये जो फीचर के विषय को मुखरित करे फीचर को कलात्मक और रोचक बनाये तथा पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति विश्वसनीयता बनाये।
ब्रांड प्रबंधन
ब्रांड प्रबंधन को समझने से पूर्व समझें कि ब्रांड क्या है।
ब्रांड किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को दी गई वह पहचान है, जो उत्पाद के नाम, लोगो और ट्रेडमार्क आदि के रूप में प्रदर्शित की जाती है।
ब्रांडों का ही कमाल है कि आज कई ऐसी वस्तुएें भी हैं जो अपनी वास्तविक पहचान या नाम के बजाय अपने ब्रांड के नाम से ही जानी जाती हैं।
जैसे: ताले को हरीसन का ताला, अल्मारी को गोदरेज की अल्मारी, वनस्पति घी को डालडा, डिटरजेंट पावडर को सर्फ, टूथ पेस्ट को कोलगेट को उनकी कंपनी के नाम से जाना जाता है।
कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं, जिनकी कंपनियों के नाम ही उस उत्पाद के नाम के रूप में स्थापित हो गये हैं, जैसे फोटो स्टेट की जीरोक्स मशीन, टुल्लू पंप व जेसीबी मशीन। गौरतलब है कि जीरोक्स, टुल्लू व जेसीबी कंपनियों के नाम हैं, न कि उत्पाद के लेकिन उत्पाद के नाम के रूप में यही प्रचलन हैं।
ब्रांड का लाभ यह है कि इसके जरिये सामान्य वस्तु को भी असामान्य कीमत पर बेचा जा सकता है।
ब्रांड से एक ओर जहां उच्च गुणवत्ता की उम्मीद की जाती है, तो दूसरी ओर उसके उपभोक्ताओं को किसी ब्रांड वाले उत्पाद के प्रयोग से आम लोगों से हटकर दिखने की आत्म संतुष्टि भी मिलती है।
ब्रांड को विकसित करने में गारंटी, वारंटी जैसी बिक्री बाद सेवाओं की काफी बड़ी भूमिका रहती है, जिसके जरिये उत्पाद के प्रति अपने प्रयोगकर्ताओं, ग्राहकों के मन में अपनत्व, विश्वास का भाव जागृत किया जाता है। और कोई उत्पाद यदि इन तरीकों से ब्रांड के रूप में स्थापित हो जाता है तो फिर ब्रांड की बडी धनराशि में खरीद-बिक्री भी की जाती है।
क्या है ब्रांड :
ब्रांड उत्पाद की कंपनी के नाम व ‘लोगो’का सम्मिश्रण है, जिसकी अपनी छवि से उपभोक्ताओं के बीच उस उत्पाद का जुड़ाव उत्पन्न होता है। ब्रांड की पहचान कंपनी के लोगो व मोनोग्राम से होती है। जैसे एडीडास, नाइकी, बाटा, टाटा आदि ब्रांड के लोगो व मोनोग्राम एक खास तरीके के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं।
आने वाला समय ब्रांड का:
बीते दौर में कुछ गिनी-चुनी चीजें ही ब्रांड के साथ मिलती थीं, जैसे वाहन, गाड़ियां, अल्मारी, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, जूते व भोजन सामग्री में चाय।
लेकिन बदलते दौर में कपड़ों के साथ ही सोना, हीरा जैसे महंगे आभूषणों से लेकर भोजन सामग्री में चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, चीनी व सब्जी आदि भी ब्रांड के साथ बेचने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। और वह दिन दूर नहीं जब अंडे, मांस व फल जैसे उत्पाद भी ब्रांड के नाम से बेचे जाएेंगे।
ब्रांड विकसित करने की प्रक्रिया:
1. गुणवत्ता :
ब्रांड का सर्वप्रमुख गुण उसकी गुणवत्ता है। उपभोक्ता किसी उत्पाद को उसका ब्रांड देखकर सबसे पहले इसलिये खरीदते हैं कि वह उस उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति अपनी ओर से बिना किसी जांच किये संतुष्ट महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि अमुख ब्रांड के उत्पाद की गुणवत्ता हर बार ठीक वैसी ही होगी, जैसी उन्होंने पिछली बार उस उत्पाद में पाई थी।
उदाहरण के लिये यदि उपभोक्ता किसी ब्रांड के सेब या आलू खरीदते हैं तो हमें हर बार समान आकार व स्वाद के सेब या आलू ही प्राप्त होंगे।
लिहाजा, ब्रांड विकसित करने के लिये सबसे पहले उत्पाद की गुणवत्ता तय की जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गुणवत्ता से तात्पर्य उत्पाद की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होना नहीं वरन तय मानकों के अनुसार होना है।
2. श्रेष्ठ होने की आत्म संतुष्टि :
किसी ब्रांड के उत्पाद को उपभोक्ता इसलिये भी खरीदते हैं कि उसके प्रयोग से वह सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का प्रयोग करने का दंभ पालता है और दूसरों को ऐसा प्रदर्शित कर आत्म संतुष्टि प्राप्त करता है।
इसी भाव के कारण अक्सर धनी वर्ग के उपभोक्ता खासकर वस्त्रों, जूतों व गाड़ियों जैसे प्रदर्शन करने वाले उत्पादों को बड़े शोरूम से खरीदना पसंद करते हैं, और दोस्तों के बीच स्वयं की शेखी बघारते हुऐ उस शोरूम से उत्पाद को खरीदे जाने की बात बढ़-चढ़कर बताते हैं।
वहीं कई लोग जो ऐसे बड़े शोरूम से महंगे दामों में उत्पाद नहीं खरीद पाते वह उस ब्रांड के पुराने उत्पाद फड़ों से खरीदकर झूठी शेखी बघारने से भी गुरेज नहीं करते।
अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में भी खासकर लक्जरी यानी विलासिता की वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण को मांग व पूर्ति के सिद्धांत से अलग रखा गया है। ब्रांड के नाम पर सामान्यतया उत्पाद अपने वास्तविक दामों से कहीं अधिक दाम पर बेचे जाते हैं, और उपभोक्ता इन ऊंचे दामों को खुश होकर वहन करता है, वरन कई बार कम गुणवत्ता के उत्पादों को भी अधिक दामों में खरीदने से गुरेज नहीं करता।
3. विज्ञापन एवं प्रस्तुतीकरण:
विज्ञापन एवं प्रस्तुतीकरण की ब्रांड के निर्माण में निर्विवाद तौर पर बड़ी भूमिका होती है। विज्ञापन व प्रस्तुतीकरण दो तरह से ब्रांड की छवि के उपभोक्ताओं के मन में विस्तार व स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
पहला, विज्ञापन व प्रस्तुतीकरण से नये उपभोक्ता उत्पाद के प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरे, उसे प्रयोग कर चुके उपभोक्ताओं में अपने पसंदीदा ब्रांड के विज्ञापनों को देखकर अन्य लोगों से कुछ अलग होने का भाव जागृत होता है।
4. गारंटी एवं वारंटी :
गारंटी एवं वारंटी खरीद बाद सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। यदि किसी उत्पाद को खरीदे जाने के बाद भी कंपनी उसके सही कार्य करने की गारंटी देती है, और कोई कमी आने पर उसे दुरुस्त करने का प्रबंध करती है तो उपभोक्ता उस उत्पाद पर आंख मूँद कर विश्वास कर सकते हैं। यही विश्वास ब्रांड के प्रति उपभोक्ता के जुड़ाव को और मजबूत करता है।
कई बार उपभोक्ता एक ब्रांड को खरीदने के बाद दूसरे ब्रांड के उत्पाद में मौजूद गुणों का लाभ न ले पाने की कमी व निराशा महसूस करता है। गारंटी व वारंटी उसके इस भाव को कम करने तथा खरीदे गये ब्रांड के प्रति उसके प्रेम को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
भूमंडलीकरण का मीडिया पर प्रभाव
भूमंडलीकरण यानी (Globalization) आज के दौर में कमोबेश सर्वाधिक चर्चित शब्द है। वास्तव में इस शब्द का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख भारतीय मिथकों, धर्मग्रंथों में “वसुधैव कुटुंबकम्” के रूप में मिलता है। “वसुधैव कुटुंबकम्” के माध्यम से एक “विश्व ग्राम” की कल्पना की गई थी, जो अपने तब के अर्थ के विपरीत इतर रूप में आज साकार होता नजर आता है।
भूमंडलीकरण की चुनौतियां:
आज के दौर में भूमंडलीकरण से तात्पर्य दुनिया के संचार माध्यमों से आपस में जुड़ जाने और करीब आ जाने से लिया जाता है। इस तरह अत्याधुनिक संचार माध्यमों के जरिये जहां एक सेकेंड से भी कम दूरी में संदेशों, समाचारों को दुनिया के हर कोने में प्रसारित किया जा सकता है, वहीं यह प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई है कि इसे ‘सूचना विष्फोट” तक कहा जा रहा है। वहीं इसके कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े हैं।
भूमंडलीकरण ने बीते दो दशकों में भारत जैसे महादेश के समक्ष कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। अत्यधिक सूचनाओं को संभालने में अफरा-तफरी जैसा माहौल है। जन संचार माध्यम भी पल-प्रतिपल बदल रहे हैं। और व्यापक अर्थाें में भूमंडलीकरण जन संचार को बाजारीकरण में तब्दील कर रहा है।
आज के दौर में मीडिया के लिये आफत बने एफडीआई भी इसी भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप हैं।
भूमंडलीकरण और एफडीआई :
उल्लेखनीय है कि भारत देश की आजादी के बाद शुरुआती नीतियां विदेशी आयात को हतोत्साहित करने वाली थीं। केवल सरकार ही गिने-चुने क्षेत्रों में आयात व विदेशी निवेश कर सकती थी। लेकिन धीरे-धीरे देश में विकास की गति बढ़ाने के नाम आयात व विदेशी निवेश को छूट मिलने लगीं।
1990 के दशक में भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत होने लगी, और देश की नीतियां कमोबेश विदेशी निवेश के मामले में उलट गईं। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने लगा। अब कोई भी व्यक्ति विदेशी उत्पाद खरीद सकता था।
1992 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई (फारन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट) के लिये झिझक के साथ रास्ते खुलने लगे। मीडिया को अलग रखते हुऐ कुछ क्षेत्रों में 26 प्रतिशत एफडीआई को अनुमति दे दी गई।
लेकिन 1999 तक एफडीआई की हवा भूमंडलीकरण की आंधी बन चुकी थी। आकर्षक ग्लेज्ड कागज पर छपीं विदेशी पत्र-पत्रिकाऐं पहले-पहल भारत आने लगीं। बेहतर गुणवत्ता व साज-सज्जा के कारण यह भारतीय पत्र-पत्रिकाओं के मुकाबले अधिक बिकते थे, जिनसे मुकाबला करने के लिये भारतीय मीडिया भी तकनीकी संवर्धन (Technical Enhancement) के लिये एफडीआई की मांग करने लगे। परिणामस्वरूप पूर्व में इसकी धुर विरोधी रही अटल विहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने पहली बार मीडिया में भी 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दे दी।
इसके साथ ही देश में केबल और इसके जरिये विदेशी चैनलों की बाढ़ आ गई, जिनसे मुकाबले के लिये देश के अनेक मीडिया संस्थानों ने भी बड़े एफडीआई का सहारा लिया। लेकिन एफडीआई की शर्तें काफी कठिन थीं, इस कारण अपेक्षा के विपरीत अधिक मीडिया संस्थान एफडीआई से दूर ही रहे।
एफडीआई और विज्ञापनों के लिये गला काट प्रतिस्पर्धा
लेकिन हालात ऐसे हो गये कि एफडीआई का सहारा लेने वाले संस्थान जहां एफडीआई की कड़ी शर्ताें से छुटकारा पाने के लिये, तो अन्य बिना एफडीआई के ही विदेशी मीडिया का मुकाबला करने के लिये विज्ञापनों का सहारा लेने लगे। परिणामस्वरूप विज्ञापन लेने के लिये आज के दौर की मीडिया की सबसे बड़ी परेशानी, विज्ञापनों के लिये मीडिया संस्थानों में गला काट प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, और इस तरह भूमंडलीकरण के कारण मीडिया का पूरा परिदृश्य ही बदल गया।
भूमंडलीकरण बनाम बाजारवाद-उत्पाद बना मीडिया, बिकने को बैठा बाजार में
वास्तव में भूमंडलीकरण को आज के परिप्रेश्य में बाजारवाद का ही एक पर्यायवाची शब्द तक कहा जाने लगा है। अधिक लाभ कमाने की होड़ में मीडिया आज जो बिकता है वही लिखता या दिखाता है। इलेक्ट्रानिक व प्रिंट दोनों तरह की मीडिया इसकी गिरफ्त में हैं। बाजारवाद के प्रभाव में एक ओर खबरें बाजार और विज्ञापनदाताओं से प्रभावित हो रही हैं, दूसरी ओर भाषा के स्तर पर जबर्दस्त ह्रास हो रहा है। एक ओर स्थानीय भाषाओं का पुट खबरों में जुड़ रहा है तो दूसरी ओर बाजार के चलताऊ शब्द तेजी से आ रहे हैं। हिंदी ने जरूर स्वयं को, स्वयं की दुनिया में सबसे बड़ी पाठक संख्या होने के कारण आगे बढ़ाया है पर अंग्रेजी को स्वयं पर हावी होने देने की शर्त पर। हिंदी मीडिया में अंग्रेजी शब्दों की इतनी भरमार है कि “हिंग्लिश” जैसे नये शब्द पैदा हो गये हैं। यह भाषा हिंदी के शुद्धतावादियों को कदापि पसंद नहीं आ रही, अलबत्ता युवा पीढ़ी जरूर ऐसी स्थितियों से गद्गद् है। लेकिन सर्वमान्य तथ्य है कि भाषा का जबर्दस्त ह्रास हुआ है।
कंटेंट पर प्रभाव:
इसी तरह कंटेंट के मामले में एक ओर मीडिया जहां अधिक लाभ कमाने के फेर में छोटे शहरों, कश्बों की ओर जाता चला जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रीयता का हास भी होता जा रहा है। स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में अब राष्ट्रीय खबरें कम ही दिखती हैं, और इसी तरह राष्ट्रीय चैनलों, पत्रों में छोटे शहरों की बड़ी खबरों को भी जगह नहीं मिलती।
अधिक लाभ की कोशिश में कम मानदेय पर संवाददाता पत्रकार रखे जा रहे हैं, और जब तक वह अनुभवी होकर अधिक वेतन की मांग करते हैं, उन्हें संस्थान से बाहर का रास्ता दिखाकर अनुभवहीन नये लोगों को कम खर्च पर लाने को वरीयता दी जाती है, इसका प्रभाव भी खबरों के कंटेंट पर साफ दिख जाता है।
लाभ :
भूमंडलीकरण के नुकसान ही नहीं, कई लाभ भी हैं। वास्तव में आज हम भारत में जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के किसी भी देश की बराबरी पर आ गऐ हैं। देश की बड़ी जनसंख्या इंटरनेट से जुड़ गई है। फेसबुक व ट्विटर सरीखी सोशियल साइटों पर विचार साझा कर रहे हैं, अखबारों के इंटरनेट संस्करण और ई-पेपर उनके छपने से पूर्व ही अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। मोबाइल के जरिये ही दुर्घटना की फोटो तत्काल पहुंचाकर समाचारों में तेजी ला रहे हैं, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर भूमंडलीकरण के कारण ही है। डिश के माध्यम से देश-दुनिया के मनचाहे चैनलों तक हमारी पहुंच है और हम दुनिया के किसी कोने में भी अपनी लोक भाषा के कार्यक्रम तथा अपने छोटे शहरों की खबरें ले पा रहे हैं, या अपने बिछुड़ गये मित्रों से तथा दुनिया भर के अनजाने लोगों से संपर्क व दोस्ती कर पा रहे हैं। कंम्यूटर, मोबाइल पर ही लाखों रुपये के लेन-देन कर पा रहे हैं तो यह भी कहीं न कहीं भूमंडलीकरण का ही लाभ है।
समुदाय संचालित विकास (Society Driven Development)
समुदाय संचालित विकास यानी (Society Driven Development) को सामान्यतया CDD भी कहा जाता है। विकास की इस नई अवधारणा में समुदाय को न केवल विकास का प्रमुख अंग माना जाता है, वरन समुदाय स्वयं ही अपनी विकास योजनाओं का संचालन करता है।
इसके तहत योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी समुदाय को दे दी जाती है, समुदाय के लोग ही योजना को बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन और आगे संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जबकि सरकारी विभाग तकनीकी के स्तर पर उनकी मदद करते हैं।
वर्ष 1970 से सर्वप्रथम विकास में सहभागिता यानी PARTICIPATION की बात शुरू हुई थी, जबकि 1990 के बाद से विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी विकास कार्यों के लिये धन देने वाली वैश्विक संस्थाओं ने समुदाय संचालित विकास के आधार पर ही योजनाएें चलानी शुरू कीं।
समुदाय संचालित विकास के तहत समुदाय स्वयं अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुऐ अपनी जरूरत की योजनाएें बनाता है। गांव के गरीब ग्रामीणों को भी साझेदार यानी पार्टनर का दर्जा दे दिया जाता है।
समुदाय संचालित विकास की विशेषताएें
1. समुदाय संचालित विकास आवश्यकता पर आधारित होती है।
2. इसमें क्षेत्र की जरूरत के आधार पर समस्याओं के समाधान तलाशे जाते हैं।
3. प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रित उपयोग किया जाता है।
4. निर्णयों की शक्ति समुदाय के हाथ में दे दी जाती है।
5. शक्ति का विकेंद्रीकरण समुदाय संचालित विकास की बड़ी विशेषता है।
समुदाय संचालित विकास के लाभ
1. Demand Driven Approach : समुदाय संचालित विकास आवश्यकता यानी पर आधारित होता है।
2. Site Specific Solutions : इसमें क्षेत्र की जरूरत के अनुसार समाधान मिल जाते हैं।
3. Decentralisation (विकेंद्रीयकरण): पंचायतों जैसे स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां व संस्थाएें कार्य कराती हैं। इस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। छोटे-छोटे निर्णयों के लिये सरकार या बड़े अधिकारियों का मुंह नहीं ताकना पड़ता।
4. Institutional Arrangements : समुदाय के लोग स्वयं सहायता समूहों-एनजीओ, संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मियों, ग्राम पंचायत सहित कई संस्थाओं से जुड़े लोग मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार सामुदायिक सहभागिता के जरिये बहुत से लोगों के ज्ञान का उपयोग होता है, व कार्य बेहतर होते हैं।
5. Participation (भागेदारी): Participatory Development Communication यानी विकास सहभागी संचार के जरिये विभिन्न वर्गों के बीच संचार तथा भागेदारी होती रहती है। हर किसी के उपयोगी विचारों को योजना में शामिल किया जाता है।
6. Low Maintenance Cost (मितव्ययिता) : योजनाओं के संचालन (Running Cost) में मितव्ययिता रहती है।
7. अधिक पारदर्शिता : सरकारी विभागों, समुदाय, सामाजिक संस्थाओं आदि के एक साथ मिलकर कार्य अधिक पारदर्शिता से होते हैं। सबको पता होता है कि क्या कार्य हो रहे हैं, और क्यों तथा किस तरह हो रहे हैं।
8. इस प्रकार कार्यों की गुणवत्ता अन्य किसी प्रविधि से बेहतर होती है।
समुदाय संचालित विकास की हानियां
हर किसी प्रविधि की भांति समुदाय संचालित विकास पद्धति में कार्य करने की भी अनेक हानियां हैं।
1. Elite Domination : अक्सर समर्थ लोग विकास योजनाओं को अपने पक्ष में मोड़कर उनके लाभ हड़प जाते हैं। क्योंकि असमर्थ और योजना के वास्तविक जरूरतमंद लोग समर्थों की उपस्थिति में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। इसलिये उन्हें योजनाओं के लाभ भी नहीं मिल पाते हैं।
2. अधिक संस्थाओं की भागेदारी होने के कारण अक्सर उनके बीच में समन्वय स्थापित करने की दिक्कत आती है। इस कारण कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं।
3. लाल फीताशाही भी समुदाय संचालित विकास की राह में बड़ा रोढ़ा है। पुरानी व्यवस्था के अभ्यस्त लोग व अधिकारी जल्दी इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
4. संस्थाएें, सरकारी विभागीय अधिकारी अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। इस कारण भी समुदाय संचालित विकास का लाभ समाज को नहीं मिल पाता है।
समुदाय संचालित विकास के महत्वपूर्ण अंग: समुदाय संचालित विकास के दो महत्वपूर्ण अंग हैं।
अ. Opinion Leaders : ‘Two Step Theory’ में ओपिनियन लीडर्स की उपयोगिता बताई गई है। ओपिनियन लीडर्स-
1. Heavy Media Users होते हैं।
2. ज्ञान वैशिष्ट्य : उन्हें विषय का विशिष्ट ज्ञान (Specialized knowledge) होता है।
3. वह बड़ी हैसियत (High Esteem) वाले लोग होते हैं।
वहीं कार्ट्ज (Kartz) के अनुसार ओपिनियन लीडर्स की शख्शियत बड़ी व विश्वसनीय होती है। वह ज्ञानवान होते हैं, और समाज में उनकी बात सुनी और मानी जाती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं।
ब.Change Agents: चेंज एजेंट्स वे लोग हैं जो समुदाय संचालित विकास की नई अवधारणा को समाज के लोगों को समझाकर इसे उनके लिये ग्राह्य बनाते हैं।
उनका मुख्य कार्य इस बदलाव के लिये भूमिका बनाना होता है।
1. वह मूलत: स्थानीय लोग ही होते हैं।
2. इस प्रकार एक तरह से वह समुदाय एवं सरकारी एजेंसी के बीच फैसीलिटेटर (Facilitator) की भूमिका निभाते हैं।
3. वह संचार के माध्यमों का प्रयोग कर समुदाय के लोगों को उन्हीं की भाषा में योजना के गुण-दोष (खासकर गुण) समझाते हैं।
4. ग्रामीणों से सूचनाएें, उनके विचार लेते हैं, उनकी समस्याओं, आपत्तियों का समाधान तलाशते हैं, और अपने मूल कार्य के उद्देश्य को पूरा करते हुऐ उन्हें योजना के लिये राजी करते हैं।