सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है कुमाउनी शास्त्रीय होली

- पौष माह के पहले रविवार से ही शुरू हो जाती हैं शास्त्रीय रागों में होलियों की बैठकें और सर्वाधिक लंबे समय चलती हैं होलियां
- प्रथम पूज्य गणेश से लेकर पशुपतिनाथ शिव की आराधना और राधा-कृष्ण की हंसी-ठिठोली से लेकर स्वाधीनता संग्राम व उत्तराखंड आंदोलन की झलक भी दिखती है (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मार्च 2025 । देश भर में जहां होली रंगों से भरी होती है और मौज-मस्ती के त्यौहार पर फाल्गुन माह में गाई व खेली जाती है, वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होली की शुरुआत पौष माह के पहले रविवार से ही विष्णुपदी होली गीतों के साथ ही हो जाती है। कुमाऊं की होली की दूसरी विशिष्टता बैठकी होली यानी अर्ध शास्त्रीय गायकी युक्त होली की है। जबकि एक अन्य विशिष्टता खड़ी होली की है, जिसमें होल्यारों यानी होली गायक एक विशिष्ट तरीके से ढोल की थाप पर पद संचालन करते हुए नृत्य करते हैं।
इसके अलावा ‘चीर बंधन’ एवं ‘चीर हरण’ भी कुमाऊं की होली की एक अन्य विशिष्टता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुमाऊं की होने और अर्ध शास्त्रीय तरीके से गाये जाने के कारण शास्त्रीय होली भी कही जाने के साथ कुमाउनी होली में कुमाऊं की लोकभाषा कुमाउनी की जगह ब्रज एवं अवधी भाषाओं के शब्दों की अधिकता होती है, और इससे भी बड़ी बात यह कि कुमाउनी होली करीब 1500 वर्ष पुरानी परंपरा की थाती है, जो कि 10वीं शताब्दी में चंद शासनकाल से शुरू मानी जाती है।
इसलिये पौष माह से शुरू हो जाती है कुमाउनी होली
कुमाउनी होली के पौष माह से ही प्रारंभ हो जाने के पीछे यह कहा जाता है कि पौष मास में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। हिंदू कलेंडर का यह दसवां महीना पूजा पाठ जप-तप व दान के लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शीतकाल के इस माह में विश्व की उत्पत्ति का जीवन की ऊर्जा के स्रोत सूर्य की आराधना आरोग्य तथा सौभाग्य देती है। यह भी माना जाता है पर्वतीय शीत जलवायु का प्रदेश होने और इस दौरान दिन छोटे व रात्रि लंबी होने के कारण लोग ईश्वर को याद करते हुए होलियां गाकर ठंडी रातें बिताते थे।
इसीलिये पौष के प्रथम रविवार से प्रारंभ होने वाली कुमाऊं की होली को निर्वाण की होली कहा जाता है जो बैठकर गायी जाती है, और बैठी होली भी कही जाती है। इस दौरान गायी जाने वाले होली गीत या होलियां भगवान गणेश व शिव आदि की भक्ति पर आधारित होती हैं। आगे बसत पंचमी से इन होलियों में श्रृंगार का भाव आने लगता है और राधा-कृष्ण तथा राम-सीता आदि की होलियां गायी जाने लगती हैं।
कुमाउनी होलियों में कुमाउनी लोकभाषा से अधिक बाहरी शब्दों का कारण
कुछ विद्वानों के अनुसार चंद शासनकाल में बाहर से ब्याह कर आयीं राजकुमारियां अपनी परंपराओं व रीति-रिवाजों के साथ होली को भी यहां साथ लेकर आयीं। वहीं अन्य विद्वानों के अनुसार प्राचीनकाल में यहां के राजदरबारों में बाहर के गायकों के आने से यह परंपरा आई है। कुमाऊं के प्रसिद्ध जनकवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’ के अनुसार कुमाऊं की शास्त्रीय गायकी होली में बृज व अवध से लेकर दरभंगा तक की परंपराओं की छाप स्पष्ट रूप से नजर आती है तो नृत्य के पद संचालन में ठेठ पहाड़ी ठसक भी मौजूद रहती है।
इस प्रकार कुमाउनी होली कमोबेश शास्त्र व लोक की कड़ी तथा एक-दूसरे से गले मिलने में ईद जैसे आपसी प्रेम बढ़ाने वाले त्यौहारों की झलक भी दिखाती है। साथ ही कुमाउनी होली में प्रथम पूज्य गणेश से लेकर गोरखा शासनकाल से पड़ोसी देश नेपाल के पशुपतिनाथ शिव की आराधना और ब्रज के राधा-कृष्ण की हंसी-ठिठोली से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड आंदोलन की झलक भी दिखती है, यानी यह अपने साथ तत्कालीन इतिहास की सांस्कृतिक विरासत को भी साथ लेकर चली हुई है।
कुमाउनीं होली में चीर व निशान की विशिष्ट परम्परायें
कुमाऊं में चीर व निशान बंधन की भी अलग विशिष्ट परंपरायें हैं। इनका कुमाउनीं होली में विशेश महत्व माना जाता है। होलिकाष्टमी के दिन ही कुमाऊं में कहीं कहीं मन्दिरों में ‘चीर बंधन’ का प्रचलन है। पर अधिकांशतया गांवों, शहरों में सार्वजनिक स्थानों में एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। इसके लिए गांव के प्रत्येक घर से एक एक नऐ कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े ‘चीर’ के रूप में लंबे लटठे पर बांधे जाते हैं। इस अवसर पर ‘कैलै बांधी चीर हो रघुनन्दन राजा’, ’सिद्धि को दाता गणपति बांधी चीर हो’ जैसी होलियां गाई जाती हैं।
इस होली में गणपति के साथ सभी देवताओं के नाम लिऐ जाते हैं। कुमाऊं में ‘चीर हरण’ का भी प्रचलन है। गांव में चीर को दूसरे गांव वालों की पहुंच से बचाने के लिए दिन-रात पहरा दिया जाता है। चीर चोरी चले जाने पर अगली होली से गांव की चीर बांधने की परंपरा समाप्त हो जाती है। कुछ गांवों में चीर की जगह लाल रंग के झण्डे ‘निशान’ का भी प्रचलन है, जो यहां की शादियों में प्रयोग होने वाले लाल सफेद ‘निशानों’ की तरह कुमाऊं में प्राचीन समय में रही राजशाही की निशानी माना जाता है।
 बताते हैं कि कुछ गांवों को तत्कालीन राजाओं से यह ‘निशान’ मिले हैं, वह ही परंपरागत रूप से होलियों में ‘निशान’ का प्रयोग करते हैं। सभी घरों में होली गायन के पश्चात घर के सबसे सयाने सदस्य से शुरू कर सबसे छोटे पुरुष सदस्य का नाम लेकर ‘घर के मालिक जीवें लाख सौ बरीस…हो हो होलक रे’ कह आशीष देने की भी यहां अनूठी परंपरा है।
बताते हैं कि कुछ गांवों को तत्कालीन राजाओं से यह ‘निशान’ मिले हैं, वह ही परंपरागत रूप से होलियों में ‘निशान’ का प्रयोग करते हैं। सभी घरों में होली गायन के पश्चात घर के सबसे सयाने सदस्य से शुरू कर सबसे छोटे पुरुष सदस्य का नाम लेकर ‘घर के मालिक जीवें लाख सौ बरीस…हो हो होलक रे’ कह आशीष देने की भी यहां अनूठी परंपरा है।
 कुमाउनी होली के समापन अवसर पर दी जाने वाली आशीषें
कुमाउनी होली के समापन अवसर पर दी जाने वाली आशीषें
 गावैं ,खेलैं ,देवैं असीस, हो हो हो लख रे।
गावैं ,खेलैं ,देवैं असीस, हो हो हो लख रे।
बरस दिवाली बरसै फ़ाग, हो हो हो लख रे।
जो नर जीवैं, खेलें फ़ाग, हो हो हो लख रे।
आज को बसंत कृष्ण महाराज का घरा, हो हो हो लख रे।
श्री कृष्ण जीरों लाख सौ बरीस, हो हो हो लख रे।
यो गौं को भूमिया जीरों लाख सौ बरीस, हो हो हो लख रे।
यो घर की घरणी जीरों लाख सौ बरीस, हो हो हो लख रे।
गोठ की घस्यारी जीरों लाख सौ बरीस, हो हो हो लख रे।
पानै की रस्यारी जीरों लाख सौ बरीस, हो हो हो लख रे।
गावैं होली देवैं असीस, हो हो हो लख रे॥
कुमाउनी होली में रंगों से अधिक रागों में भी उड़ते हैं होली के विविध ‘रंग’, यहां अनूठी है बैठकी, खड़ी, धूम व महिला होलियों की परंपरा
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मार्च 2025। देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं अंचल में रामलीलाओं की तरह राग व फाग का त्योहार होली भी अलग वैशिष्ट्य के साथ मनाई जाती हैं। यूं कुमाऊं में होली के दो प्रमुख रूप मिलते हैं, बैठकी व खड़ी होली, परन्तु अब दोनों के मिश्रण के रूप में तीसरा रूप भी उभर कर आ रहा है। इसे धूम की होली कहा जाता है।
इनके साथ ही महिला होलियां भी अपना अलग स्वरूप बनाऐ हुऐ हैं। इन सब के बीच परंपरागत कुमाउनी होली में रंगों से अधिक, रागों में भी होली के विविध ‘रंग’ उड़ते हैं। माना जाता है कि प्राचीनकाल में यहां के राजदरबारों में बाहर के गायकों के आने से राग-रागिनियों पर आधारित यह होली गीत यहां आऐ हैं। इनमें शास्त्रीयता का अधिक महत्व होने के कारण इन्हें शास्त्रीय होली भी कहा जाता है।
अलग-अलग समयों पर अलग-अलग तरह की होलियों को गाये जाने की परंपरा
पूरे देश में जहां होली सामान्यता एक दिन मनायी जाती है, वहीं कुमाऊं में बैठकी होली की शुरुआत होली के पूर्वाभ्यास के रूप में पौष माह के पहले रविवार से विष्णुपदी होली गीतों से होती है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रहरों में अलग अलग शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियां गाई जाती हैं। इसकी शुरुआत बहुधा धमार राग से होती है, और फिर सर्वाधिक काफी व पीलू राग में तथा जंगला काफी, सहाना, बिहाग, जैजैवन्ती, जोगिया, झिंझोटी, भीमपलासी, खमाज व बागेश्वरी सहित अनेक रागों में भी बैठकी होलियां विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रो के साथ गाई जाती हैं।
बैठकी होली के अंतर्गत आगे बसंत पंचमी से शिवरात्रि तक अर्ध श्रृंगारिक और उसके बाद श्रृंगार रस में डूबी होलियाँ गाई जाती हैं। इनमें भक्ति, वैराग्य, विरह, कृष्ण-गोपियों की हंसी-ठिठोली, प्रेमी प्रेमिका की अनबन, देवर-भाभी की छेड़छाड़ के साथ ही वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति जैसे सभी रस मिलते हैं।
होली के विविध रूप
 अपने समृद्ध लोक संगीत के कारण बैठकी होली कुमाऊं की लोक संस्कृति में रच बस गई है, खास बात यह भी है कि कुछ को छोड़कर अधिकांश होलियों की भाषा कुमाऊंनी न होकर ब्रज व कुछ की अवधी है। सभी बंदिशें राग-रागनियों में गाई जाती है, और यह काफी हद तक शास्त्रीय गायन है। इनमें एकल और समूह गायन का भी निराला अंदाज दिखाई देता है। लेकिन यह न तो सामूहिक गायन है, और न ही शास्त्रीय होली की तरह एकल गायन। महफिल में मौजूद कोई भी व्यक्ति बंदिश का मुखड़ा गा सकता है, जिसे स्थानीय भाषा में ‘भाग लगाना’ कहते हैं।
अपने समृद्ध लोक संगीत के कारण बैठकी होली कुमाऊं की लोक संस्कृति में रच बस गई है, खास बात यह भी है कि कुछ को छोड़कर अधिकांश होलियों की भाषा कुमाऊंनी न होकर ब्रज व कुछ की अवधी है। सभी बंदिशें राग-रागनियों में गाई जाती है, और यह काफी हद तक शास्त्रीय गायन है। इनमें एकल और समूह गायन का भी निराला अंदाज दिखाई देता है। लेकिन यह न तो सामूहिक गायन है, और न ही शास्त्रीय होली की तरह एकल गायन। महफिल में मौजूद कोई भी व्यक्ति बंदिश का मुखड़ा गा सकता है, जिसे स्थानीय भाषा में ‘भाग लगाना’ कहते हैं।
वहीं खड़ी होली में होल्यार दिन में ढोल-मंजीरों के साथ गोल घेरे में पग संचालन और भाव प्रदर्शन के साथ होली गाते हैं, और रात में यही होली बैठकर गाई जाती है। होली गायन के दौरार होल्यारों को परंपरागत तौर पर गुड़ और बीडी-सिगरेट जबकि अब आलू के गुटके, चिप्स व फल खिलाने की परंपरा भी रहती है।
देवी-देवताओं के साथ भी खेली जाती है होली
देश-प्रदेश में जहां लोग अपने परिजनों, सगे संबंधियों व मित्रों के साथ होली के रंग खेलते हैं, वहीं देवभूमि उत्तराखंड के लोग अपने देवी-देवताओं के साथ भी होली खेलते हैं। होली की टोलियां गांव या शहर के मंदिरों में जाती हैं और वहां होली गायन करती हैं। बागेश्वर में बागनाथ और गरुड़ क्षेत्र में कोट भ्रामरी के साथ ही नैनीताल के नयना देवी मंदिरों में होने वाली होलियां दर्शनीय होती हैं। नयना देवी मंदिर में स्थित हनुमान जी की विशाल मूर्ति सहित सभी मूर्तियों को होली के दिन बकायदा अन्य होल्यारों की तरह सफेद वस्त्र पहनाये जाते हैं और रंग चढ़ाते हुए उनके साथ भी होली खेली जाती है।
स्वांग विधा के तहत महिलाएं करती हैं पुरुषों के स्वांग और करती हैं सामयिक स्थितियों पर कटाक्ष
कुमाउनी होली की एक विशिष्टता अनूठी-स्वांग विधा भी है, जिसके तहत खासकर महिलाएं महिलाओं के साथ ही पुरुषों का रूप-वेषभूषा धारण कर उनका स्वांग करती हैं। इस विधा में वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल करने की परंपरा भी रही है। ‘स्वांग’ विधा के तहत, जिसमें खासकर महिला होल्यार अपने आसपास के अथवा चर्चित व्यक्तित्वों के भेष बदलकर आते हैं। हाल के वर्षों में महिलाओं के स्वांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, मेलोनिया ट्रंप, विंग कमांडर अभिनंदन व भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भी नजर आये हैं। देश के सैनिक, पुलवामा की आतंकी घटना और पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक की झलक भी बीते वर्षों में सरोवरनगरी में आयोजित हो रहे फागोत्सव में नजर आई हैं।
दिलों को जोड़ने के साथ बंद पड़े घरों के दर खोलने का माध्यम भी बनी होली
नैनीताल। ‘होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं..’ यह बात तो होली में दिखती ही है। आज के आपाधापी के दौर में अनेक लोग पूरे वर्ष में केवल इसी दिन आपस में मिल पाते हैं। वहीं होली पलायन की मार झेल रहे पहाड़ों के बंद-वीरान पड़े घरों के दरवाजे खोलने का मौका-माध्यम भी साबित हो रही है। पलायन पर प्रवास में रह रहे अनेक लोग होली के मौके पर ही वर्ष में एक बार अपने घर लौटते हैं और अपने बंद पड़े घरों के ताले खोलते हैं। इससे कई वीरान घरों व गांवों में भी इस मौके पर रौनक लौट आती है।
सैलानियों के लिए पसंदीदा ‘होली डेस्टिनेशन’ के रूप में स्थापित हो रहे पहाड़
नैनीताल। होली की अपनी विशिष्टता के कारण पर्वतीय पर्यटन नगरी सरोवरनगरी सहित पूरा पर्वतीय क्षेत्र रंगों के पर्व होली पर सैलानियों के लिये ‘होली डेस्टिनेशन’ यानी होली का त्योहार मनाने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित होता भी नजर आ रहा है। देश भर के सैलानी जहां इस दौरान स्वच्छंदता के साथ ही शांति एवं सुरक्षा के साथ होली का आनंद ले पाते हैं। वहीं दुनिया भर के जिज्ञासु व संस्कृति प्रेमी सैलानी भी खास तौर पर यहां की होली के वैशिष्ट्य को जानने के लिये यहां पहुंचते हैं।
नैनीताल में अमेरिकियों ने भी खेली होली
नैनीताल। सरोवरनगरी नैनीताल में होली के आगाज के साथ अमेरिका के टैक्सास प्रांत के न्यू मैक्सिको से आये आठ विदेशी सैलानियों के एक दल ने भी होली खेलकर माहौल को रंगीन बना दिया, और कुमाऊं की होली में विदेशी रंग भी भर दिये। दल की महिला सदस्यों नोरी टवेरा, डोना जीन विलार्ड व कैथरीन हैरिस टिलेरीना ने तो श्रीराम सेवक सभा के तत्वावधान में फागोत्सव के तहत चल रही महिला होली प्रतियोगिता में महिला होल्यारों के साथ होली नृत्य भी किया,
जबकि दल के पुरुष सदस्य गैबिनो टवेरा, लिन विलार्ड, मैन्युअल टिलेरीना, जॉर्ज ली व विजीनिया ली ने पूरे समय होली का आनंद लिया व कुमाउनी लोक संस्कृति को जानने का प्रयास किया। इस दल को आयोजन में लाने वाले नगर के एंबेसी रेस्टोरेंट स्वामी विक्रम स्याल ने बताया कि उन्होंने यहां की लोक संस्कृति को जानने की इच्छा जताई थी, जिस पर वह उन्हें यहां लेकर आये।
अपनी परंपरा को न छोड़ने का दर्शन भी कराती है कुमाउनी होली
यह भी पढ़ें: होली छाई ऐसी झकझोर कुमूं में

 कभी सोचा है कि देश-दुनिया में अपने अनूठी ठसक व प्रस्तुतीकरण के अंदाज के लिये प्रसिद्ध और करीब 400 वर्ष पुरानी बताई जाने वाली कुमाउनी होली में कुमाउनी की जगह ब्रज व अवधी के शब्दों की प्रचुरता क्यों मिलती है। इस सवाल का जवाब काली कुमाऊं यानी मूल कुमाऊं अंचल चंपावत की संस्था संस्कृति संगठन पाटी के प्रमुख होल्यार राजेंद्र गहतोड़ी देते हैं। गहतोड़ी के अनुसार कुमाऊं में अधिकांश लोग मूलतः मैदानी क्षेत्रों से साथ में वहां की संस्कृति को भी लेकर आये। उदाहरण के लिये काली कुमाऊं अंचल के लोगों को यूपी के झूसी इलाहाबाद क्षेत्र का मूल निवासी माना जाता है।
कभी सोचा है कि देश-दुनिया में अपने अनूठी ठसक व प्रस्तुतीकरण के अंदाज के लिये प्रसिद्ध और करीब 400 वर्ष पुरानी बताई जाने वाली कुमाउनी होली में कुमाउनी की जगह ब्रज व अवधी के शब्दों की प्रचुरता क्यों मिलती है। इस सवाल का जवाब काली कुमाऊं यानी मूल कुमाऊं अंचल चंपावत की संस्था संस्कृति संगठन पाटी के प्रमुख होल्यार राजेंद्र गहतोड़ी देते हैं। गहतोड़ी के अनुसार कुमाऊं में अधिकांश लोग मूलतः मैदानी क्षेत्रों से साथ में वहां की संस्कृति को भी लेकर आये। उदाहरण के लिये काली कुमाऊं अंचल के लोगों को यूपी के झूसी इलाहाबाद क्षेत्र का मूल निवासी माना जाता है।
गहतोड़ी कहते हैं इसलिये कुमाउनी होली में शब्द तो ब्रज व अवध की परंपरागत होलियों के मिलते हैं, किंतु इसमें पुरुषों व महिला होल्यारों का एक खास अंदाज में हाथों में हाथ डालकर और कुमाऊं के परंपरागत झोड़ा नृत्य से मिलते-जुलते अंदाज में कदमों से कदम मिलाते हुये उठना-बैठना आदि मिलाकर एक अलग तरह का अंदाज उत्पन्न करता है। इस प्रकार कुमाउनी होली में शब्द तो मूल ब्रज व अवधी संस्कृतियों के हैं, किंतु अंदाज ठेठ कुमाउनी संस्कृति का है। इस प्रकार दो से अधिक संस्कृतियों के समावेश की यह खाशियतें भी कुमाउनी होली को अन्य से अलग और खास बनाती हैं।
इसके साथ ही श्री गहतोड़ी होली को ईद की तरह मिलन का पर्व भी मानते हैं। इसके साथ ही वह कहते हैं कि होली में ताल प्रमुख बात है। ‘ताल’ में ‘ता’ से कायनात के स्वामी शिव और ‘ल’ से शक्ति का बोध होता है। इस प्रकार होली में महिला-पुरुष एक साथ शिव-शक्ति के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी सार्थक करते हैं।
साथ ही होली होश में रहते हुये जोश प्रकट करने का माध्यम भी है। वहीं श्रीकृष्ण के होली पर महारास मनाने को लेकर गहतोड़ी कहते हैं कि इस तरह से स्वयं को कृष्ण के सर्वाधिक करीब बताने वाली गोपियों को श्रीकृष्ण ने सबके साथ प्रकट होकर उनके अहंकार का शमन किया था। होली सब लोगों को एक रंग में रंगकर सबमें भगवान को देखने का त्योहार भी है। होली को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।
‘होली जलियांवालान बाग मची…’, ‘कैसे हो इरविन ऐतवार तुम्हार….’से ‘डॉन्ट टच माइ अंचलिया मोहन रसिया’ तक बदलती भी रही है कुमाउनी होली
-कुमाउनी होली में होते रहे हैं नये प्रयोग भी, तत्कालीन परिस्थितियों पर कड़े तंज भी कसती रही है होली
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मार्च 2022। अपने शास्त्रीय गायन के लिए ब्रज एवं मथुरा की होली के साथ देश-दुनिया में विख्यात कुमाउनी होली के एक विशेषता यह भी है कि यह स्वयं को वर्तमान के साथ जोड़ती हुई चलती रही है। साथ ही इसमें समय-समय पर नये-नये प्रयोग भी होते रहे हैं। यहां की पारंपरिक चांचरी व गीतों में ‘जोड़’ डालने की परंपरा भी हर वर्ष और वर्ष दर वर्ष समृद्ध करती रही है, और यहां के लोककवि भी होली पर नए प्रासंगिक रचनाएँ देते रहे हैं।
कुमाउनी होली के पुराने जानकार बताते हैं कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को दिल दहला देने वाली घटना हुई थी. इस दिन हजारों भारतीयों पर ब्रिटिश सैनिकों ने फायरिंग की थी, इसमें आदमी, औरत और बच्चे सब मारे गए थे। इस नरसंहार पर कुमाऊं में गौर्दा ने 1920 की होलियों में ‘होली जलियांवालान बाग मची…’ के रूप में नऐ होली गीत से अभिव्यक्ति दी।
इसी प्रकार गुलामी के दौर में ‘होली खेलनू कसी यास हालन में, छन भारत लाल बेहालन में….’ तथा ‘कैसे हो इरविन ऐतवार तुम्हार….’ तथा आजादी के आन्दोलन के दौर में तत्कालीन शासन व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुये ‘अपना गुलामी से नाम कटा दो बलम, स्वदेशी में नाम लिखा दो बलम, मैं भी स्वदेशी प्रचार करूंगी, मोहे परदे से अब तो हटा दो बलम, देश की अपनी बैरागन बनूंगी, सब चीर विदेशी जला दो बलम, अपना गुलामी से नाम कटा दो बलम’
और विदेशी फैशन के खिलाफ ‘छोड़ो कुबाण नवल रसिया’ जैसी होलियों का सृजन हुआ तो आजाद भारत में आजादी के नाम पर उत्श्रृंखलता और गरीबी की स्थितियों पर भी कुमाउनी होली इन बोलों के साथ कटाक्ष किये बिना नहीं रही ‘कां हरला यां चीर कन्हैया, स्यैंणिन अंग उघड़िये छू, खीर भद्याली चाटणा हूं नैं, भूखैल पेट चिमड़ियै छू, गूड़ चांणा लै हमू थैं न्हैंतन, आङन लागी भिदड़ियै छू’ यानी कन्हैया यहां किसकी चीर हरोगे, यहां तो स्त्रियों के पहले से ही खुले हुये हैं।
इधर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के जनकवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’ ने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2001 की होलियों में ‘अली बेर की होली उनरै नाम, करि लिया उनरि लै फाम, खटीमा मंसूरी रंगै ग्येईं जो हंसी-हंसी दी गयीं ज्यान, होली की बधै छू सबू कैं…’ जैसी अभिव्यक्ति दी। इसी कड़ी में आगे चुनावों के दौर में भी गिर्दाने ‘ये रंग चुनावी रंग ठहरा…’ जैसी होलियों का सृजन किया।
लेकिन इधर कुमाउनी होली पर नये दौर में अंग्रेजी और सूफियान कलाम के रंग भी चढ़ते नजर आये हैं। जहां एक ओर ‘डॉन्ट टच माइ अंचलिया मोहन रसिया, आई एम ए लेडी श्रीवृंदावन की, यू आर द लॉर्ड ऑफ गोकुल रसिया’ के साथ अंग्रेजी के शब्द भी कुमाउनी होली में प्रयोग किए गए हैं तो वहीं ‘आज रंग है मेरे ख्वाजा के घर में, मेरे महबूब के घर में, मोहे रंग दे ख्वाजा अपने ही रंग में, तुम्हारे हाथ हैं सुहाग मेरा, मैं तो जोबन तुम पै लुटा बैठी’ और ‘छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके, मोहे सुहागन कीन्ही रे मोसे नैना मिलाइके’ जैसे सूफियाना कलाम भी होली के रूप में पेश किये जा रहे हैं। इधर ऐसी होली भी आई सामने :
‘कुछ काम अब तो कर लो बलम,
बंद करा क्यूं ग्यूं चावल हमरा, गुझिया हुंणी चीनी दिला दो बलम,
खाली खजाना जेब भी खाली-करने वाले जेल चलें,
मुख पे मलो उनके कालो डीजल, भ्रष्टाचार की होरी जलें,
औरों पर तो बहुत चलाई, कुछ खुद पर भी तो चला दो कलम, कुछ काम अब तो कर लो बलम’ जैसी होली रचना सामने आई है।

सामान्यतया कुमाउनी होली को भी कुमाउनी रामलीला की तरह ही करीब 150-200 वर्ष पुराना बताया जाता है, लेकिन जहां कई विद्वान इसे चंद शासन काल की परंपरा की संवाहक बताते हैं, वहीं प्रख्यात होली गायक और बॉलीवुड में भी प्रदेश के लोक संगीत को पहचान दिलाने वाले प्रभात साह गंगोला सहित अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इसका इतिहास प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा की स्थापना से भी पूर्व से चार शताब्दियों से भी अधिक समय पुराना है।
इनके अनुसार कुमाउनी होली का मूल स्वरूप काली कुमाऊं से खड़ी होली के स्वरूप में आया होगा, लेकिन चंद वंशीय शासकों की राजधानी अल्मोड़ा में उस दौर के प्रख्यात शास्त्रीय गायक अमानत अली खां और गम्मन खां की शागिर्द ठुमरी गायिका राम प्यारी जैसी गायिकाएं यर्हां आइं, और स्थानीय शास्त्रीय संगीत के अच्छे जानकार शिव लाल वर्मा आदि उनसे संगीत सीखने लगे। वह 14 मात्रा में पूरी राग-रागिनियों के साथ होली गाते थे।
ऐसे ही अन्य बाहरी लोगों के साथ कुमाउनी होली में ब्रज, अवध व मगध के अष्टछाप कवियों के ईश्वर के प्रेम में लिखे गीत आए। कालांतर में होलियों का मूल शास्त्रीय स्वरूप वाचक परंपरा में एक से दूसरी पीढ़ी में आते हुए और शास्त्रीय संगीत की अधिक गहरी समझ न होने के साथ लोक यानी स्थानीय पुट से भी जुड़ता चला गया, और कुमाउनी होली कमोबेश शास्त्र व लोक की कड़ी सी बन गई। कुमाउनी होली की एक और खासियत यह भी है कि यह पौष माह के पहले रविवार से ही शुरू होकर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तक सर्वाधिक लंबे अंतराल तक चलती है।
इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि (प्राचीन काल में) शीतकाल में पहाड़ों में कृषि व अन्य कार्य सीमित होते थे। ऐसे में लंबी रातों में मनोरंजन के साधन के तौर पर भी होली गायकी के रात-रात लंबे दौर चलते थे। यह परंपरा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। कुमाउनी होली में विभिन्न प्रहरों में अलग अलग शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियां गाई जाती हैं। शुरुआत बहुधा धमार राग से होती है, और फिर सर्वाधिक काफी व पीलू राग में तथा जंगला काफी, सहाना, बिहाग, जैजैवन्ती, जोगिया, झिंझोटी, भीम पलासी, खमाज व बागेश्वरी सहित अनेक रागों में भी बैठकी होलियां विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रो के साथ गाई जाती हैं।
यह भी पढ़ें : सरोवरनगरी में होली पर सर्वधर्म सम्भाव की मिसाल, पिछले 25 वर्षों से जहूर करा रहे हैं होली
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 25 मार्च 2021। सर्वधर्म की नगरी सरोवरनगरी की अनेक खाशियतें हैं, और इनमें से एक है यहां पिछले 25 वर्षों से हो रहे फागोत्सव व होली महोत्सव। 1976 में इन महोत्सवों की नैनीताल से शुरुआत से होने के बाद वर्तमान में प्रदेश के अनेक स्थानों पर ऐसे महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, इस तरह नैनीताल पूरे प्रदेश के ऐसे आयोजनों का प्रणेता भी है। इसके अलावा भी नैनीताल के होली महोत्सव की एक और खाशियत यह भी है कि यहां होने वाले होली महोत्सव के पीछे जहूर आलम नाम के रंगकर्मी हैं, जो सरोवरनगरी की होली में सर्वधर्म सम्भाव का रंग भी भर देते हैं।
जहूर बताते हैं 70 के दशक में नैनीताल सहित पहाड़ों की होली में मैदानी क्षेत्रों की होली के कपड़े फाड़ने, कीचड़ फैंकने व मुंह पर जले तेल आदि की कालिख पोतने जैसे दुर्गुण आ गए थे। इस पर उनके साथ ही उनकी नाट्य संस्था युगमंच के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय गिरीश तिवारी ‘गिर्दा’, विश्वंभर नाथ साह ‘सखा’, राजीव लोचन साह, डॉ. विजय कृष्ण आदि के साथ श्रीराम सेवक सभा व शारदा संघ आदि संस्थाओं के लोग जुटे और कुमाउनी होली को उसके पारंपरिक स्वरूप में बचाने के लिए 1976 से फागोत्सव-होली महोत्सव की शुरुआत हुई।
इसके तलत पहली बार गांवों में अपने घरों व पटांगणों तक सीमित महिलाओं व पुरुष होल्यारों की खड़ी व बैठकी होलियां आयोजित हुईं। बाहर से आने वाले होल्यारों के दलों को कलाकारों के रूप में पहली बार न केवल प्रतिष्ठा दी गई, बल्कि उन्हें इसका पारिश्रमिक भी दिया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में कुमाउनी होली को विषय में रूप में शामिल किया गया। साथ ही कुमाउनी होली को प्रतिष्ठित करने के लिए दो-तीन वर्ष संगोष्ठियां भी आयोजित हुईं और नई पीढ़ी को पारंपरिक कुमाउनी होली पहुंचाने के लिए कार्यशालियां भी लगातार आयोजित की जाने लगीं, जोकि अब भी होती हैं। जहूर कहते हैं उनकी इस पहल का ही प्रभाव है कि आज यहां पारंपरिक तरीके से ही होली का आयोजन होता है, और उसमें मैदानी क्षेत्रों से आए दुर्गुण नहीं दिखाई देते हैं।
यह भी पढ़ें : होलाष्टक के बीच कोई शुभ कार्य, जानें क्यों
शास्त्रानुसार होली से आठ दिन पूर्व होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार होलाष्टक 13 मार्च से शुरू होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस समय आठ दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किये जाते। ज्योतिषाचार्य पण्डित दयानन्द शास्त्री के अनुसार इस बार होलाष्टक रात्रि 12.02 बजे से लग रहे हैं जो कि 20 मार्च होलिका दहन तक चलेगा। इस वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस वर्ष यह 21 मार्च 2019 को मनाया जाएगा।यानी 20 मार्च को होलाष्टक खत्म होने के साथ होलिका दहन होगा और 21 मार्च को रंगों के साथ त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन को लोग छोटी होली भी कहते हैं।
इस अवधि में शुभ कार्य- गर्भाधान, विवाह, नामकरण, विद्यारम्भ, गृह प्रवेश और नव निर्माण आदि नहीं करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से ही होलिका दहन करने वाले स्थान का चयन भी किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव से स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है।
पण्डित दयानन्द शास्त्री बताते हैं कि इन आठ दिनों किसी भी व्यक्ति को ना तो भूमि-भवन खरीदना चाहिये और ना ही वैवाह आदि करना चाहिये। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में शुरू किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रह अपना स्थान बदलते हैं।
धर्मशास्त्रों में वर्णित 16 संस्कार जैसे- गर्भाधान, विवाह, पुंसवन (गर्भाधान के तीसरे माह किया जाने वाला संस्कार), नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, गृह शांति, हवन-यज्ञ कर्म आदि नहीं किए जाते। पण्डित दयानन्द शास्त्री के अनुसार इन दिनों शुरु किए गए कार्यों से कष्ट की प्राप्ति होती है। इन दिनों हुए विवाह से रिश्तों में अस्थिरता आजीवन बनी रहती है अथवा टूट जाती है. घर में नकारात्मकता, अशांति, दुःख एवं क्लेष का वातावरण रहता है।
इस अवधि में भोग से दूर रह कर तप करना ही अच्छा माना जाता है। इसे भक्त प्रह्लाद का प्रतीक माना जाता है। सत्ययुग में हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। वह पहले विष्णु का जय नाम का पार्षद था, लेकिन शाप की वजह से दैत्य के रूप में उसका जन्म हुआ था। वरदान के अहंकार में डूबे हिरण्यकशिपु ने देवताओं सहित सबको हरा दिया। उधर भगवान विष्णु ने अपने भक्त के उद्धार के लिये अपना अंश उसकी पत्नी कयाधू के गर्भ में पहले ही स्थापित कर दिया था, जो प्रह्लाद के रूप में पैदा हुए।
प्रह्लाद का विष्णु भक्त होना पिता हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगता था। दूसरे बच्चों पर प्रह्लाद की विष्णु भक्ति का प्रभाव पड़ता देख पहले तो पिता हिरण्यकशिपु ने उसे समझाया। फिर न मानने पर उसे भक्ति से रोकने के लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बंदी बना लिया। जान से मारने के लिए यातनाएं दीं, पर प्रह्लाद विष्णु भक्ति के कारण भयभीत नहीं हुए और विष्णु कृपा से हर बार बच गए। इसी प्रकार सात दिन बीत गए।
आठवें दिन अपने भाई हिरण्यकशिपु की परेशानी देख उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा जी ने अग्नि से न जलने का वरदान दिया था, प्रह्लाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर गई, पर हुआ उल्टा। देवकृपा से वह स्वयं जल मरी, प्रह्लाद को कुछ नहीं हुआ। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। तभी से भक्ति पर आए इस *संकट के कारण इन आठ दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है।
क्यों होते हैं ये अशुभ दिन?
पण्डित दयानन्द शास्त्री ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के प्रथम दिन अर्थात फाल्गुन शुक्लपक्ष की अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु का उग्र रूप रहता है। इस वजह से इन आठों दिन मानव मस्तिष्क तमाम विकारों, शंकाओं और दुविधाओं आदि से घिरा रहता है, जिसकी वजह से शुरु किए गए कार्य के बनने के बजाय बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को इन आठों ग्रहों की नकारात्मक शक्तियों के कमजोर होने की खुशी में लोग अबीर-गुलाल आदि छिड़ककर खुशियां मनाते हैं। जिसे होली कहते हैं।
जानिए होलाष्टक के इन 8 दिनों में कौन से कार्य करने अशुभ हैं– होलाष्टक में भूलकर भी ना करें शुभ कार्य
- गर्भवती स्त्री को इन दिनों नदी-नाले पार करके यात्रा नहीं करनी चाहिये। ऐसा करने से पेट में पल रहे शिशु को कष्ट होता है।
- होलाष्टक के दौरान विवाह नहीं करना चाहिये क्योंकि तब विवाह का मुहूर्त नहीं होता। इसके अलावा सगाई भी नहीं करनी चाहिये।
- इन दिनों नये घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिये।
- होलाष्टक के दौरान ना ही नया घर खरीदना चाहिये और ना ही भूमि पूजन करवाना चाहिये।
- नवविवाहिताओं को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है।
- होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही है लेकिन इन दिनों में अपने देवी देवता की पूजा करना अनिवार्य हो जाता है। यही नहीं उपवास करने और दान करने से भी लाभ मिलता है।
(Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
यह भी पढ़ें : सरोवरनगरी में सर्वदल-सर्वधर्म की महिलाओं ने एक मंच पर की होली की मस्ती
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 मार्च 2021। सरोवरनगरी में रंगों के पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। पुरुषों की होली की बैठकों के बाद अब महिलाओं की होली, हंसी-ठिठोली, मस्ती भी नजर आने लगी है। बीती शाम के बाद शुक्रवार दोपहर नगर के शारदा संघ सभागार में महिला होल्यारों की मस्ती देखी गई। ऑल इंडिया वीमन कांफ्रेंस में नगर की भाजपा-कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों एवं सर्वधर्म से जुड़ी महिलाएं एक मंच पर होली की मस्ती में झूमती थिरकती नजर आईं। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
यहां संस्था की अध्यक्ष मुन्नी तिवारी, सचिव गौरा देवी देव की अगुवाई में सावित्री सनवाल, तारा बोरा, सभासद गजाला कमाज, रेखा आर्या व निर्मला चंद्रा, भाजपा की पूर्व दायित्वधारी शांति मेहरा, ममता पांडे, डॉ. सरस्वती खेतवाल, दया बिष्ट, रेखा त्रिवेदी, विनीता पांडे, हेमा कांडपाल, दीपा जोशी, अश्की व आफरीन आदि महिलाएं ‘कामिनी भर-भर मारत, मलत-मलत नैना भये लाल, जल भरन चलीं दोनों बहना व भर पिचकारी मारी कुंज गलिन में…’ आदि होली गीतों की मस्ती में झूमती व नाचती नजर आईं।
कुमाऊं में है अनूठी बैठकी, खड़ी, धूम व महिला होलियों की परंपरा
देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं अंचल में रामलीलाओं की तरह राग व फाग का त्योहार होली भी अलग वैशिष्ट्य के साथ मनाई जाती हैं। यूं कुमाऊं में होली के दो प्रमुख रूप मिलते हैं, बैठकी व खड़ी होली, परन्तु अब दोनों के मिश्रण के रूप में तीसरा रूप भी उभर कर आ रहा है। इसे धूम की होली कहा जाता है। इनके साथ ही महिला होलियां भी अपना अलग स्वरूप बनाऐ हुऐ हैं। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
कुमाऊं में बैठकी होली की शुरुआत होली के पूर्वाभ्यास के रूप में पौष माह के पहले रविवार से विष्णुपदी होली गीतों से होती है। माना जाता है कि प्राचीनकाल में यहां के राजदरबारों में बाहर के गायकों के आने से यह होली गीत यहां आऐ हैं। इनमें शास्त्रीयता का अधिक महत्व होने के कारण इन्हें शास्त्रीय होली भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रहरों में अलग अलग शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियां गाई जाती हैं।
शुरुआत बहुधा धमार राग से होती है, और फिर सर्वाधिक काफी व पीलू राग में तथा जंगला काफी, सहाना, बिहाग, जैजैवन्ती, जोगिया, झिंझोटी, भीमपलासी, खमाज व बागेश्वरी सहित अनेक रागों में भी बैठकी होलियां विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्रो के साथ गाई जाती हैं।
बैठकी होली पौष माह के पहले रविवार से ही शुरू हो जाती हैं, और फाल्गुन तक गाई जाती है। पौष से बसंत पंचमी तक अध्यात्मिक, बसंत पंचमी से शिवरात्रि तक अर्ध श्रृंगारिक और उसके बाद श्रृंगार रस में डूबी होलियाँ गाई जाती हैं। इनमें भक्ति, वैराग्य, विरह, कृष्ण-गोपियों की हंसी-ठिठोली, प्रेमी प्रेमिका की अनबन, देवर-भाभी की छेड़छाड़ के साथ ही वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति जैसे सभी रस मिलते हैं। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
बैठकी होली अपने समृद्ध लोक संगीत की वजह से यहाँ की संस्कृति में रच बस गई है, खास बात यह भी है कि कुछ को छोड़कर अधिकांश होलियों की भाषा कुमाऊंनी न होकर ब्रज है। सभी बंदिशें राग-रागनियों में गाई जाती है, और यह काफी हद तक शास्त्रीय गायन है। इनमें एकल और समूह गायन का भी निराला अंदाज दिखाई देता है। लेकिन यह न तो सामूहिक गायन है, और न ही शास्त्रीय होली की तरह एकल गायन। महफिल में मौजूद कोई भी व्यक्ति बंदिश का मुखड़ा गा सकता है, जिसे स्थानीय भाषा में ‘भाग लगाना’ कहते हैं। वहीं खड़ी होली में होल्यार दिन में ढोल-मंजीरों के साथ गोल घेरे में पग संचालन और भाव प्रदर्शन के साथ होली गाते हैं, और रात में यही होली बैठकर गाई जाती है।
कुमाउनी होली में रंगों नहीं, रागों में उड़ते हैं होली के ‘रंग’ (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
कुमाउनी होली में दिन व रात के अलग-अलग प्रहरों तथा अलग-अलग समय में अलग-अलग राग-रागिनियों में होलियां गाने का प्राविधान है। हमेशा पहली होलियां प्रथम पूज्य भगवान गणेश की गाई जाती हैं। पौष माह के पहले रविवार से शुरू होने वाली निर्वाण की होलियां कही जाने वाली होलियां भी भगवान गणेश, शिव और कृष्ण की भक्ति युक्त होती हैं। यह सिलसिला शिवरात्रि तक चलता है। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
इनमें ‘दैंण होया सबूं हुं हो गणेश, बांणी गावै को दुब धरण लागि रयां, त्यार निभाया बिघ्नेश’, राग काफी में ‘गणपति को भज लीजै’ जैसी होलियों से शुरू करते हुए आगे ‘क्यों मेरे मुख पै आवे रे भंवरा, नाही कमल यह श्याम सुंदर की सांवरी सूरत को क्यों मोहे याद दिलाए’, श्याम कल्याण राग में ‘माई के मंदिरवा में दीपक बारूं’ जंगला काफी में ‘होली खेलें पशुपतिनाथ नगर नेपाल में’ जैसी होलियां प्रमुख रूप से गायी जाती हैं। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
वहीं शिवरात्रि से शिव की होलियां अधिक गाई जाती हैं। अलबत्ता, शिवरात्रि से होलिका अष्टमी तक बिना रंग के ही होलियां गाई जाती हैं। आगे बसंत पंचमी से होली गीतों में श्रृंगार रस चढ़ने लगता है, जबकि फाल्गुन माह में पुरुषों के द्वारा रंग युक्त खड़ी व महिलाओं के द्वारा बैठकी होलियां गाई जाती हैं। होलिका अष्टमी को मंदिरों में आंवला एकादशी को गाँव-मोहल्ले के निर्धारित स्थान पर चीर बंधन होता है और रंग डाला जाता है, और होली गायन की शुरुआत बसन्त के स्वागत के गीतों से होती है, जिसमें प्रथम पूज्य गणेश, राम, कृष्ण व शिव सहित कई देवी देवताओं की स्तुतियां व उन पर आधारित होली गीत गाऐ जाते हैं। बसन्त पंचमी के आते आते होली गायकी में क्षृंगारिकता बढ़ने लगती है यथा :
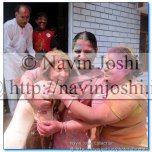
‘आयो नवल बसन्त सखी ऋतुराज कहायो, पुष्प कली सब फूलन लागी, फूल ही फूल सुहायो’
के अलावा जंगला काफी राग में
‘राधे नन्द कुंवर समझाय रही, होरी खेलो फागुन ऋतु आइ रही’
व झिंझोटी राग में
‘आहो मोहन क्षृंगार करूं में तेरा, मोतियन मांग भरूं’
तथा राग बागेश्वरी में
‘अजरा पकड़ लीन्हो नन्द के छैयलवा अबके होरिन में…’
आदि होलियां गाई जाती हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर्व तक के लिए होली बैठकों का आयोजन शुरू हो जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर शिव के भजन जैसे
‘जय जय जय शिव शंकर योगी’
होली के रूप में गाऐ जाते हैं। इसके पश्चात कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में होलिका एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक खड़ी होली गीत जैसे
‘शिव के मन मांहि बसे काशी’, ‘जल कैसे भरूं जमुना गहरी’ व ‘सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन, होरी खेलें गिरिजापति नन्दन’ आदि होलियां गाई जाती हैं।
सामान्यतया खड़ी होलियां कुमाऊं की लोक परंपरा के अधिक निकट मानी जाती हैं और यहां की पारंपरिक होलियां कही जाती हैं। यह होलियां ढोल व मंजीरों के साथ बैठकर व विशिष्ट तरीके से पद संचालन करते हुऐ खड़े होकर प्रायः पीलू राग में गाई जाती हैं। इन दिनों होली में राधा-कृष्ण की छेड़छाड़ के साथ क्षृंगार की प्रधानता हो जाती है। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
इधर कुमाउनीं होली में बैठकी व खड़ी होली के मिश्रण के रूप में तीसरा रूप भी उभर रहा है, इसे धूम की होली कहा जाता है। यह ‘छलड़ी’ के आस पास गाई जाती है। इसमें कई जगह कुछ वर्जनाऐं भी टूट जाती हैं, तथा ‘स्वांग’ का प्रयोग भी किया जाता है। महिलाओं में स्वांग अधिक प्रचलित है। इसमें महिलाएं खासकर घर के पुरुषों तथा सास, ससुर आदि के मर्दाना कपड़े, मूंछ व चस्मा आदि पहनकर उनकी नकल उतारती हैं, तथा कई बार इस बहाने सामाजिक बुराइयों पर भी चुटीले कटाक्ष करती हैं। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
होलियों के दौरान युवक, युवतियों और वृद्ध सभी उम्र के होल्यारों को होली के गीतों में सराबोर देखा जा सकता है। खासकर ग्रामीण अंचलों में तबले, मंजीरे और हारमोनियम के सुर में होलियां गाई जाती हैं, इस दौरान ऐसा लगता है मानो हर होल्यार शास्त्रीय गायक हो गया हो। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत की होलियां खास मानी जाती हैं, जबकि बागेश्वर, गंगोलीहाट, लोहाघाट व पिथौरागढ़ में तबले की थाप, मंजीरे की छन-छन और हारमोनियम के मधुर सुरों पर जब ‘ऐसे चटक रंग डारो कन्हैया’ जैसी होलियां गाते हैं। इधर शहरी क्षेत्रों में हर त्योहार की तरह होली में भी कमी आने लगी है। लोग केवल छलड़ी के दिन ही रंग लेकर निकलते हैं, और एक-दूसरे को रंग लगाते हुए गुजिया और भुने हुए आलू के गुटके खिलाते हैं। गांवों में भांग का प्रचलन भी दिखता है। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
यह भी पढ़ें : नैनीताल में होली के रंग मिले अमीर खुसरो की कव्वाली के संग…
-स्कूली बच्चों के होली गायन में सैनिक स्कूल रहा प्रथम
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मार्च 2022। सरोवरनगरी में नगर की सर्वप्राचीन धार्मिक-सामाजिक संस्था श्रीराम सेवक सभा के तत्वावधान में मनाये जा रहे फागोत्सव के तहत सोमवार को रंग भरी कव्वाली के साथ स्कूली बच्चों की होली प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। नगर के आवागढ़ कंपाउंड के शाहिद अली वारसी की टीम ने ‘होली के रंग अमीर खुसरो के संग’ नाम से कव्वालियों का आयाजन किया। (Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(Holi-Kumaoni, Kumauni classical Holi, Kumauni Holi, Cultural Heritage, Kumaoni Holi, Kumauni Culture, Kumaoni Culture, Holi Swang, Kumaoni Holi, Traditional Holi, Uttarakhand Culture, Kumaon Festival, Holi Celebration, Baithki Holi, Khadi Holi, Vishnupadi Holi, Classical Holi Songs, Folk Music, Chheer Bandhan, Chheer Haran, Indian Festivals, Cultural Heritage, Traditional Music, Holi Dance, Festive Traditions, Pahadi Culture, Ancient Holi, Regional Festivities,)


























